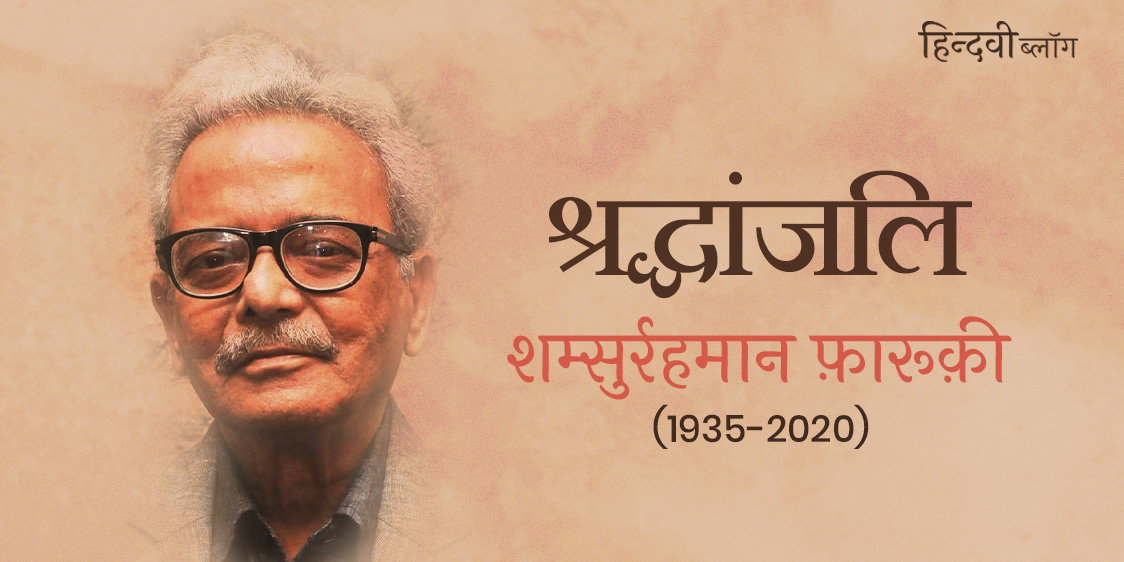
उनकी नज़र और उनकी कहन इस मंज़र में लासानी थी
 अविनाश मिश्र
दिसम्बर 25, 2020
अविनाश मिश्र
दिसम्बर 25, 2020
इस मनहूस साल के आख़िरी सप्ताह में एक और मनहूस ख़बर—शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी (1935–2020) नहीं रहे। उनके भतीजे, दास्तानगो और फ़िल्म निर्देशक महमूद फ़ारूक़ी ने यह सूचना ट्विटर पर दी।
फ़ारूक़ी साहब कई रोज़ से बीमार चल रहे थे। उनके न रहने में बहुत कुछ का न रहना निहाँ है, और इसके साथ ही उनके बहुत कुछ का रह जाना ज़ाहिर है। आज उनके हम सबसे जुदा हो जाने पर, बार-बार दुहराई गई यह बात एक बार और दुहराने की ज़रूरत है कि इस तरह के व्यक्तित्व कभी अपने चाहनेवालों से जुदा नहीं होते हैं। उनके न रहने पर भी उनके चाहने वाले कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते ही जाते हैं।
एक बेहतरीन अफ़सानानिगार, एक दृष्टिवान आलोचक, एक अग्रणी संपादक के रूप में समादृत फ़ारूक़ी साहब का अस्ल जल्वा और रुतबा हिंदी में तब उरूज पर पहुँचा, जब उनका उपन्यास ‘कई चाँद थे सरे-आसमाँ’ [पहला उर्दू संस्करण : 2005, पहला हिंदी संस्करण : 2010 (अनुवाद : नरेश नदीम)] सामने आया। क़रीब साढ़े सात सौ पन्नों के इस उपन्यास को न पढ़ना या न पढ़ पाना, हिंदी में लगभग अनपढ़ होने की अलामत माना गया। इस उपन्यास का उन्वान अहमद मुश्ताक़ के इस शे’र से लिया गया :
कई चाँद थे सर-ए-आसमाँ कि चमक चमक के पलट गए
न लहू मिरे ही जिगर में था न तुम्हारी ज़ुल्फ़ सियाह थी
अठारहवीं सदी का हिन्दुस्तानी जीवन, बेशुमार ब्योरों से भरे हुए पन्ने और उन पर चलती कहानियाँ… इसे पढ़नेवाले पर एक अलग ही दुनिया खुलती है। एक से बढ़कर एक व्यक्तियों, स्थितियों, जगहों और वस्तुओं के वर्णन पढ़ते हुए लगता है कि यह महज़ लेखक का अध्ययन या कल्पना नहीं है, मानो लिखनेवाला इनके बीच से सचमुच गुज़रा है और तब लिख रहा है। एक बातचीत में फ़ारूक़ी साहब ने इस सिलसिले में फ़रमाया :
‘‘आज बीसवीं या इक्कीसवीं सदी में कितने लोगों ने यह कल्पना की होगी कि फ़िरोज़पुर से दिल्ली तक कै दिन में आना-जाना होता था, ऐसी कौन-सी जगहें होती होंगी जहाँ लोग ठहरते होंगे। कुछ मुझे पता था, मसलन मुझे रामपुर से ग़ालिब का सफ़र मालूम था, मीर का भी। दिल्ली से लखनऊ या भरतपुर के रास्ते कैसे-कैसे रहे होंगे या कि कैसे-कैसे थे। मुझे यह किसी हद तक मालूम था कि उस ज़माने में लोग कैसे यात्रा करते थे। मैंने इस उपन्यास में यात्रा को नई आँख से देखा है। मसलन, जब शम्सुद्दीन अहमद निकलता है, दुनिया जानती थी कि उसे अँग्रेज़ों ने बुलाया है और वे उसे मरवा देंगे। वे तभी बाहर निकलकर उसका स्वागत करते हैं, अपने पास ठहराते हैं। मैं यह जानता था कि यह रास्ता है और ऐसे ही लोग उसे मिले होंगे। या जब वह पालम तक पहुँचता है, वह रास्ता वही था जिस पर हम भी पहले गए थे। जब हाईवे नहीं थी, मैं दिल्ली से जयपुर उसी रास्ते से कई बार गया हूँ। उन दिनों पालम का क़िला मेरे सामने पड़ता था। यह सोचना भी कठिन नहीं था कि जब कोई नवाब जैसा रईस वहाँ से गुज़र रहा है, उसके दस-बीस आदमी पहले ही आकर पालम का क़िला ठीक कर दें।’’ [उपन्यासकार का सफ़रनामा, पृष्ठ : 98, शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी से उदयन वाजपेयी का संवाद, राजकमल प्रकाशन, संस्करण : 2018]
ऊपर उद्धृत कथ्य से फ़ारूक़ी साहब के अफ़सानानिगार को और उनके काम करने के ढब को कुछ समझा जा सकता है। उन्हें यह बहुत शुरू में ही लग गया था कि अगर क़लम घिसनी है तो अफ़साने लिखने चाहिए। उनके लड़कपन में आख़िर उर्दू अदब में अफ़सानानिगार ही छाए हुए थे। इस छाया में ज़माना कुछ यों था कि अगर आप जवान और मुसलमान हैं, तब आपके सामने दो ही रास्ते थे : एक वामपंथ का और दूसरा जमात-ए-इस्लामी का। वह 1950-51 का वक़्त था। देश बँट चुका था और फ़ारूक़ी साहब सरीखे नौजवान—जिनके परिवारों पर इस बँटवारे का कुछ ख़ास असर नहीं हुआ था—इन दो रास्तों के बीच ही डोल रहे थे। फिर धीमे-धीमे यह हुआ कि दोनों ही रास्ते काम के नहीं लगे और एक नए रास्ते की तलाश शुरू हुई। इस नए रास्ते में नारों के प्रति ऊब थी और संतुलन के प्रति चिढ़। इस दौर में फ़िक्शन का अधिकांश अख़बारी रपट-सा बाज़ारू हो चला था। ऐसे में फ़ारूक़ी साहब को रास्ता मिला शेक्सपीयर को पढ़कर। उन्हें समझ आ गया कि इस तरह का लेखक न प्रगतिशीलों में जाएगा, न मुल्लों में। टॉमस हार्डी से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ‘‘वह बताता है कि दुःख बहुत है, लेकिन दुःख को बयान करने का भी एक तरीक़ा हुआ करता है, ये वह तरीक़ा नहीं है जो रामानंद सागर या कृश्न चंदर या मंटो के यहाँ नज़र आता है। कुछ और तरीक़ा भी हो सकता है।’’ [उपन्यासकार का सफ़रनामा, पृष्ठ : 28, शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी से उदयन वाजपेयी का संवाद, राजकमल प्रकाशन, संस्करण : 2018]
हार्डी को पढ़ने और समझने से उनकी आंतरिक ज़िंदगी में फ़र्क़ आया। ‘‘उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ीं, जैसे दु:ख बढ़ा, खोने की अनुभूति बढ़ी, सारे ब्रह्मांड की अर्थहीनता की अनुभूति बढ़ी।’’ [वही]
फ़ारूक़ी साहब को अपने फ़िक्शन पढ़ने की तरबियत और ताक़त पर बहुत गर्व रहा। एक साक्षात्कार में ‘दास्तान-ए अमीर हम्ज़ा’ के हवाले से वह बताते हैं कि आज संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं है, जिसने ‘दास्तान-ए अमीर हम्ज़ा’ को पूरा पढ़ा हो। वह इस बात को और दमदार बनाते हैं, जब वह इसमें यह जोड़ते हैं : ‘‘सिर्फ़ मैंने ही उसे पूरा पढ़ा है।’’
फ़ारूक़ी साहब की अदबी ज़िंदगी को अगर एक वाक्य में बताना हो, तब कह सकते हैं कि उन्होंने आलोचना लिखने से पहले अफ़साने लिखे और आलोचना लिखने के बाद भी अफ़साने लिखे। जहाँ तक भारतीय साहित्य का सवाल है, हमने ऐसे बड़े लेखक कम ही देखे हैं। इस मायने में फ़ारूक़ी साहब सचमुच दुर्लभ हैं।
फ़ारूक़ी साहब का जन्म आज़मगढ़ (उत्तर प्रदेश) में हुआ और उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। 1966 से 2005 तक उन्होंने उर्दू साहित्य में आधुनिकता की रहनुमाई करने वाली पत्रिका ‘शबख़ून’ के 299 अंकों का प्रकाशन और संपादन किया। हिंदी में उनके काम-काज का इंतिज़ार और इस्तिक़बाल हमेशा होता रहा। यहाँ तक आते-आते वह समूचे भारतीय साहित्य की एक अज़ीम शख़्सियत के बतौर पहचाने गए। उनकी नज़र और उनकी कहन इस मंज़र में लासानी थी। उन्हें पढ़ना, उन्हें देखना, उन्हें सुनना बहुत कुछ पाने की राह थी। माफ़ कीजिए, थी नहीं; अब भी है।






