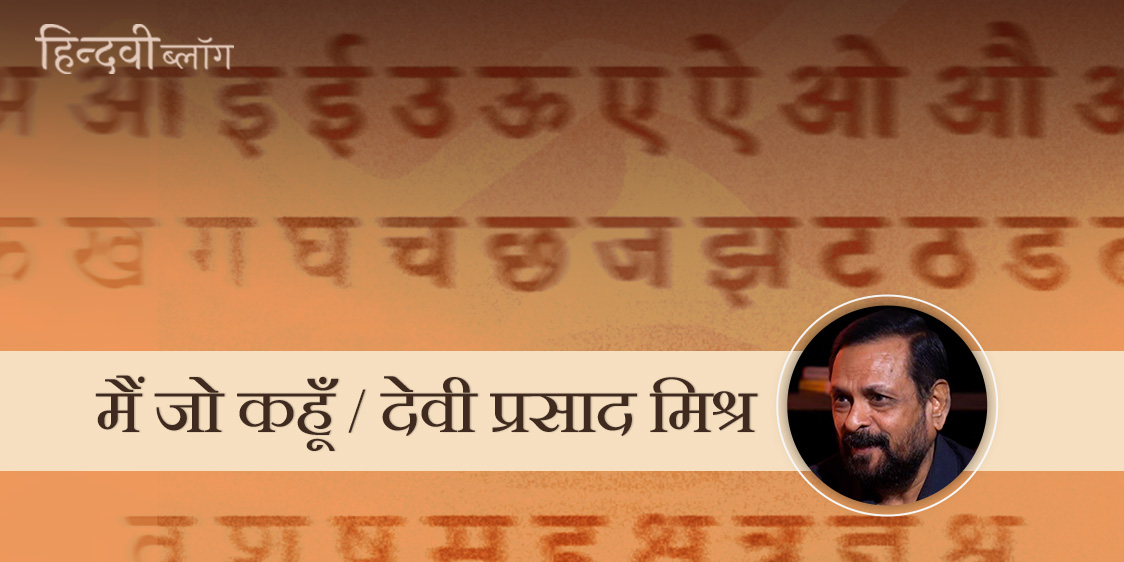
हिंसा ही नहीं है हिंदी
 देवी प्रसाद मिश्र
जुलाई 22, 2022
देवी प्रसाद मिश्र
जुलाई 22, 2022
हिंदी एक विचारधारा है और यह विचारधारा पुनरुत्थानवादी और सांप्रदायिक है जो किसी प्रतिगामी हिंदी राष्ट्रवाद से अभिज्ञापित की जा सकती है।
भाषा एक विचारधारा हो सकती है, यह एक नया विचार है। इस तरह से देखें तो अँग्रेज़ी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की भाषा है। ज़ाहिर है : अँग्रेज़ी यदि आधिपत्य के विमर्शों में प्रयुक्त हुई तो इस भाषा में ही प्रतिकार और प्रबोध का अप्रतिम ज्ञान भी संभव बनाया गया। फ़्रांसीसी को हम सभी संस्कृति भाषा का पर्याय भले ही मानते हों, फ़्रांस की धुर दक्षिणपंथी मरीन ल पेन की अंध राष्ट्रवादी और आव्रजन विरोधी विषाक्त बातें चेक या सर्ब में नहीं, फ़्रांसीसी में ही कही जाती रही हैं। एरडोगॉन का राष्ट्रवाद और ओरहन पामुक के निर्बंधता का गौरवगान करने वाले उपन्यास एक ही भाषिक लैंडस्केप में हैं जो तुर्की है।
इस बात का ज़िक्र मैं एक और आलेख में कर चुका हूँ कि ‘विस्मृति’ नाम की फिल्म में एक बूढ़ी होती स्री किसी अलग-थलग पड़े द्वीप में इसलिए रहने लगी है कि वह उस भाषा को नहीं बोलना चाहती जो नस्लवादी वर्चस्व की भाषा है, जो यंत्रणा-शिविरों की भाषा है, जो व्यापक और सामूहिक नरसंहार की भाषा है। वह पूरी जर्मन जाति की तरफ से पश्चाताप कर रही है। लोककथा सरीखी इस तरह की अकर्मक पस्ती और एकांतवास का मानवीय और रूपकात्मक मूल्य है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दिक़्क़त यह है कि नात्सीवाद का सिद्धांतीकरण और उसका बर्बर क्रियान्वन यदि जर्मन भाषा में किया गया तो मनुष्यों की मुक्ति के कितने ही बड़े विचार भी इसी भाषा में व्यक्त किए गए। अब न रहे कवि मंगलेश डबराल ने इस बात पर गहरी चिंता और किसी निरुपायता को छूता अवसाद व्यक्त किया था कि हमारी संघर्ष भाषा हिंदी का अपहरण बेहद प्रतिगामी मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है। हाल में कितने ही शब्दों जिनसे सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम लिया जाता था असंसदीय करार दिया गया है।
कौन नहीं जानता कि समय के विभिन्न चरणों और दौरों में एक ही भाषा अत्यंत प्रगतिशील और धुर प्रतिगामी विचारों की संवाहिका हो सकती है। ऐसा भी होता है कि एक साथ कितनी ही भाव-धाराएँ एक भाषा में सचल और सक्रिय रहती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस समय हिंदी को घृणा-भाषा के तौर पर प्रभूत तरीक़े से इस्तेमाल किया जा रहा है। वह बाँटने का उपकरण बन गई है। उसे अनाधुनिकता के वितरण और विस्तार के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। उसे ज्ञान विरुद्ध अंधता का एजेंट बना दिया गया है। लेकिन क्या इस आधार पर उसकी यह ब्रांडिंग ठीक होगी कि हिंदी मूलतः घृणा के प्रत्ययन और क्रियात्मकता की भाषा है। तब तो इस समय लिखी जाती हिंदी कविता की परिघटना को किस तरह से मूल्यांकित किया जाए जो प्रतिरोध और प्रतिकार की अपूर्व मिसाल है। दलित प्रश्न और स्री प्रश्न इसी भाषा में उठाए जा रहे हैं। चिंतक और विचारक ही नहीं सामान्य लोग भी इस भाषा का ऊर्ध्वगामी और बदलाव कामी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी भाषा में अभी डेढ़ साल पहले तक पहल निकली जो हिंदी की प्रकट-अप्रकट बौद्धिक और वैचारिक सचेतनता को संभव बनाती रही थी।
हिंदी जिस समाज की भाषा है, वह कितने ही संस्तरों का समानांतर समाज है और इसलिए एक गतिशील और गवेषणाशील समाज भी है; अगर उसमें बहुत कुछ विगलित, क्षयिष्णु और अंधकारमय दिखता हो। वह लालसा का समाज है तो ललक और अग्रगामिता का समाज भी है, जहाँ पुनर्प्रत्ययन की कितनी ही अलक्षित-लक्षित कारगुज़ारियाँ संपन्न की जा रही हैं।
हिंदुत्व की तर्ज़ पर ‘हिंदीत्व’ जैसा पद गढ़ना और उसे अंधराष्ट्रवाद का पर्याय मानना या अपराध-भाषा या घृणा-भाषा में घटित कर देना ग़ैरज़िम्मेदार काम-काज है। यह भाषा और समाज के बीच के जटिल रिश्ते की अनदेखी करना है—एक उथली सूझ को सिद्धांतीकृत करने का व्यामोह पालना भर है।
हिंदी की लानत-मलामत समकालीन सांस्कृतिक इतिहास का पेचीदा अध्याय रहा है। बांग्ला वाले हिदी को पता नहीं कब से संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि इसमें कुछ काम का काम हुआ भी है या नहीं। हिंदी के प्रति बांग्ला हिक़ारत किंवदंती का हिस्सा हो चली है। तमिलभाषी हिंदी को सांस्कृतिक हिंसा का पर्याय मानते हैं और अँग्रेज़ी के लिए अपनी भीड़वादी वफ़ादारी को औपनिवेशिक ग़ुलामियत का लक्षण देखने से इंकार करते हैं।
पूरी हिंदी को हिंदू सांप्रदायिकता का परचम बनाना हिंदी को मीडियाकर संस्कृति और मीडियाकर भाषा मानने की इस अवमानना से पैदा होता है कि प्रेमचंद और मुक्तिबोध की रचनात्मकता को संभव बनाने वाली भाषा होने के बावजूद इस ज़बान में है तो कोई बुनियादी कमी।
कमियाँ उत्तर भारत के समाज में हैं जो नवजागरण को संभव बनाने वाली किसी भी यात्रा का हमसफ़र नहीं हो सका। कमी जातिवादी और वर्णपोषित समाज में है। कमी उत्तर भारत के स्त्रीविरोध में है। कमी अंतःकरण के अनात्मीकरण और निर्बुद्धिकरण में है। लेकिन इसी हिंदी भारत में लेखक, कवि, विचारक और प्रतिरोध करने वाले भी मर-खप रहे हैं। हिंदी का इस्तेमाल यदि ब्राह्मणवादी और मंदिरवादी और यथास्थितिवादी कर रहे हैं तो यही हिंदी बदलावकारी और सिविल सोसायटी के काम आ रही है। इसलिए हिंदी को केवल सांप्रदायिकता और विभाजन और विग्रह की ज़बान मानना सांस्कृतिक-सामाजिक शक्तियों की मीमांसा से किनाराकशी करके कोई सामान्यीकृत निर्णय दे देना है। पलड़ा बेशक इस समय पुनरुत्थानवादियों का भारी हो, हिंदी में अभिव्यक्त होते दलित उभार, परालैंगिक आग्रहों, लिबरल और सिविल सोसायटी की आवाजों को न सुनना बौद्धिक उदासीनता की सूचना देता है ।
जैसा कि कहा गया हिंदुत्व के वज़्न पर ‘हिंदीत्व’ जैसा पद गढ़ना चौंकाने की कोशिश भर जान पड़ती है। यह दमनकारी सत्ता से स्तब्ध होना है और उससे जनित निष्क्रियता की हडबड़ी में ख़ुद को किसी निरुपाय अवधारणा के हवाले कर देना है। यह आत्मसमर्पण है कि हिंदी बस प्रतिगामिता की ही भाषा है और हम प्रतिपक्ष में बैठे इसका क्रियाशील और उन्नयनकारी प्रयोग करने में समर्थ नहीं रहे। यह कुछ ऐसा है कि लड़ने वाला अपना हथियार ही प्रतिपक्षियों के हवाले कर दे। इसका निहितार्थ यह भी है कि अब सिविल सोसायटी की लड़ाई केवल अँग्रेज़ी और अँग्रेज़ीपरस्तों के क्लबों द्वारा ही लड़ी जाएगी, जबकि सच यह है कि लड़ने-भिड़ने और गुहार-पुकार लगाने का और जनतंत्र को बहाल करने का मूल्यवान और जनोन्मुखी कारोबार हिंदी वाले तमाम गाँव-क़स्बों और नगरों में हिंदी में कर रहे हैं—यह अगर हिंदीत्व है भी तो यह एक आत्मवान् और मनुष्योन्मुख भाषा का औदार्य और औदात्य है जो किसी भी अंधराष्ट्रवाद या संकीर्णता के अँधेरे में न बुझती रौशनी है।






