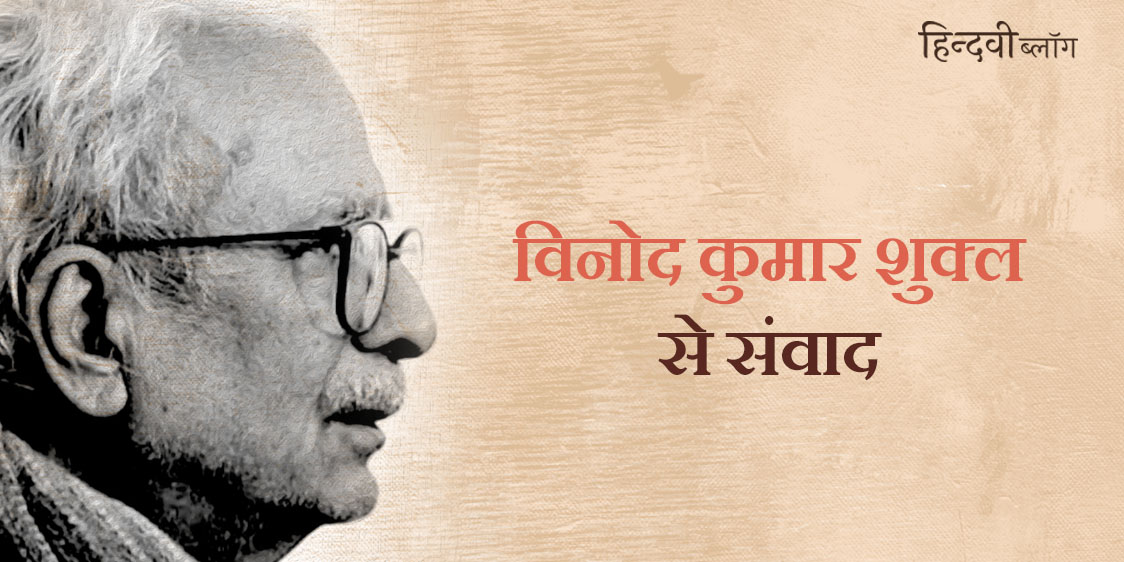
‘मैं अपने लिखे में हर जगह उपस्थित हूँ’
विनोद कुमार शुक्ल से महेश वर्मा की बातचीत
 हिन्दवी
मार्च 9, 2021
हिन्दवी
मार्च 9, 2021
स्मृति
स्मृति को मैं जीने के अनुभव के ख़ज़ाने की तरह मानता हूँ, आगे की ज़िंदगी ख़र्च करने के लिए इसकी ज़रूरत है। अगर भूलने से काम रुकता है, तो परेशानी होती है। जैसे चावल ख़रीदने घर से निकले, दुकान पहुँचे तो मालूम हुआ जेब में पैसे नहीं हैं। रचनात्मकता में भूलना सहूलत है।
जब नया लिखते हैं तो अपना पहले का लिखा भूल जाते हैं। दूसरों का लिखा हुआ भी भूला रहता है। भूलना छलनी है, आपकी मौलिकता को बचाए रखने में। भूलना रचनात्मकता का कवच है। इसमें बीती रचनाओं और दूसरों का प्रभाव उतना घातक नहीं होता।
मुझे ख़राब बीता हुआ अधिक याद आता है। ग़लतियाँ याद आती हैं। टूटा हुआ याद आता है, टूटने के पहले जो साबुत था, वह उतना नहीं। बचपन बहुत याद आता है। अम्मा को जितना सुख देना था, नहीं दे सका। परिवार क लोगों के साथ घर से बाहर का घूमना-फिरना मुझसे बहुत कम हुआ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम देखा और दुहराव की ज़िंदगी जी।
नींद और सपने
नींद नहीं आती। थक कर बार-बार लेटता हूँ। कुर्सी पर बैठने में तो झपकी आती है, लेटने से झपकी भी नहीं आती। कंप्यूटर में लिखना बंद हो गया। हाथ से लिखना भी कम हुआ। बोलकर लिखना बचा हुआ है।
रात में सोचता हूँ तो लगता है कि नींद में सपना देख रहा हूँ। और जब सपना देखता हूँ तो लगता है सोच रहा हूँ।
एक सपना मुझे कुछ वर्ष पहले बहुत आता था कि मैं उड़ रहा हूँ। मुझे उड़ना आता है। मैं उड़कर कहीं भी चला जाता हूँ। इसके बाद जो सपन आया, वह भटकने का सपना था कि मैं नंगे पैर पैदल किसी का घर ढूँढ़ते हुए भटक रहा हूँ। इत्तफ़ाक़ से जब आधे-एक घंटे की नींद आती है, तो डरावने सपने देखता हूँ। तब ख़ुद नींद में बचता हूँ।
कविता और उपन्यास
कविता लिखते समय कि कविता लिखनी है, तब कविता लिखना मेरे लिए बहुत कठिन है। उपन्यास लिखते समय मैं आसानी से कविता लिख पाता हूँ। उपन्यास लिखना उपन्यास के साथ-साथ कविता लिखना भी है।
लिखना एक लगातार यात्रा की तरह है कि यह ख़त्म नहीं होगी, परंतु प्रत्येक रचना अपने आपमें एक अधूरी यात्रा होती है। लिखना निकल पड़े की यात्रा है, जिसमें उसी जगह लौटना नहीं होता।
प्रत्येक रचना यात्रा की एक जगह होती है, जिसमें बीते अनुभव के जाने-पहचाने दृश्य भी होते हैं।
एक रचना की यात्रा के बाद सुस्ताना अच्छा लगता है। इस यात्रा में हम सब कुछ नहीं देख पाते, जैसे सब कुछ लिख नहीं पाते। जिसे देखा जाना है, उसे देखते हैं और जानबूझकर अनदेखा जैसा छूटता रहता है।
‘खिलेगा तो देखेंगे’ उपन्यास का लिखना अच्छा लगा था, क्यों अच्छा लगा था मालूम नहीं। लिख लेने के काफ़ी दिनों बाद जो कुछ भी लिखा जाता है, वह फिर अच्छा नहीं लगता और अपने संतोष का कोई मायने नहीं होता।
आलोचना की पहरेदारी से बचकर भी ज़्यादातर रचनाएँ आख़िर स्वतंत्र होकर पाठकों तक तो पहुँच जाती हैं। और जिन गिनी-चुनी रचनाओं को आलोचक पीठ थपथपाकर आगे बढ़ाते हैं, वे अलग गिने-चुने पाठक होते हैं। पाठकों को सोचकर मैंने कभी रचना नहीं की, जो लिख सकता था वही लिखा।
सिनेमा
बचपन में सिनेमा का गहरा प्रभाव पड़ता है। घर के ठीक सामने सिनेमा घर भा। और यह एक दूसरे घर की तरह था। मैं अपने घर से भागकर इस दूसरे घर में ही छुटकारा पाता था। सेकंड-शो का एक-एक डायलॉग घर में सुनाई देता था। घर की मुश्किलों और भावुकता के समय होने वाली घटनाएँ और फुसफुसाहट, चिल्लाकर बातचीत मुझे सिनेमा के डायलॉग की तरह लगती थी।
फ़िल्मों के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। अब थिएटर में सिनेमा नहीं देखता। आधा एक घंटा कभी टी.वी. देखता हूँ तो पाँच-सात मिनट के टुकड़ों-टुकड़ों में, वह भी रोज़ नहीं। टी.वी. जब ख़राब होती है तो दो-तीन साल तक घर में बनवाने की याद भी नहीं आती।
कई बार लगा कि मैंने ‘नौकर की क़मीज़’ के एक-दो दृश्य कहीं मणि कौल की फ़िल्म देखकर तो नहीं लिए। आश्चर्य अधिक था देखने में—अपने लिखे को मणि कौल की दृष्टि से। जबकि उपन्यास पर फ़िल्म वर्षों बाद बनी।
लिखा हुआ देखे में कहीं-कहीं समानार्थी होता है। कई बार इतना समानार्थी भी कि आईने में लिखे हुए दृश्य का प्रतिबिंब देख रहे हैं। और हम अपना देखा हुआ ही लिखते हैं। ‘नौकर की क़मीज़’ को लिखा हुआ देख भी लिया, पर जो देखा वह मणि कौल की रचना थी, मेरी नहीं।
पात्र
मेरे लिखे हुए पात्र ज़्यादातर मेरे देखे हुए जाने-पहचाने हैं। इसके अलावा जो पात्र हैं वे, जिन्हें देखने की आशा करता था। और मैं अपने लिखे में हर जगह उपस्थित हूँ।
~•~
विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के अत्यंत समादृत कवि-उपन्यासकार हैं। महेश वर्मा सुपरिचित हिंदी कवि और कलाकार हैं।






