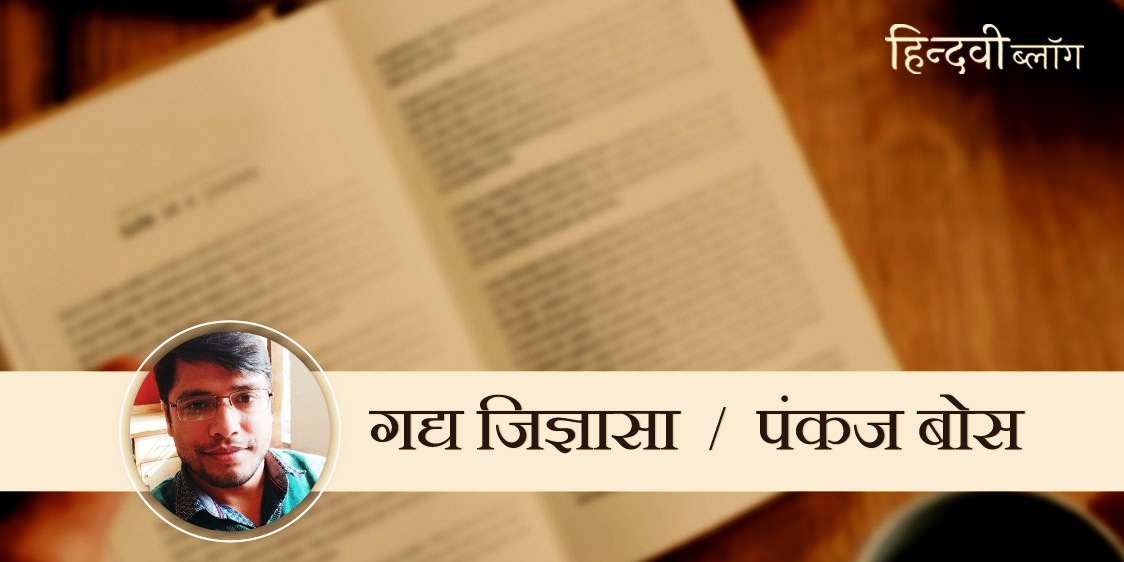
सही नाम से पुकारने की कला
 पंकज बोस
जनवरी 17, 2021
पंकज बोस
जनवरी 17, 2021
क्या लिखते हुए हम चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारते हैं? चाहे गद्य हो या कविता—यह प्रश्न आत्ममंथन की माँग करता है। साहित्य में शब्द की ‘सत्ता’ और उसकी ‘संज्ञा’ की बराबर भूमिका होती है। जब टॉमस मान ने यह कहा होगा कि “लिखना एक सक्रिय किस्म की उम्मीद है” तो उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि इस उम्मीद को पूरा करने के लिए ‘सत्ता’ और ‘संज्ञा’ में साहचर्य ज़रूरी है। कोई फूल जब ईश्वर को अर्पित किया जाता है तो ‘अर्घ्य’ हो जाता है; किसी मृत सैनिक के शव पर चढ़ाते हुए ‘श्रद्धांजलि’ की वस्तु और प्रेमी-प्रेमिका के बीच आदान-प्रदान के कारण ‘शृंगार’ का उपादान। एक फूल की अनेक अर्थच्छवियाँ वास्तव में एक ही ‘संज्ञा’ का अनेक संदर्भों में उपयोग है। इसके विपरीत, कभी-कभी एक ही वस्तु की अनेक संज्ञाओं में भी अर्थ-वैविध्य होता है। ‘फुहार’, ‘दौंगरा’, ‘रिमझिम’, ‘बारिश’, ‘मूसलाधार’, और ‘झंझावात’ वस्तुतः एक ही मूल अनुभव की अलग-अलग संज्ञाएँ हैं। अच्छा गद्य लिखने की एक पहचान है : एक शब्द का भिन्न संदर्भों में उचित उपयोग, और एक ही मूल के सहयोगी शब्दों का प्रसंगानुसार प्रयोग। यह शब्द-विवेक की कसौटी है। किसी विश्लेषण में, जो भी शब्द ध्यान में आ जाए, उसी को लिख देना शब्द-ज्ञान तो हो सकता है, शब्द-विवेक नहीं। इसलिए महाभाष्यकार पतंजलि ने ‘एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः’ की बात की थी। बीसवीं शताब्दी में उपन्यासों का विवेचन करते हुए रैल्फ फॉक्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा था : “अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की विलुप्त कला है।” क्या हम रैल्फ़ फ़ॉक्स की ‘सीख’ से टॉमस मान की ‘उम्मीद’ का अर्थ समझ सकते हैं!
संयोगवश हमारे साहित्य में कुछ ऐसे रचनाकार हैं, जिन्हें पढ़ते हुए गद्य की इस विलुप्त कला का सुखद अनुभव होता है। मिसाल के तौर पर निर्मल वर्मा। फ़िलहाल हम कथा या निबंध विधा से अलग उनकी डायरी ‘धुंध से उठती धुन’ से उदाहरण लेंगे। यों तो हर लेखक अपने तईं गद्य की इस विलुप्त कला की खोज में लगा रहता है, लेकिन निर्मल की यह खोज दुर्लभ है। चाहे उनकी वैचारिकी हो या उनके लेखक का निजी स्पेस; चाहे रचना-प्रक्रिया, जीवन, मृत्यु, समय, अनुभव और स्मृति से संबंधित चिंतन हो या प्रकृति या प्राणियों से समन्वित दृश्य-जगत का पर्यवेक्षण—सबमें ‘चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने’ की सरल किंतु एक सूक्ष्म पद्धति दिखलाई पड़ती है।
निर्मल वर्मा को आप बिल्कुल तात्कालिक या ‘इंस्टेंट’ रूप में नहीं पढ़ सकते। क्योंकि उन्हें कहीं से भी पढ़ना शुरू करें, ‘इंटेंसिटी’ का एक विद्युत्प्रवाह धमनियों में दौड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको ठहर कर समय देना होगा। उन्हें पढ़ने का मतलब है—अपने समय को ठहरा देना या एक ठहरे हुए समय में पढ़ना। अपने देशकाल की सत्ता भूल जाना और पढ़ने के बाद अपने को किसी दूसरी दुनिया में पाना। ‘धुंध से उठती धुन’ या उनकी कोई भी किताब निथरे हुए पानी के एक सान्द्र जलाशय की तरह है, जिसे आप मुग्ध होकर देर तक निहारते रहते हैं। एकबारगी उसे ‘डिस्टर्ब’ नहीं करना चाहते। पढ़ना शुरू करना मानो धीरे-धीरे किसी तालाब में उतरना। और पढ़ते हुए किसी पंक्ति पर ठहरना मानो उस तालाब में एक कंकड़ फेंक देना। यदि आपने एक भी कंकड़ फेंका तो उससे जलाशय में नहीं, भीतर आपके अस्तित्व में कंपन होगा; एक वलय बनना शुरू होगा। निर्मल वर्मा को पढ़ना अपनी ही आत्मा के तालाब में उतरने जैसा है।
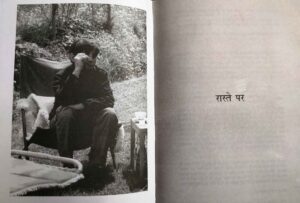
‘धुंध से उठती धुन’ से
‘धुंध से उठती धुन’ में क्षण-विशेष या काल-विशेष के ताज़े टटके अनुभवों को उसी रूप में दर्ज किया गया है जिस रूप में वे घटित हुई हैं। ‘शिमला : 12 जून, 1973’ या ‘पचमढ़ी : 14 अप्रैल, 1988’ जैसे शीर्षकों में किसी न किसी स्थान का नाम तो है ही, समय भी है—शीर्षक के साथ या शीर्षक की वस्तु में। यों केवल उल्लेख में ही नहीं, प्रत्येक डायरी की परिधि और विस्तार में भी स्थान और समय, या व्यापक अर्थों में देश और काल संघनित होकर आ गया है। जैसे एक जगह किसी झील के वर्णन में उसके चारों ओर नए-पुराने होटलों की चर्चा। सभी होटल ‘लेक व्यू’ का दावा करते हैं : यानी अलग-अलग कोण से एक ही स्थान के अलग-अलग ‘व्यू’। कुछ पुराने होटल भी आधुनिक स्थापत्य शैली के कारण अपने नये ‘लुक’ में आकर्षित कर रहे हैं। निर्मल वर्मा पुराने को नया या बासी को ताज़ा करने की—वहाँ के देशकाल की—प्रवृत्ति को उसी रूप में दर्ज करते हैं। इसलिए डायरी की पुरानी तिथियाँ आज भी उतनी ही नई लगती हैं, जितनी लिखते समय रही होंगी। पुरानी वस्तुओं में नयापन देखना या स्थान के पुरानेपन को विवरण की नवीनता देना भी उसे सही नाम से पुकारने की कला है। ‘नवनवोन्मेषशालिनी’ कला। जैसे बढ़ई अपने औज़ार से लकड़ी के कुंदे को तब तक छीलता है, जब तक उसकी परिकल्पना के अनुसार वह फिर से नया न हो जाए। इस प्रक्रिया में पुरानी लकड़ी का नामकरण भी बदलता है और अंतःकरण भी। बढ़ई अपने काम में ‘विलुप्त कला’ का संधान करता है। लेखक भी करता है—वस्तुओं के नामकरण के साथ-साथ अंतःकरण का संधान। पुराने होटल अलग-अलग समय के स्मारक हैं, वे उन्हें बनाने वाले कारीगरों के हस्ताक्षर हैं। लेकिन उन सबके बीच ‘झील’ सबसे पुराने समय की प्रतिनिधि है। वह समय जो अब ‘स्पेस’ में बदल गया है—वहाँ का ‘लैंडमार्क’ हो गया है। इसी तरह लेखक के देखे हुए अलग-अलग स्थान अब अलग-अलग तिथियों (समय) के ‘लैंडमार्क’ हो गए हैं।
एक जगह वह जर्मन की तुलना में फ़्रांसीसी चिंतकों की “साफ़-सुथरी तर्क-पद्धति” से आकर्षित होने की वजह बताते हैं : “वे अमूर्त से अमूर्त विचारों को जीवंत और उज्ज्वल आवेगों (Passions) में अनूदित कर सकते हैं। उनकी सैद्धांतिक अवधारणाएँ भी काव्यात्मक अंतर्दृष्टि से छन कर बाहर आती हैं—मांसल, तात्कालिक और पारदर्शी… फ़्रांसीसी स्वभाव से रूपकों में सोचता है—विचार और आवेग के बीच रूपक एक सेतु की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ एक की ठूँठ अमूर्तता दूसरे छोर पर जाकर सेंसुअल भाव में घुल जाती है। उनकी कल्पना-शक्ति एक इमेज के द्वारा आकस्मिक छलाँग लगाती है, जिससे तर्क का समूचा लैंडस्केप आलोकित हो उठता है।” निर्मल की निगाह में यह चीज़ों को सही नाम से पुकारने की फ़्रांसीसी कला है।
क्या चीज़ों को सही नाम से पुकारने की कला केवल उनके नामकरण में दिखती है? क्या किसी कृति को ‘गोरा’, ‘ग़बन’, ‘मृत्युंजय’ या ‘संस्कार’ जैसा नाम दे देना ही सचमुच इस कला का निर्वाह है? नहीं। नामकरण संस्कार कृति के रचे जाने के पहले हो या बाद, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता—लेकिन क्या हम ‘जस्टिफ़ाई’ कर पाते हैं कि वह नाम इतना विशिष्ट या प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि नामकरण से आगे बढ़ कर यह ‘विश्लेषण’ का काम है। नाम-धर्म का विश्लेषण। यहाँ ‘धर्म’ महत्त्वपूर्ण है। नई कविता के दौर में जब लगभग सारे कवि और आलोचक ‘कवि-कर्म’ की व्याख्या एक विशिष्ट पद के रूप में कर रहे थे तो रघुवीर सहाय ने ‘सीढ़ियों पर धूप में’ में ‘कवि-धर्म’ शब्द का प्रयोग किया। ज़ाहिर है कि अनेकानेक धाराओं के बीच रहते हुए भी देखने-सोचने के अलग तरीक़ों से विश्लेषण का कोई नया पद जोड़ा जा सकता है। नामकरण-संस्कार से कहीं अधिक ज़रूरी है विश्लेषण का संस्कार या परिष्कार। वैसा परिष्कार जिसके बाद एक पारदर्शिता पाई जा सके—जिसकी काँच में अपने विचार साफ़-साफ़ देखे जा सकें। यदि उस पर धूल जमा हो तो उसे फिर पोंछा जा सकें। रचनाकार यही काम करता है। हमारी चेतना के दर्पण पर जमी हुई धूल की परतों को खुरचता है।
निर्मल की एक ख़ूबी यह है कि वह जब किसी ‘शब्द’ को अपनी ओर से कोई संज्ञा नहीं देते तो उसे अपना कोई अनुभव दे देते हैं : “मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं है, फिर भी न जाने कैसे एक विचित्र स्नेहिल-सी कोमलता मेरे अस्तित्व के गहनतम तल में भाप-सी उठने लगती है, जब मैं अपने लेखन में कभी ‘ईश्वर’ का नाम लिखता हूँ।” इस पंक्ति में ‘ईश्वर’ का कोई नया नाम नहीं है, लेकिन पाठक के लिए ‘अनुभव’ की रोशनी में हिलते-डुलते ‘ईश्वर’ शब्द को पकड़ना एक नया काम है। ध्वनि यह है कि निर्मल के गद्य में कभी अनुभव को नाम और कभी नाम को अनुभव देने का धूपछाँही खेल लगातार चलता रहता है।
कभी-कभी वह सीधा और सपाट नाम नहीं लेते, बल्कि उसकी एक सही व्याख्या कर देते हैं। जैसे : “मेरे लिए ‘सफलता’ एक ऐसे खिलौने की तरह है, जिसे एक अजनबी किसी बच्चे को देता है, इससे पहले कि वह उसे स्वीकार करे, उसकी नज़र अपने माँ-बाप पर जाती है और वह अपने हाथ पीछे खींच लेता है।” कभी प्रथम पुरुष में ही ‘मैं’ की जगह ‘वह’ का प्रयोग करना और वर्णन को सहसा अपने से अलग कर वस्तुपरक बना देना : “और वह किताब से सिर उठाता है।” यहाँ लेखक अपने लिए ही ‘वह’ का प्रयोग कर रहा है। ऐसे प्रयोगों के बावजूद गद्य के इस खेल से हम चमत्कृत नहीं होते, बल्कि उसकी सहजता से प्रभावित होते हैं। गद्य में केवल चमत्कार पैदा करने की मंशा रखने वाले लेखकों को पढ़ते हुए हम एक बिंदु से टकरा कर वापस लौट आते हैं, लेकिन सर्जक लेखकों के यहाँ गद्य की त्वचा के भीतर प्रवेश करते हैं।
निर्मल वर्मा ने कहीं-कहीं अपने लिखे हुए में कुछ जोड़ा है और बताया है कि बीस साल बाद वह यह जोड़ रहे हैं। यह अपने लेखन में एक ‘वैल्यू एडिशन’ करना है। रचनाओं का संस्कार या परिष्कार संपादक तो करते ही हैं, लेकिन हर बड़ा लेखक पहले अपना संपादक ख़ुद होता है। वह केवल किताब के पन्ने या प्रूफ़ नहीं, अपने ‘विज़न’ को भी संस्कारित करता है। अपनी दृष्टि को परिष्कृत करते हुए एक मूल्य अर्जित करता है। जब कोई लेखक लिखता है, “आधुनिकता एक मूल्य है; नहीं, मूल्य के प्रति एक दृष्टि है” तो एक साथ ही वह टेक्स्ट को, और अपने ‘विज़न’ को संपादित करते हुए लिखता है। जिस तरह पन्नों के हाशिए पर या कंप्यूटर पर कोई संपादन होता है, वैसा ही एक संपादन हमारे अंतर्मन के हाशिए पर भी चलता रहता है। यह आत्म-संपादन वास्तव में आत्म-मूल्यांकन की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। और हमारी विनम्रता की पहली सीढ़ी भी यही है—भाषा और तेवर में विनम्रता, जो हमारे कथ्य को अकाट्य बनाती है। इसकी एक बड़ी मिसाल है घास, जो झंझावातों में भी अपना अस्तित्व बचा कर रख सकती है। बाँस की तरह टूट नहीं सकती। एक ही प्रजाति के दो पादप की प्रकृति कितनी भिन्न है! दो लेखक भी एक मनुष्य प्रजाति के सदस्य होते हैं, लेकिन कितने भिन्न! इस भिन्नता को समझने के लिए उनके संपादन और परिष्कार को पहले समझना होगा। यहाँ यह ध्वनि है कि कोई भी लेखक कभी भी अपने आपमें एक बेहतर लेखक की संभावनाओं को प्रकट कर सकता है।
लेखक की अपनी संभावनाओं या मौलिकता के बारे में एक जगह निर्मल लिखते हैं : “हर छोटा लेखक मौलिक होने की चेष्टा करता है, जहाँ वह अपने पूर्ववर्ती लेखकों से अलग कुछ लिख सके… किंतु जो सही अर्थों में ‘मौलिक’ होता है; वह हमेशा अपने प्रिय, महान लेखकों की नक़ल करना चाहता है—किंतु लिखने की घड़ी में वे महान लेखक विनयशील, शालीन मित्रों की तरह उससे विदा ले लेते हैं और उसे अकेले कमरे में छोड़ देते हैं—जो उसका नरक है—और मौलिकता का उद्गम स्रोत भी।” अक्सर किसी लेखक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे थे, उसने उसका बेहतर बयान कर दिया है। पढ़ते हुए उस बिंदु पर हमारा सोचना, और सोचे हुए को पा लेना, हमारे आस्वाद के अनुभव का क्षण होता है। जैसे किसी फ़िल्म को देखते हुए स्क्रीन पर भागते चित्रों के साथ हम भी गतिशील होते हैं और अनुमान लगाते हैं। अगले ही पल जब अनुमानित घटित होता है तो लगता है कि हमने कला के मर्म को या आस्वाद-क्षण को पकड़ लिया है। ऐसा ही किसी उपन्यास को पढ़ते हुए हो सकता है। यह विलुप्त कला का हमारा अपना संधान है, जिसे हम अलग-अलग माध्यमों में ढूँढ़ते हैं—चित्र में, दृश्य में, कविता या गद्य में। जिस रचनाकार ने हमारे भीतर यह एहसास जगाया, उसने कला के एक बुनियादी सत्य को पा लिया—मानवीय सहानुभूति का सत्य, अनुभवसाम्यता का सत्य। निर्मल जैसे लेखकों को पढ़ते हुए हम इस सत्य के सम्मुख होते हैं। अक्षय ऊर्जा-स्रोत की तरह ऐसा गद्य हर बार पढ़े जाने पर अपने पुनर्नवा रूप में मिलता है।
यही है जिज्ञासा, जिससे हम कहानियाँ सुनते हैं; कविताएँ पढ़ते हैं या कोई भारी-भरकम उपन्यास चट कर डालते हैं। जिस जिज्ञासा से हम देखते, सुनते या पढ़ते हैं; उसी की ‘रिवर्स’ प्रक्रिया से हम अपना देखना, सुनना या लिखना भी शुरू करते हैं। कुछ लिखते हुए किसी ज्ञात या अज्ञात की ललक होती है जिसका हम लगातार पीछा करते हैं। हम प्यासे भटकते हैं कि कहीं संतुष्टि मिल जाए, कहीं कोई सिरा पकड़ में आए, कहीं कोई ऐसी बात हो जो जँच जाए। कोई ऐसा हो कि पढ़े तो फिर से प्यासा हो जाए। हम परस्पर प्यास में संचरण करते हैं। एक प्यास को हम महसूस करते हैं—जब हम पाठक होते हैं : इसे कोई और भी महसूस करेगा—जब वह पाठक होगा।
~•~
पंकज बोस हिंदी की नई पीढ़ी के अत्यंत मेधावी आलोचक हैं। ‘हिन्दवी’ के लिए वह पाक्षिक स्तंभ ‘गद्य जिज्ञासा’ के अंतर्गत देश-विदेश के चुनिंदा रचनाकारों के बहाने साहित्य के सौंदर्य और सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। यहाँ प्रस्तुत स्तंभ में निर्मल वर्मा के सभी उद्धरण उनकी पुस्तक ‘धुंध से उठती धुन’ (वाणी प्रकाशन, संस्करण : 2018) से लिए गए हैं।






