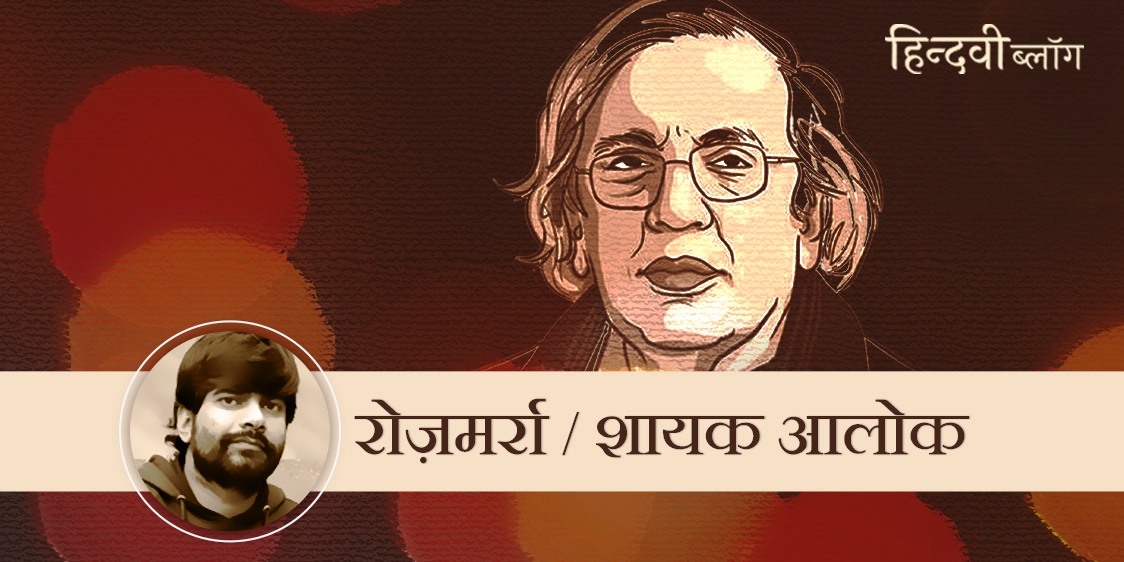
विलग उपस्थिति का ‘कभी-कभार’
अशोक वाजपेयी के मशहूर स्तंभ ‘कभी-कभार’ के बहाने उनकी सघन, बहसतलब और ज़रूरी उपस्थिति और दख़ल पर
 शायक आलोक
जनवरी 19, 2021
शायक आलोक
जनवरी 19, 2021
वह लिखेंगे—‘‘मक़बूल फ़िदा हुसेन से मुलाक़ात अचानक ही हो सकती है : तय करके मिलने के मौक़े पर वह अक्सर ग़ायब हो जाते हैं। कई महीनों पहले एक दिन काफ़ी सुबह हुसेन हमारे घर आए। वह थोड़े दिन पहले पंढरपुर गए थे जो महाराष्ट्र में है और जहाँ उनका जन्म हुआ था। जब वह एक बरस के थे तभी उनकी माँ चल बसीं और उसके बाद ही हुसेन का परिवार इंदौर चला गया था जहाँ उनके पिता को एक मिल में नौकरी मिल गई थी। हुसेन उसके बाद अब तक कभी पंढरपुर नहीं गए जो कि एक प्रख्यात मंदिर नगर है।’’
मुझे एक बार हुसेन शती वर्ष के अवसर पर अपनी और हुसेन की कविताएँ पढ़नी थीं। हुसेन की कविताएँ मैंने इंटरनेट से जुटाईं, अपनी कविताओं के लिए लैपटॉप के गोल चक्कर लगा वे कविताएँ ढूँढ़ीं जिनमें कला-पूर्वग्रह हो या वे 2014 की बाद की राजनीति पर कोई मुज़ाहिमत हो। उनके पास हुसेन हैं, मेरे नज़दीक संस्मरण के लिए हसन को चुनना हुआ। सादिया हसन मेरे कॉलेज दिनों की सहपाठी रही। वह ट्यूशन क्लास में थिन पेपर पर लिखे नोट्स हवा में लहराती और आवाज़ लगाती—सेवइयाँ ले लो, सेवइयाँ। मैंने अपने ‘कभी-कभार’ में ही कभी लिखा होगा कि ‘‘गुजरात ने हम दोनों को बदल दिया था सादिया हसन।’’
मेरी उपस्थिति इतनी प्लास्टिक रही कि विंदा करंदीकर की मेरी स्मृति इंटरनेट पर बनी स्मृति है। उनके विंदा करंदीकर ‘‘दिखने में कुछ रूखे से हैं—अँग्रेज़ी के अध्यापक रहे हैं—उनके गद्य के कुमार गंधर्व बड़े प्रशंसक थे।’’ मेरे विंदा करंदीकर ने बस एक कविता लिखी है जिसकी पहली पंक्ति हिंदी अनुवाद में ‘चोखा उजाला बोली दादी’ हुई है, जिसमें एक ही बिस्तर से उतर दादी और विंदा तितर-बितर हुए हैं, दोनों के बीच एक अशरीरी लज्जा रुनझुना गई है, दादी पूछ रही—क्या देखता है रे, क्या देखता है रे, और विंदा ने अपने कुर्ते के छोर को कुछ ज़्यादा ही लंबा कर लिया है।
कुमार गंधर्व एंग्जायटी-दिनों के साथी हैं जो गा रहे हैं—सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञाआआआनी, ज्ञानी—मैंने मुहल्ले में नए बन रहे मकान की छत पर दिखी छोटी जंगली चिड़िया की तस्वीर खींच ली है और ‘अलख निर्वाणी’ शीर्षक से फ़ेसबुक पर रख दिया है। वह बिरजू महाराज पर कुछ कह रहे हैं और मुझे उनकी ही दूसरी बात याद आ रही कि रश्मि जैन बिरजू महाराज की पहली शिष्याओं में से एक हैं, रश्मि ने ही तो एक दुनिया सँभाल रखी जो वह एक दूसरी दुनिया में कुछ सक्रियता रख पाते हैं। बेगूसराय में एक नर्तक हुए सुदामा जी। मैंने दूरदर्शन पर पहली बार बिरजू महाराज को देखा तो उन्हें सुदामा जी ही समझ लिया।
लेकिन यहीं, एक ‘कभी-कभार-सा’ लिखने के मध्य में ही ‘अनुकरण की अधीरता’ पर उनके पाठ का अपना एक तात्पर्य क्यों न तलाश लिया जाए। हम कवि, नागरिक और मनुष्य के कर्तव्य बरतने की कुछ साझा पूर्व-शर्तें अपनी पीठों पर लादे रखें तो ‘कुछ खोजते हुए’ अचानक एक दिन एक किसी जगह पर क्यों नहीं मिल पड़ेंगे?
बक़ौल उनके—‘‘बिना लक्ष्य के या किसी प्राप्ति की आशा के खोज क्यों नहीं की जा सकती? अगर यह संभव है, भले कुछ अतर्कित है तो इन पृष्ठों में जो कुछ खोजा जाता रहा है, इसका कुछ औचित्य बनता है। खोजने की प्रक्रिया में कुछ सच, कुछ सपने, कुछ रहस्य, कुछ जिज्ञासाएँ, कुछ उम्मीदें, कुछ विफलताएँ सब गुँथे हुए-से हैं। शायद कोई भी लेखक कुछ पाने के लिए नहीं खोजता : कई बार अकस्मात् अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ कुछ लग जाता है। कई बार वह कुछ, इससे पहले कि लेखक को इसका सजग बोध हो या कि वह उसे विन्यस्त कर पाए वह फिसल भी जाता है और कई बार ऐसे ग़ायब हो जाता है कि दुबारा फिर खोजे नहीं मिलता। एक साप्ताहिक स्तंभ के बहाने अपनी ऐसी ही बेढब खोज को दर्ज करता रहा हूँ। इसमें संस्मरण, यात्रा-वृत्तांत, पुस्तक और कला-समीक्षा, इधर-उधर हुए संवाद और मिल गए व्यक्तियों से बातचीत आदि सभी संक्षेप में शामिल हैं। यह उन ‘चाहियों’ में से एक है जो मुझसे नहीं सधे।’’
तब फिर विलग उपस्थिति के एक ‘कभी-कभार’ को दो टुकड़ों में यूँ दर्ज किया जाए—
किसान-आकांक्षा अब देशद्रोह है
बाहर बाहर ऐसा दिखेगा कि अधिकार के ज़मीनी आंदोलन के दो ही तरीक़े होते हैं—अहिंसक व हिंसक। सुझाव भी इन्हीं दो दिशाओं को प्रेरित और नेतृत्व भी। लेकिन यह समझ लेना चाहिए किसानों की वर्तमान आवश्यकताएँ व आकांक्षाएँ अलग हैं। उनका संघर्ष किसी विदेशी औपनिवेशिक सरकार, बिचौलियों, भूपतियों, वंशानुगत राजा से नहीं है, बल्कि अपने ही लोकतांत्रिक देश की नीतियों से है।
फिर तीन पक्ष बनते हैं। किसान, सरकार और राजनीतिक/बौद्धिक विपक्ष।
तीनों को संरेखण में आना होगा। इस संरेखण के लिए फिर विषय के बिंदु चुनने होंगे। तीन बिंदु चुन सकते हैं—ऋण का बोझ, लागत में वृद्धि, मूल्य के लिए संपूरक समर्थनकारी नीतियाँ।
यह ऐसा ऐतिहासिक समय है जहाँ पूरे देश के किसान एक-सी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के साथ एक ही ज़मीन पर खड़े हो सकते हैं। यह चंपारण, खेड़ा, मोपला, तेभागा, नक्सलबाड़ी की अलग-अलग आवश्यकताओं व अनुप्रेरणाओं से अलग स्थिति है। यह ऐसा समय भी है, जहाँ कोई भी पक्ष इस एकसमता को आज़माने और संबोधित होने को उद्यत नहीं।
मैं फिर तीन आंदोलनों की कल्पना करता हूँ। एक आंदोलन अखिल भारतीय किसान आंदोलन हो जहाँ सबके सींग और पूँछ एक दूसरे से जुड़े हों। हिंसक-अहिंसक वक़्त तय कर देगा। दूसरा आंदोलन विपक्ष का हो जो संकट से संवाद के तमाम औज़ार आज़माए और सड़क से संसद तक सरकार पर दबाव बनाए। तीसरा आंदोलन ख़ुद सरकार का हो कि अभी के लिए और हमेशा के लिए वह कोर्स करेक्शन को तैयार है। यह आंदोलन उसके अंदर घटित हो जहाँ वह मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और नीति-नवाचार का प्रदर्शन करे। किसान बजट और नए किसान क़ानून एक सकारात्मक शुरुआत हो सकते थे जो ‘स्टंट’ रह गए।
तब तक उनकी आत्महत्याएँ हैं। हत्याएँ हैं। और अब देशद्रोह है…
मेरी तत्समता मेरे तद्भव का परिष्करण थी
एक पूर्ति तो यह की जानी थी कि चूँकि कविता की यह नायिका कविता में अभी सोकर उठी है तो उसके संवाद कुछ नींद में डूबे हों। वाक्य के कुछ शब्द अस्पष्ट सुनाई पड़ते हों, कुछ अंताक्षर छूट गए हों।
एक समूचा वाक्य ही संवाद में काला रह गया हो और मैंने कविता में उसे वैसे ही रख दिया हो।
फिर उसकी हिंदी पर उसके भाषा/बोली-परिवार का असर हो। मैथिली की आँखों में अशरीरी लज्जा हो, भोजपुरी की ज़ुबाँ आवारा शब्दों पर ठिठकती न हो। बांग्ला विस्मय भर उत्पन्न कर कोलकाता नहीं लौट गई हो।
स्वयं मेरी तत्समता मेरे तद्भव का परिष्करण थी। कविता में यह बात प्रकट नहीं हो पाती थी। जिन बिंदुओं, विरामों पर मैं ठहर गया था, पाठकों के पास उनके पते न थे।
अब जो कविता मेरे सामने थी, उसमें न मैं था, न वह थी, न बात थी। आठ पंक्तियों की कविता भी मेरी कविता नहीं थी और मैं अपनी कविता लिखना चाहता था। मैंने शिकायत की कि मेरी कविता के लिए मेरी भाषा के पास टूल्स नहीं हैं।






