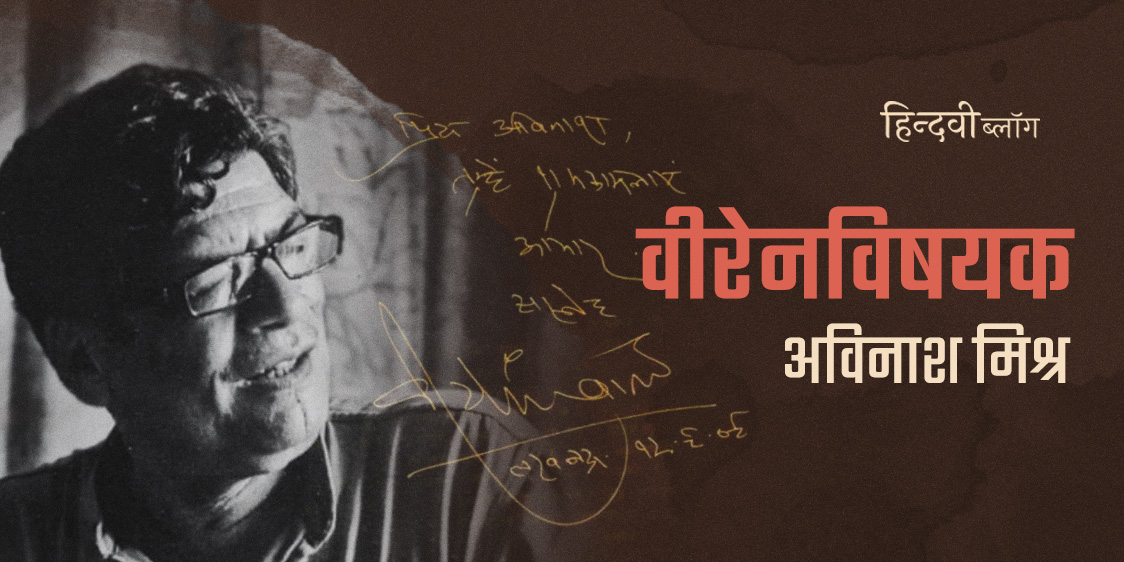
एक कवि और कर ही क्या सकता है
 अविनाश मिश्र
अगस्त 5, 2021
अविनाश मिश्र
अगस्त 5, 2021
एक अलग रास्ता पकड़ने वाले वीरेन डंगवाल (1947–2015) की आज जन्मतिथि है। हिंदी की आठवें दशक की कविता ने स्वयं को कहाँ पर रोका यह समझना हो तो मंगलेश डबराल को पढ़िए और वह कहाँ तक जा सकती थी यह समझना हो तो वीरेन डंगवाल को। इस दौर के बाक़ी सब कवि इन दो पहाड़ों के बीच बसे गाँवों की तरह हैं, जिनमें बिजली नहीं है और पानी पाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। इन गाँवों में प्रकृति की ऊब है और कविता का जीवन कोई अर्थ नहीं रखता है, जबकि जीवन की कविता भरपूर है।
‘नवारुण’ से प्रकाशित ‘कविता वीरेन’ (वीरेन डंगवाल की संपूर्ण कविताएँ) पढ़ना समकालीन हिंदी कविता की वास्तविक राजनीति और शक्ति का एहसास करना है।
वीरेन डंगवाल कभी मायूसी के पक्ष में नहीं रहे। वह कभी उस अपराधबोध के भी पक्ष में नहीं रहे जो सिर्फ़ सतह पर नज़र आता है। नई संस्कृति—जिसका पूरा स्थापत्य हिंसा पर आधारित है—वीरेन डंगवाल की कविताओं में उम्मीद को बेदख़ल नहीं होने देती। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप इस भयावह समय में भी अपनी कविता में बार-बार उम्मीद और उल्लास की तलाश कैसे कर लेते हैं? उन्होंने कहा था कि तुम मेरी छाया से मिल रहे हो, अगर मुझसे मिले होते तो यह सवाल नहीं करते प्यारे!
इस बयान में सचाई थी। मैं उनकी छाया से ही मिला था। मैं उनसे मिल पाता, इससे पहले ही वह एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके थे। मैं अपने आस-पास के परिचितों से बस यही सुनता रहा कि वीरेन डंगवाल से अगर तुम मिले होते, तब जानते कि वीरेन डंगवाल होने का क्या अर्थ है। यह बहुत कम अंतरालों में हुआ कि उन्हें लेकर मेरे आस-पास इतने सारे सनसनीख़ेज़ संस्मरण जमा हो गए कि उनसे मिलने पर मुझे भी यह लगने लगा कि मैं वीरेन डंगवाल से नहीं, उनकी छाया से मुख़ातब हूँ।
इस छाया से ही मैंने एक बार जानना चाहा था कि क्या प्रेम बीत जाता है?
उन्होंने कहा कि यह मैं कैसे बता सकता हूँ? यह तो उससे पता करो प्यारे जिसका प्रेम बीत गया हो।
मैंने कहा कि क्या आपको याद नहीं है कि मैं आपसे भी मिला हूँ?
उन्होंने कहा : ”आलोक(धन्वा) कहता है :
अब तो भूलने की भी बड़ी क़ीमत मिलती है
अब तो यही करते हैं
लालची ज़लील लोग।
मैं न तो लालची हूँ और न ज़लील, इसलिए मैं सब कुछ याद रखता हूँ।”
मैं वीरेन डंगवाल की कविता से 2005 में मिला और उनसे 2009 के सितंबर में। यह अवसर लखनऊ में आयोजित ‘जन संस्कृति मंच’ के एक तीन दिवसीय फ़िल्म समारोह का था। इस अवसर पर ही ‘हिरावल’ समूह द्वारा प्रस्तुत वीरेन डंगवाल की कविता ‘हमारा समाज’ का एक दूसरा ही असर ज़ेहन में जज़्ब हुआ था। यह असर अब भी कभी-कभी याद आता है। ‘हमारा समाज’ की पंक्तियाँ पढ़ते ही स्मृति में स्थायी हो जाने की सामर्थ्य रखती हैं।
लखनऊ में इस कविता की प्रस्तुति के अवसर पर वीरेन डंगवाल मौजूद थे। उनका तीसरा कविता-संग्रह ‘स्याही ताल’ बिल्कुल आया ही था और सभागार के बाहर बिक्री के लिए उपलब्ध था। मैंने इस संग्रह की एक प्रति ख़रीदी और इस पर वीरेन डंगवाल के दस्तख़त के बहाने उनसे मिलने की सोच ससंकोच उनकी ओर बढ़ा। वह कुछ युवाओं और कुछ युवतमों से घिरे थे। इस घेराव के किंचित कम होते ही मैं उनसे मिला और उन्हें बताया कि मैं आपकी कविता से मिलता रहता हूँ। इस पर उन्होंने कसकर मेरे हाथ को अपने हाथों से दबाया और कहा : ‘‘बस हौसला बढ़ा देते हो यार तुम लोग…।’’
इस पहली मुलाक़ात के चार साल बाद जब उनसे दूसरी बार मिलना हुआ, तब मैंने पाया कि पहली बार वाले वीरेन डंगवाल लगभग आधे हो चुके हैं। कैंसर ने उनकी देह को बहुत कमज़ोर कर दिया है। उनकी ज़िंदादिली अब बस एक आवरण भर है जिसके पन्ने पाने के लिए वह भीतर-बाहर सब तरफ़ बहुत लड़ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने कहा : ‘‘ये दुनिया बहुत नागवार लगती है, पर है बहुत सुंदर…।’’
इसके बाद भी बीच-बीच में उनसे मिलना-जुलना होता रहा। लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ नहीं पूछा—मन में उनसे एक बहुत बड़े साक्षात्कार की इच्छा होने के बावजूद। वह बीमारी की वजह से बहुत मुश्किल से बोल पाते थे। इस मुश्किल में वह सामने वाले को ज़्यादातर सुनते थे। लेकिन इस प्रकार के प्रसंगों में जब भी वह बोलते तब कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अनुभव ज़रूर देते जो सदा के लिए बहुत काम का और बहुत मार्मिक लगता।
मैंने कहीं किसी कवि के बारे में उसके ही समकालीन एक कवि का बयान पढ़ा था जिसमें उसने अपने उस दिवंगत साथी-कवि के लिए कहा था कि उसे केवल कवि बने रहने से ही संतोष नहीं था, वह मनुष्य भी बने रहना चाहता था। वीरेन डंगवाल भी ऐसे ही कवियों में से थे जिनके लिए केवल कवि होना भर पर्याप्त नहीं था, बल्कि मनुष्य बने रहना भी उनके लिए एक ज़रूरी कार्यभार था। …और इस कार्यभार ने देखिए, उनकी कविता को कैसी ऊँचाई दी है :
मैं ग्रीष्म की तेजस्विता हूँ
और गुठली जैसा
छिपा शहद का ऊष्म ताप
मैं हूँ वसंत में सुखद अकेलापन
जेब में गहरी पड़ी मूँगफली को छाँटकर
चबाता फ़ुरसत से
मैं चेकदार कपड़े की क़मीज़ हूँ
उमड़ते हुए बादल जब रगड़ खाते हैं
तब मैं उनका मुखर ग़ुस्सा हूँ
इच्छाएँ आती हैं तरह-तरह के बाने धरे
उनके पास मेरी हर ज़रूरत दर्ज है
एक फ़ेहरिस्त में मेरी हर कमज़ोरी
उन्हें यह तक मालूम है
कि कब मैं चुप होकर गर्दन लटका लूँगा
मगर फिर भी मैं जाता रहूँगा ही
हर बार भाषा को रस्से की तरह थामे
साथियों के रास्ते पर
एक कवि और कर ही क्या सकता है
सही बने रहने की कोशिश के सिवा
~•~
वीरेन डंगवाल की और कविताएँ यहाँ पढ़ें : वीरेन डंगवाल का रचना-संसार






