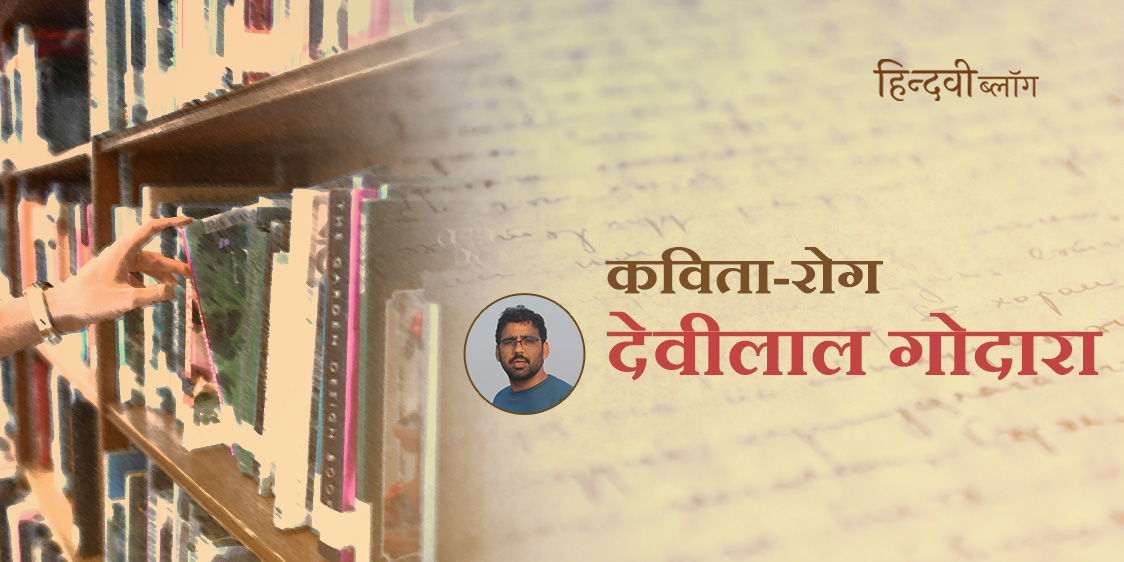
साहित्य के दरवाज़े के द्वारपाल की भूमिका में
 देवीलाल गोदारा
नवम्बर 25, 2022
देवीलाल गोदारा
नवम्बर 25, 2022
एक
‘टके सेर भाजी टके सेर खाजा’ एक लोक कहावत है जिससे हिंदी साहित्य के पाठक संभवतः भारतेंदु के नाटक ‘अंधेर नगरी’ के माध्यम से परिचित हुए (कुछ पहले भी रहे होंगे)। भारतेंदु के नाटक ‘अंधेर नगरी’ का यह केंद्रीय वाक्य है। यह संकेत है अविवेकपूर्ण कुव्यवस्था का, प्रतीक रूप में ऐसी व्यवस्था, जहाँ सोना और मिट्टी एक ही भाव हों और घोड़े-गधे एक साथ गिने जाएँ। हिंदी कविता में कविता जैसी चीज़ों की मिलावट को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि संदर्भित वाक्य ‘टके सेर भाजी…’ आज संभवतः सबसे अधिक प्रासंगिक होकर उभरा है। पूर्वाग्रह रहित आलोचना और सजग आलोचकों के अभाव में मिलावटी और रद्दी कविताएँ महामारी की तरह चहुँओर व्याप गई हैं। कविता-शास्त्र लिखने वालों ने बरसों पहले सावधान किया था कि रद्दी काव्य बहुत जल्दी प्रसार पाता है, यह एक ही दिन में दसों-दिशाओं में फैल जाता है। ऐसे रचनाकारों में नेता, प्रोफ़ेसर, अधिकारी और शोधार्थियों की संख्या अधिक है। साहित्य ही नहीं, हिंदी भाषा को भ्रष्ट करने में भी इनकी बड़ी भूमिका है। कवियों के नाम पर तुक्कड़, छंद के नाम पर तुकबंदी, सूक्ति के नाम पर सस्ते और चमत्कृत वाक्य, भावों के नाम पर नक़ली करुणा परोसी जा रही है।
चूँकि आलोचक साहित्य के दरवाज़े का द्वारपाल माना गया है, इसलिए उसका दायित्व है कि वह निर्दोष कविता को उस दुनिया में प्रवेश दे और रद्दी कविता की गर्दन पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाए। इधर आलोचना में ‘क्या बात कही है’, ‘मर्म तक पहुँचे हैं’, ‘समकालीन संदर्भों की जड़ों तक गए हैं’, ‘दलित-स्त्री संवेदना को बख़ूबी उभारा है’, ‘क्या ख़ूब लिखा है’, ‘वाह’ जैसे वाक्य-विन्यासों का बोलबाला है। लेखक (?) को आसमान पर चढ़ाने वाली उक्तियों, किसी दल-विशेष के माननीय की प्रशस्तियों, अपने पक्ष की प्रशंसाओं और विपक्ष की निंदा से ही आधुनिक आलोचना समृद्ध की जा रही है।
दो
कविता क्या है? यह ऐसा प्रश्न है जो अभी तक अनुत्तरित ही रहा है। इस प्रश्न से टकराने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई विद्वानों की लंबी सूची है। कवि केदारनाथ सिंह को इस प्रश्न पर रामचंद्र शुक्ल की मूँछें और मूँछों से झाँकती कविता दिखाई दी, परंतु प्रश्न वहाँ भी अनुत्तरित ही रहा और (मेरे तईं) यहाँ भी। ‘कविता क्या है’ की अपेक्षा मेरे लिए ‘कविता क्या नहीं है’ के बारे में कहना अधिक आसान है (जिसकी चर्चा फिर कभी)। कवि बनाया नहीं जाता, लेकिन विडंबनाजन्य स्थिति यह है कि देश की राजधानी में कविता जैसी दिखती पंक्तियाँ, चालू क़िस्म के उपन्यास और सतही इतिहास की किताबें लिखने वाले कविता की न्यूनतम समझ से भी वंचित व्यापारी काव्य-कला सिखाने की ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं। ट्यूशन पढ़कर कवि/लेखक होने की हसरत पालने वालों (जिसे एक समकालीन कवि ने ‘कविताबाज़’ कहा है) के लिए बहुत पहले ‘छंदानुशासन’, ‘कविप्रिया’, ‘पिंगल परिचय’, ‘कवि-रहस्य’, कवि-शिक्षा’, ‘कविता-कलापिनी’ जैसे सैकड़ों शास्त्र रचे गए। नहीं मालूम कि आधुनिक ‘कवि-गुरुओं’ का इन ग्रंथों से कभी परिचय हुआ भी है या नहीं, परंतु कविता और काव्य-कला के संबंध में कुछ बातें हैं जो सामान्य कविता पाठक के लिए शायद काम की हों!
तीन
भाषा को तमीज़ से बरतना कविता-कर्म की बुनियादी शर्त है। अनुचित शब्द चयन कवि और कविता दोनों के लिए प्राणहंता है। कविता में किसी शब्द का कोई बदल/पर्याय नहीं होता। वहाँ फूल/पुष्प/सुमन/प्रसून कभी एक अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते। स्वयं को कवि/कवयित्री कहलाने से पहले भाषा सीखो, शब्द-चयन की मर्यादा सीखो। अन्यथा ‘बात फँसती जाएगी, उसकी चूड़ी मारते रहोगे’ [बात सीधी थी (कविता) : र. स.], शब्दों का कौमार्य भंग करते रहोगे। कविता जैसी दिखती हर चीज़ कविता नहीं होती, इतना सब जानते हैं। छपास की हवस में ‘कागद मत गोदो’। शब्द-सजगता के दृष्टांत सुनो :
कालिदास लकड़ी का गठ्ठर लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में एक पंडित ने उनसे संस्कृत में पूछा :
‘भारवाह! भाराक्रांत भारस्त्वां बहु बाधति?’
(अर्थात्, हे बोझ ढोनेवाले! क्या यह बोझा तुम्हें बहुत दुःख दे रहा है?)
कालिदास का उत्तर था :
“यथा ‘बाधति’ बाधते मां, तथा भारो न बाधते।”
(यानी जितना तुम्हारा ‘बाधति’ शब्द मेरे हृदय को पीड़ा पहुँचा रहा है, उतना यह बोझ नहीं।)
संस्कृत व्याकरण के अनुसार ‘बाधति’ का प्रयोग करना अशुद्ध है, ‘बाधते’ शुद्ध है।
अज्ञेय अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने दर्द को ‘इंटालरेबल’ (असह्य) कहा। अज्ञेय ‘सीवियर’ (तीखे) पर अड़े रहे। अंततः डॉक्टर ने कहा कि अजीब पेशेंट है, दिल के दौरे में भी शब्दों पर बहस करता है। अज्ञेय ने कालिदास की तर्ज़ पर ही कहा, “क्यों न करूँ? इंटालरेबल : यानी जो सहा न जाए। सह तो रहा हूँ—दर्द के अतिरिक्त भाषा के साथ आपका अन्याय भी तो सह ही रहा हूँ।’’
हिंदी का एक चर्चित कवि अपनी पत्नी से कह बैठा, ‘‘आज चाँद जैसी बेदाग़ रोटी बनाओ तो जानूँ। पत्नी ने कहा कि पहली बात, चाँद बेदाग़ नहीं है… दूसरी बात, जिस अर्थ में आपने चाँद-सी बेदाग़ रोटी माँगी है, उस हिसाब से यह सही है। इतना कहकर चकोटी पर पड़ी कच्ची रोटी पकड़ा दी। सुना है कि उस दिन कवि भूखा रहा और इस वृत्तांत पर एक सुंदर कविता लिखी।
पुराने आचार्य श्लोक और छंद की शिक्षा देते थे, लेकिन सबसे पहले भाषा के व्याकरण की समझ अनिवार्य मानते थे। जिसे भाषा की समझ नहीं, वह काव्य का अधिकारी नहीं होता था। उनका ज़ोर भाषा की शास्त्रीय परंपरा पर रहता था, लेकिन आज प्रतिमान बदल गए हैं। भाषा क्लासिकल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। लोक की बोली-बानी और घूरे पर फेंक दिए गए शब्द भी समकालीन कविता में आकर अलग ही दीप्ति देते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि सबसे पुराना और त्याज्य शब्द कविता में आकर बहुमूल्य हो जाता है। बहुत पुराने बरगद के बीज-सा शब्द! जो अपने आप में अनंत वृक्षों की संभावना लिए रहता है। कविता का संबंध साधारण जीवन-प्रसंगों से यदि है, तो लोक-भाषा के शब्द उन प्रसंगों को प्रामाणिकता देते हैं। एक कवि को चाहिए कि वह विभिन्न प्रांतों में प्रचलित बोलियों से भी नए शब्द सीखे।
एक क़िस्सा है कि शेक्सपियर अपनी देहाती प्रेमिका को चूम रहे थे। तभी उसने अपनी लोकभाषा में कोई शब्द बुदबुदाया। शेक्सपियर ने उसे परे धकेला, पेंसिल से उस शब्द/वाक्य को नोट किया और पुनः उसे चूमने लगे। किसी के बड़ा रचनाकार होने का रहस्य यही है कि वह शब्दों को लेकर कितना सचेत रहता है। कवि नागार्जुन की काव्य-भाषा देखें तो लगता है कि उन्होंने भाषा के सबक़ खेत-खलिहानों, पान की गुमटियों, मिस्त्रियों, कलाकारों, कामगारों, मज़दूरों, लोक, शास्त्र, चौपालों से सीखे हैं। दरअस्ल, भाषा का विस्तार अनुभव का ही विस्तार है।
उचित शब्द-चयन ही बात कहने का ढंग देता है। कवि को कहना आना चाहिए। अगर बात को प्रभावी तरीक़े से कहना है तो भावों के मूल और आदिम रूप की ओर जाने की ज़रूरत है, जो पाठक के मन को स्पर्श करे। बात कहने की तीन शक्तियाँ आचार्यों ने बताई हैं—अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यह विवाद रहा है कि तीनों शक्तियों में श्रेष्ठ कौन-सी है! लेकिन अच्छे शब्द-शिल्पी के पास यह हुनर होता है कि वह अपनी बात में प्रभाव ले आता है। किसी शक्ति का बंधन वह नहीं मानता। बीच में एक-दो क्षेपक जोड़ता चलूँ। प्रवाद है कि सामान्य बातचीत में स्त्रियाँ लक्षणा और व्यंजना का अधिक प्रयोग करती हैं। इस संदिग्ध तथ्य से सहमत होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हिंदी के सबसे बड़े कथाकार ने इसे दूसरे रूप में कहा है कि ‘गूढ़ और रहस्य की बात कहने में स्त्रियाँ चतुर होती हैं।’ इससे संबंधित क़िस्सा है कि कवि रहीम का नौकर छुट्टी लेकर घर गया। उसका विवाह हुआ। नववधू के साथ थोड़े दिन रह अवधि उपरांत नौकरी पर लौट आया। अब नवागता वधू का जी ऊबने लगा। उसने एक बरवै लिखा और अपने पति को भेज दिया। साथ ही ‘फ़ुटनोट’ भी डाल दिया कि यह छंद रहीम को ज़रूर दिखाया जाए। वह पत्र रहीम को दिखाया गया, उसमें लिखा था :
‘प्रेम प्रीति को बिरवा दियो लगाय।
सींचन की सुधि लीज्यो मुरझा ना जाय।’
(अर्थात् हे साजन! प्रेम-प्रीति का पौधा तो आपने लगा दिया है, इसे समय-समय पर सींचते रहना, कहीं मुरझा न जाए।) रहीम समझ गए और नौकर को लंबे अवकाश के लिए घर भेजा। यह छंद रहीम को इतना पसंद आया कि बाद में ‘बरवै नायिका भेद’ के लिए इसी छंद को चुना।
एक दूसरा क़िस्सा यह है कि ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी और प्रेयसी प्रवीणराय की सुंदरता, नृत्य और काव्य-कला के चर्चे दिल्ली के बादशाह अकबर तक पहुँचे। अकबर ने संदेश भेजा कि प्रवीण हमारी सेवा में चाहिए, उसे तुरंत दिल्ली भेजा जाए। बेमन से प्रवीण दिल्ली आई। बादशाह ने कुछ सुनाने-दिखाने का आदेश दिया। प्रवीणराय ने एक दोहा सुनाया :
विनती राय प्रवीन की, सुनिए साहि सुजान।
झूठी पातरी भखत है, बारी, बायस, स्वान।
(अर्थात्, हे शाहे अकबर! मेरी विनती सुनो। झूठी पत्तल नीच व्यक्ति, कौवे और कुत्ते ही खाते हैं। यदि आप इन तीनों में से कोई एक हो तो मैं आपकी हुई।)
कहते हैं कि अकबर ने ससम्मान प्रवीणराय को ओरछा वापस भेज दिया। पहली ने अपनी चतुराई से प्रेमी पाया, दूसरी ने अपनी चतुराई से बलात् गले पड़े प्रेमी से पीछा छुड़ाया।
एक क़िस्सा रीतिकालीन स्वच्छंद कवि आलम की विदुषी पत्नी शेख से संबंधित है। उनके पुत्र का नाम जहान था। एक बार शहज़ादा मुअज़्ज़म ने शेख़ से शरारतन पूछा कि सुनते हैं कि आप आलम की औरत हैं? तो शेख़ ने उत्तर दिया कि जी हाँ, मैं ही जहान की माँ हूँ। उर्दू वाले जानते हैं कि ‘आलम’ और ‘जहान’ के यहाँ क्या अर्थ हैं। विदित रहे कि यह वही शेख़ रंगरेजिन है, जिनकी कवि-प्रतिभा से प्रभावित होकर आलम जैसे पंडित ने कलमा पढ़ लिया था। प्रचलित है कि आलम का एक कुर्ता शेख़ के घर धुलने गया, जिसकी जेब में एक दोहे का आरंभिक हिस्सा लिखा हुआ था, जिसके अगले दो चरण कवि से बन नहीं पाए था। दोहे का आरंभिक हिस्सा यूँ था :
‘‘कनक छरी-सी कामिनी, काहे को कटि छीन।’’
(अर्थात् कामिनी की देह-आभा स्वर्ण-छड़ी के समान है, किंतु उसकी कमर इतनी पतली क्यों है?)
इसे आलम ने पूरा करके वापस जेब में रख दिया। आलम को पूरा दोहा मिला :
“कनक छरी-सी कामिनी, काहे को कटि छीन।
कटि को कंचन काटी विधि, कुचन मध्य धरि दीन।”
(अर्थात् उसकी कमर पतली इसलिए है कि विधाता ने उसकी कमर के स्वर्ण को काट कर स्तनों में भर दिया है।)
बात थोड़ी विषयांतर हो गई। बहरहाल; लक्षणा, व्यंजना या कूट भाषा कविता की कसौटी नहीं है। भवानीप्रसाद मिश्र ने भाव और विचारों की सरलता के लिए बरसों पहले सीख दी थी कि ‘जिस तरह हम बोलते हैं, उस तरह तू लिख’। सुमित्रानंदन पंत ने भी अलंकारों की चटक-मटक की अपेक्षा विचारों के संप्रेषण पर ज़ोर देते हुए लिखा :
‘तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार।
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार।’
यह अलग बात है कि उनकी आरंभिक कविताओं को पढ़ने के क्रम में सामान्य पाठक को शब्दकोश लेकर ही बैठना पड़ता है।
समकालीन कवियों से नई पीढ़ी सीख ले सकती है कि साधारण भाषा में असाधारण भाव भरे जा सकते हैं। इस संबंध में त्रिलोचन आदर्श कवि हैं। त्रिलोचन से सीखा जा सकता है कि साधारण से प्रतीत होते वाक्यों में अर्थ-विस्तार कैसे दिया जा सकता है! राजेश जोशी की कविता ‘बच्चे काम पर जा रहे हैं’ के सरल से दीखते वाक्य ‘बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं’ के भीतर कितने प्रश्नों की अनुगूँज है? वर्तमान के कितने स्याह पक्ष इस एक वाक्य में गुम्फित हैं…
तो बात कहने के लिए सरल-जटिल के बंधन में पड़ने की अपेक्षा कहन शैली को सुदृढ़ बनाएँ। पाठक उस भाव तक पहुँचे, जो भाव कवि का था। यह अच्छी कविता की सार्थकता है। ये भाषा ग्रहण और भाव-प्रस्तुति के कुछ आइडियाज हैं, जिनसे सहमति का आधार स्वेच्छा है।
कविता सिखाने और कवि बनाने की कोई फ़ैक्टरी नहीं होती। धन पिपासु और फ़रमाइशी लिखारों की अपेक्षा नई पीढ़ी को चाहिए कि तुलसी, कबीर, रसखान, बिहारी, निराला, मुक्तिबोध, जैसे पुराने कवियों की रचनाओं को अपना उस्ताद बनाएँ और अपने समकालीनों की रचनाओं से अद्यतन रहते हुए दिशा-निर्देश भी पाते रहें।
अस्तु!






