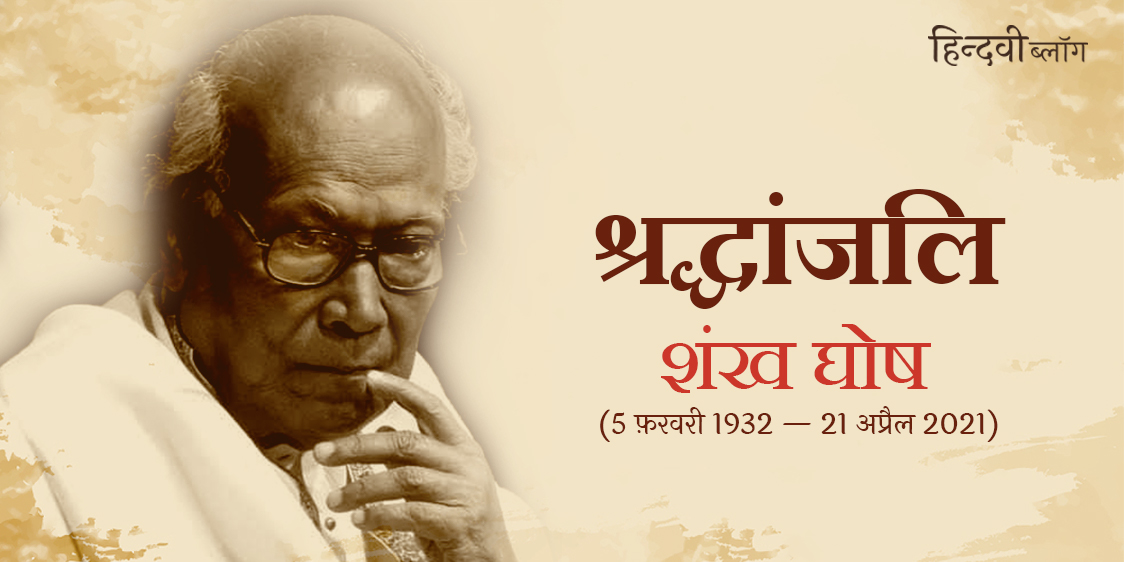
‘अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो’
 अविनाश मिश्र
अप्रैल 21, 2021
अविनाश मिश्र
अप्रैल 21, 2021
बातें बस बातें कीं बड़ी-बड़ी बातें कीं,
चतुरता! क्या क्लांति-भर बाक़ी है
वापस घर आने पर।
यही मन करता है, नहा लूँ, जलाऊँ धूप,
बैठा रहूँ चुपचाप,
चुपचाप, नीले प्रकाश में।
चोगा यह फेंक कर पिशाच का,
बनूँ फिर मैं आदमी।
आर्द्र समय बह आता, उठतीं लहरें उसकी,
सोऊँ मैं उस अनंत शैया में निर्विकार, निश्चिंत!
ऐसा लगता है सचमुच? चिंता फिर है किसकी?
चतुरता चली जाओ
ज़्यादह से ज़्यादह यही तो कहेंगे लोग,
मूर्ख है बहुत यह, दुनियावी नहीं है।
कवि के न रहने पर उसकी इस प्रकार की कविता-पंक्तियों की खोज जिनमें कवि ने अपने न रहने को, अपने अंत को पहचाना था; एक नितांत समाचाराधीन काम है। लेकिन यह काम करते हुए करने वाला कवि को एक नई नज़र से भी देखता है। इस नई नज़र में कवि अब केवल अपनी कविताओं में है।
इस अर्थ में देखें तो बांग्ला के समादृत कवि शंख घोष [5 फ़रवरी 1932—21 अप्रैल 2021] की मृत्यु इस दौर को जिसमें मृत्यु सत्य से अधिक समाचार प्रतीत हो रही है, हमें कुछ और अभावग्रस्त कर गई है। वह 89 वर्ष के थे और कई बीमारियों के साथ-साथ कुछ माह से कोरोना-संक्रमण से भी जूझ रहे थे।
ज्ञानपीठ और साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कविता के अविस्मरणीय हस्ताक्षर शंख घोष ने अपने नाम के बिल्कुल उलट जाकर अपने कविता-संसार में मौन को प्रमुखता दी है। वह शोर के प्रति निर्विकार और उससे निश्चिंत रहे आए। यह कृत्य उनके लिए एक बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया-सा रहा।
शोर के सम्मुख मौन को पहचाने के विवेक का वरण शंख घोष की कविता का केंद्रीय कार्य-भार रहा। इस कार्य-भार ने शोर के भय को कुछ कम करके अपने जन को निरुद्विग्न किया और सोचने को विवश भी। शंख घोष के कविता-संसार की यह एक दुर्लभ विशेषता है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि हिंदी में प्रकाशित अपनी प्रतिनिधि कविताओं के अनुवादों की भूमिका का शीर्षक उन्होंने ‘मौन की संकेत पताका’ रखा है।
‘‘लेकिन क्या शब्द ही मौन को नहीं रचते?’’
इस प्रश्न से संघर्ष करते हुए शंख घोष कहते हैं :
‘‘हम कितना चाहते हैं कि अनौपचारिक अभिव्यक्ति से ही काम चला सकें, जो सहज और फिर भी आत्मीय हो, स्पष्ट और सरल। यहाँ तक कि शब्द भी आड़े न आएँ और आधुनिकता के प्रपंच से रहित हों। पर कुटिल प्रवृत्तियाँ आज के समाज पर शासन करती हैं, पाखंड का फण और फैल रहा है—इन दिनों शायद ही कोई दूसरे की आँखों में झाँकता हो। हर कोई लोगों के बीच परेशान चेहरा पहनना चाहता है, जैसे किसी अनजाने समूह में हो। ऐसे में क्या हो कविता की प्रासंगिकता और भूमिका?’’
‘कविता की प्रासंगिकता और भूमिका’ लिखकर उसके आगे प्रश्नचिह्न लगाने की ज़रूरत शंख घोष के पूर्ववर्तियों को भी पड़ी और उनके वंशजों को भी पड़ रही है। यों लगता है कि जैसे समाज धीरे-धीरे अपने हिस्से का अन्न-वस्त्र-ज़मीन हड़पकर अपने हिस्से की कविता से दूर हो गया है।
यह भाषाओं का संकट है और इस संकट में ‘हमको नहीं दी कोई मातृभाषा देश ने’ यह कहने को शंख घोष सरीखे कवि विवश होते हैं। वह कविता को एक भारी शिला की तरह अपनी छाती पर धारण कर मौन में गति करते हैं :
धिक्! मेरी ग़लतियों परे जाओ, उतरो
मैं फिर से शुरू करूँ,
फिर से खड़ा होऊँ, जैसे खड़ा होता है आदमी।
नि:शब्दता, नीरवता, चुप्पी और अव्यक्तता एक व्याकुलता के साथ शंख घोष की कविताओं में बार-बार प्रकट होती है। दर्शन की सुंदरता में यह कविता-संसार आत्म-आख्यान का संसार है—अपने को भीड़ में छुपाने के लिए।
‘‘अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो।’’
उजले शब्दों में शंख घोष की कविता एक ख़ामोश कविता है। पर इसका संबंध अगर कोई केवल आध्यामिकता से ही जोड़े, तब यह उसकी भूल होगी; क्योंकि यह भौतिक जीवन से बिल्कुल विलग नहीं है। यह कविता मौन का आवरण इसलिए धारण करती है, क्योंकि यह शांत रहकर शोर का निरीक्षण करना चाहती है :
थोड़ी और चुप्पी, फिर छूता हूँ
एक को, कहता हूँ
जागो, अब
और कोई नहीं!
चुपचाप पहचान चुपचाप—
तुम्हारे आनंद में,
जागना मेरा!
इन कविताओं के मौन का भार मात्र एक शांत हृदय ही वहन और अनुभव कर सकता है। इस धरा पर ऐसे शांत-हृदय मानुषों की संख्या में वृद्धि हो, कवि के देहावसान की इस दुखद घड़ी में यह प्रार्थना ही कवि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
~•~
शंख घोष की कविता-पंक्तियों के बांग्ला से अनुवाद : प्रयाग शुक्ल






