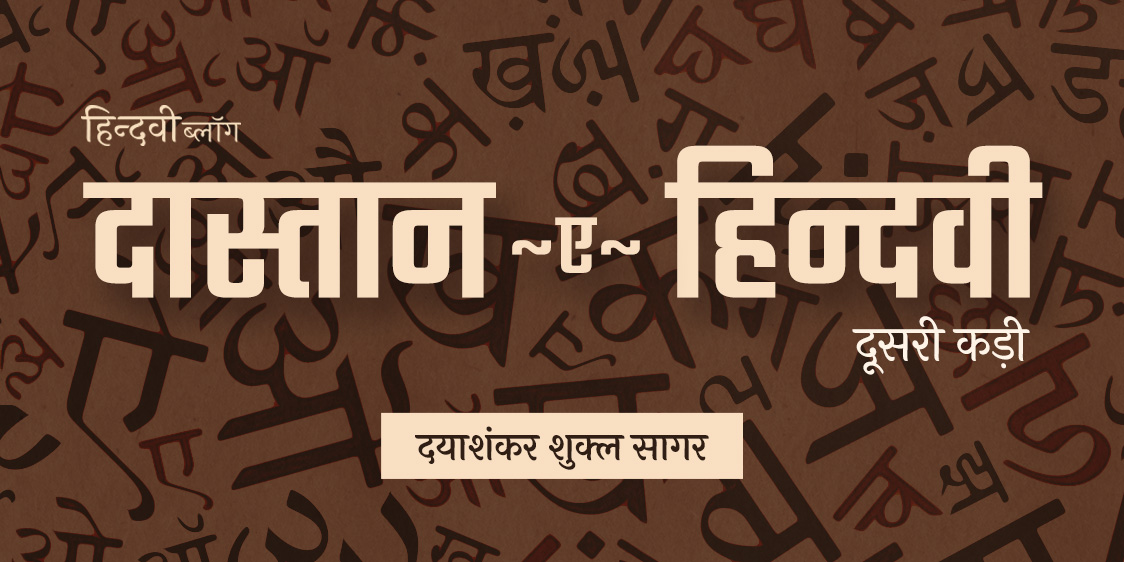
अपभ्रंश का दौर
 दयाशंकर शुक्ल सागर
जुलाई 23, 2021
दयाशंकर शुक्ल सागर
जुलाई 23, 2021
हिंदी को हमेशा हिंदुस्तानियों से जोड़कर देखा गया है, जिसे बोलने वाले मुसलमान भी थे, हिंदू भी और पारसी भी। इस तरह देखें तो हिंदी का किसी दीन या मज़हब से कुछ लेना-देना नहीं था। भारत में पारसी वे थे जिनके पूर्वजों ने इस्लाम के आने के बाद फ़ारस से भागकर हिंदुस्तान में पनाह ली थी। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पारसी हिंदुस्तान में हैं। अरबी में ‘प’ का उच्चारण ‘फ़’ है, तो उनके लिए पारसी फ़ारसी हो गया और पारस यानी पर्शिया फ़ारस जो अब ईरान के नाम से जाना जाता है। लेकिन फ़ारस की ज़बान और लिपि इतनी समृद्ध थी कि इस्लामिक स्कॉलरों की यह मक़बूल ज़बान हो गई। फिर वे तुर्क हों, पठान हों या अरबी सब फ़ारसी के मुरीद हो गए। वे अपने साथ फ़ारसी ज़बान और लिपि यहाँ ले आए। मुस्लिम सुल्तानों ने फ़ारसी को ही शाही ज़बान बना दिया। सारे सरकारी कामकाज फ़ारसी में होने लगे।
भाषा को लेकर वह एक दिलचस्प दौर था। फ़ारसी सरकारी भाषा थी, लेकिन हिंदुस्तान में ‘अपभ्रंश’ बोली जाती थी। उसके लिए एक शब्द ‘भाषा’ था, जिसे कुछ लोग ‘भाखा’ भी कहते थे। ये लफ़्ज़ ग़ालिबन उत्तर भारत में ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता था। भारत एक बड़ा देश था। हर इलाक़े की अलग ज़बान थी। जैसे बंगाली, गुजराती, अवधी, कश्मीरी वग़ैरह। इनमें हर इलाक़े की ज़बान दूसरे इलाक़े में ‘भाखा’ कहलाती थी। इस ‘भाखा’ में ज़्यादातर शब्द अपभ्रंश होते थे। मसलन माँ के लिए संस्कृत में एक शब्द है—माता। ये अपभ्रंश होकर माई, माते, मातु, महतारी जैसे शब्दों में इस्तिमाल होने लगा। ज़ाहिर है कि ये प्यार से माता के लिए अपने बोली में एक अभिव्यक्ति थी, लेकिन संस्कृत वालों के लिए ये शब्द अपभ्रंश या अपभ्रष्ट हो गए।
अपभ्रंश को किसी ने ‘भाषा’ नाम दिया, किसी ने ‘देसी भाषा’ यानी ‘गामेल्ल भाषा’ कहा। गामेल्ल भाषा से यहाँ अर्थ है—देहाती भाषा। अपभ्रंश या अपशब्द, कहीं-कहीं ‘अपभ्रष्ट’। इस शब्द को बतौर हिक़ारत की तरह पेश किया गया है। लेकिन आगे चलकर यही अपभ्रंश एक भरी-पूरी भाषा बन गई। जैसा कि 7वीं सदी में संस्कृत के महान साहित्यकार दंडी ने लिखा है कि व्याकरण-शास्त्र में संस्कृत से अलग शब्दों को ‘अपभ्रंश’ का नाम दिया। इस तरह पालि-प्राकृत-अपभ्रंश सभी के शब्द ‘अपभ्रंश’ संज्ञा के तहत आ जाते हैं। जैसा कि ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी इस किताब में उस दौर के बारे में लिखा : ‘‘जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो ‘भाषा’ या ‘देश भाषा’ ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए ‘अपभ्रंश भाषा’ का व्यवहार होने लगा।’’
यानी साफ़ है कि भारत में मुसलमानों के आने से पहले भारत में तीन प्रमुख भाषाएँ चलन में थीं। एक संस्कृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी अपभ्रंश। इनमें पहली दो भाषा के सुबूत हमें वेदों और महात्मा बुद्ध के ज़माने से मिलते आए हैं। अपभ्रंश का पहला सुबूत हमें 7वीं सदी में मिलता है। 19वीं सदी में पहली बार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। बाद में इस अपभ्रंश को शुक्लजी ने भी ‘पुरानी हिंदी’ की मान्यता दे दी।
इस अपभ्रंश भाषा का न तो कोई व्याकरण होता और न कोई स्वतंत्र शब्दावली। ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा… वाली बात थी।
वैसे देखें तो 7वीं और 12वीं सदी के बीच उत्तर भारत में कम से कम छह भाषाएँ ख़ूब प्रचलित थीं। इनमें संस्कृत, प्राकृत, शोरसैनी, अपभ्रंश, मैथिली, पिचाशी और देसी बोली शामिल थीं। देसी बोली का मतलब किसी भी इलाक़े में बोली जाने वाली मक़ामी ज़बान था। इनका ज़िक्र मरव की श्रीकंठ चरित की टीका में मिलता है। 9वीं सदी के संस्कृत आचार्य रूद्रट ने भी इनका ज़िक्र किया है। (कीर्तिलता और हवहट्ठ भाषा, डॉ. शिव प्रसाद सिंह पृष्ठ : 4) जब ये भाषाएँ थीं, तब हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं थी। यह वह दौर था जब सारी बोलियाँ अपभ्रंश से मिलकर नई भाषा बना रही थीं जिसमें आज की हिंदी की शब्द आने लगे थे। अपभ्रंश जिससे हिंदी और उर्दू पैदा हुई उसमें खड़ी बोली के सिर्फ़ कुछ शब्द मिलते हैं। ये लिखी नागरी में गई, लेकिन आज के हिंदी जानने वाले इसे मुश्किल से पढ़ और समझ पाएँगे। अब ऐसी ही अपभ्रंश की एक मिसाल देखिए जिसे ‘अवहट्ठ भाषा’ कहा गया। हिंदी के समादृत भाषाशास्त्री सुनीति कुमार चटर्जी इसे 9वीं से 12वी सदी की भाषा मानते हैं। ये उत्तर भारत के राजपूत राजाओं में प्रचलित थी। इसे मोटे तौर पर शौरसेनी अपभ्रंश कहा जाता था। अब इस अपभ्रंश की एक मिसाल देखिए जिसे पुरानी हिंदी कहा गया है। ये भाषा विद्यापति की है, जिन्हें पुरानी हिंदी का कवि माना जाता है।
‘‘सक्कय वाणी बहुअन भवाई। पाउँस रस को मम्म न पावई॥ देसिल बअना सब जन मिट्ठा। तं तैसन जम्पऔ अवहट्ठा।’’ (कीर्तिलता विद्यापति, प्रथम पल्लव 19 से 22वीं पंक्ति)
यानी विद्यपति कहते हैं : ‘‘संस्कृत भाषा केवल विद्वानों को अच्छी लगती है। प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता। देसी वचन सबको मीठा लगता है, वैसा ही मैं अवहट्ठ में लिखता हूँ।’’
‘कीर्तिलता’ की रचना विद्यापति ने की थी। वह मिथिला के थे। उनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और पिता का नाम गणपति ठाकुर। ठाकुर साहब संस्कृत के उच्चकोटि के विद्वान और राजाश्रित कवि थे। उनके बेटे विद्यापति तिरहुत यानी मिथिला के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। ग़ौर करने वाली बात यह है कि इस पुरानी हिंदी में अभी अरबी और फ़ारसी लफ़्ज़ शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि मुस्लिम हमले अभी उत्तर भारत में शुरू नहीं हुए थे। सिंध (712ई.) और मुल्तान (713 ई.) इलाक़े में ज़रूर अरबी-फ़ारसी वहाँ की स्थानीय भाषा में दाख़िल होने लगी थी, क्योंकि वहाँ 8वीं सदी के शुरू में ही मुहम्मद बिन क़ासिम हमला कर अपना असर जमा चुका था। यह असर इतना गहरा था कि हिंदुस्तान का यह हिस्सा उसी दौर में भारत से अलग-सा हो गया था। लेकिन आप देखिए विद्यापति की इस पुरानी हिंदी में एक भी लफ़्ज़ ऐसा नहीं है, जो आज की खड़ी बोली की हिंदी के आस-पास भी हो। या कहें अगले 200 साल बाद आए अमीर ख़ुसरो की हिंदी के क़रीब भी हो।
जारी…
~•~
पिछली कड़ी यहाँ पढ़ें : आया कहाँ से ये लफ़्ज…






