
दुस्साहस का काव्यफल
 आशीष मिश्र
मई 24, 2022
आशीष मिश्र
मई 24, 2022
व्यक्ति जगद्ज्ञान के बिना आत्मज्ञान भी नहीं पा सकता। अगर उसका जगद्ज्ञान खंडित और असंगत है तो उसका अंतर्संसार द्विधाग्रस्त और आत्मपहचान खंडित होगा। आधुनिक युग की क्रियाशील ताक़तें मनुष्य के जगद्ज्ञान को नियंत्रित करके उसके आत्मपहचान को बदलने की कोशिश करती थीं। चाहे पूँजीवाद हो या साम्यवाद—हर पक्ष की मूल कार्ययोजना यही थी। लेकिन उस आत्मपहचान में एक अन्विति, सममिति, मुकम्म्लपन और कंसिस्टेंसी थी—ठीक आधुनिक वास्तुकला की तरह। उस अन्विति ने ही न्यूनतम सामाजिक सहमति पर महत्तर राजकीय संस्थाओं की रचना की और उन्हें मुकम्मल सहमति जुटाने का कार्यभार सौंपा। स्वतंत्रता-समता-न्याय का वह स्वप्न रचा जिसने मनुष्य के ह्रदय को उन्मुक्त उत्साह से भर दिया। लेकिन उत्तरआधुनिकता ने इससे ठीक विपरीत व्यक्ति की जगद्चेतना और आत्मचेतना को खंडित करके उसके अवचेतन को निर्देशित करने की तरकीब खोज लिया। समता और न्याय को अनंत खंडों में ऐसा तोड़ दिया गया कि न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष ही अन्याय लगने लगा। स्त्रियों, दलितों, मजदूरों और आदिवासियों के संघर्ष को फिर से एक धार्मिक और राष्ट्रवादी उन्माद के साथ पीछे फेर दिया गया। लोकतांत्रिक संस्थाएँ अपना स्वत्व खोकर मज़ाक़ का विषय बन गईं। व्यक्ति के विशिष्ट जीवनदर्शन, नैतिकचेतना और सौंदर्यचेतना को असमाप्य उपभोग से तौलकर बिखेर दिया गया। हमारी युगचेतना और आत्मचेतना को इतना बिखेर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी विवेकपूर्ण व स्वस्थ आत्मछवि बना ही नहीं पाता। ऐसे में अन्य कला माध्यमों के साथ कविता की भी यह ज़िम्मेदारी है कि वह मनुष्य के मन को सौंदर्य और न्याय के पक्ष में पुनर्संयोजित करे। व्यक्ति को वास्तविक आत्मपहचान की खोज करने में मदद करे, नए दुश्मन और दोस्तों की पहचान कराए। हिंदी की समकालीन कविता किसी हद तक यह ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है। जसिंता केरकेट्टा के कविता-संग्रह ‘ईश्वर और बाज़ार’ में भी यह कोशिश आपको दिखाई पड़ेगी।
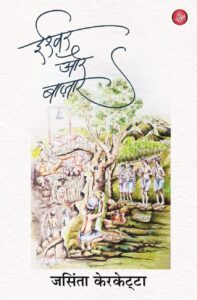
ईश्वर और बाज़ार │ स्रोत : राजकमल प्रकाशन
मनुष्य ने मनुष्यों पर शासन करने के लिए अब तक जो कुछ खोजा है उनमें सबसे कारगर चीज़ है—ईश्वर। ईश्वर है या नहीं है—इस पर कोई बहस कर भी सकता है, लेकिन ईश्वर के नाम पर वृहत्तर मनुष्यता का शोषण होता है, जिसे ईश्वर भी नहीं बचा सकता, यह आँखिन देखी सच्चाई है। हर सामाजिक दमन में ईश्वर नाम नींद की टिकिया की तरह शामिल मिलता है, यह सामजिक विश्लेषणों की सच्चाई है। इस सबके बावजूद ईश्वर जगद्दर्शन का एक पूरा कॉम्बो पैक था। लेकिन बाज़ारवाद की उसके मुकम्मल दर्शन से पटरी नहीं बैठ सकती, इसलिए इसे भी जगह-जगह से तोड़कर एक उन्मादधर्मी बाज़ारू ईश्वर पैदा कर दिया है। आज का ईश्वर पूर्व आधुनिक समाजों की विश्वास से पैदा सत्ता नहीं, बल्कि बाज़ार का आकर्षक ब्रांड है। जसिंता इसे समझती हैं और सामाजिक व्यक्तिगत दमन के तमाम पक्षों को खोलती हैं। इस तरह, इस संग्रह का नाम—‘ईश्वर और बाज़ार’—सार्थक ही लगता है।
समकालीन कविता में ईश्वर और मनुष्य के संबंधों को देखने की अतिरिक्त कोशिश मिलेगी। और वह शायद इसलिए है कि बाज़ारवाद ने धर्म और ईश्वर की रही-सही परदेदारी को भी नंगा कर दिया है। अगर आप ध्यान दें तो पिछले दशकों में हिंदी के कुछ अच्छे कवियों के संग्रह ईश्वर से शुरू होते हैं। ‘ईश्वर की अध्यक्षता में’—लीलाधर जगूड़ी, ‘ईश्वर एक लाठी है’—स्वप्निल श्रीवास्तव, ‘ईश्वर नहीं नींद चाहिए’—अनुराधा सिंह, और जसिंता केरकेट्टा का हमारा विवेच्य संग्रह—‘ईश्वर और बाज़ार’। सारे कवियों ने ईश्वर और मनुष्य के नए उभरते हुए तनाव को पकड़ा है। जितना पकड़ में आया है उतनी कविता है, जहाँ छूट गया है वहाँ स्थापित बातों का दुहराव है। पिछले दशकों में तमाम अस्मिताओं ने ईश्वर से अपने दमन और शोषण के सीधे संबंध को पहचाना है। जसिंता एक कविता में बड़ा सरल-सा प्रश्न पूछती हैं :
“मंदिर मस्जिद गिरजाघर टूटने पर
तुम्हारा दर्द कितना गहरा होता है
कि सदियों तक लेते रहते हो उसका हिसाब
पर जंगल जिनका पवित्र स्थल है
उनको उजाड़ने का हिसाब, कौन देगा साब?
जाने कब से धर्म-धर्म खेल रहे
जो तुम्हारे धर्म के दायरे में आते नहीं
वे जंगलों को पूजते हैं, जंगल को जानते हैं
वहीं जीते हैं वहीं मर जाते हैं
तुम सब बूट पहनकर
उनके पवित्र स्थलों में कैसे घुस आते हो?”
इन पंक्तियों का सौंदर्य कवीत्व के पारंपरिक लक्षणों में नहीं है, बल्कि मौलिक प्रेक्षा और नवीन प्रश्न में है—तुम सब पवित्र जंगलों में बूट पहनकर कैसे घुस आते हो? वैसे तो हमें समझ नहीं आता कि बिना बूट पहने जंगल कैसे जा सकते हैं! लेकिन जब कविता के संदर्भ से इस पर विचार करते हैं तो लगता है कि सच में जंगलों में बूट उतारकर, प्रणाम करके, विनम्रता से ही प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि वे भी किसी के पवित्र आस्था का विस्तार हैं। जंगल में बूट की व्यंजना बहुत गहरे—राजकीय दमन तक जाती है, लेकिन अभिधार्थ भी कम प्रभावी नहीं है। ईश्वर और उसकी सत्ता को सबसे सटीक ढंग से स्त्रियों ने पहचाना। ऐसी अनेक कविताएँ इस संग्रह में हैं, जहाँ स्त्री ख़ुद को समझने की कोशिश करती है तो अजब ढंग से ईश्वर बेपर्दा होता जाता है!
‘स्त्रियों का ईश्वर’ शीर्षक कविता जब ईश्वर और स्त्री के तनाव बिंदु पर पहुँचती है तो एक बौद्धिक विस्फोट बन जाती है :
‘‘मैं ईश्वर के सहारे जीती रही
और माँ ईश्वर के भरोसे मार खाती रही।’’
मुकम्मल कविता के संदर्भ में इन पंक्तियों को देखने से पता चलता है कि यह ईश्वर के भरोसे जीना और उसके भरोसे मार खाना नहीं है, बल्कि स्त्री के आत्मविस्थापित जीवन और उसकी पिटाई में कहीं उसका भी अदृश्य हाथ शामिल है।
इन दिनों हमारा लोकतंत्र किसी बवंडर में फँसा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि हम आधुनिकता और ज्ञानोदय के सदियों आगे नहीं, बल्कि कहीं उसके पीछे जी रहे हैं। पिटे-पिटाए प्रश्नों को ऐसे पूछा जा रहा है, गोया पहली बार पूछे जा रहे हों। डिज़िटल माध्यमों का हौलनाक उपयोग करके जनता की प्रगतिशील चेतना को इतना धुँधला कर दिया गया है कि वह पूछ रही है—न्याय किस चिड़िया का नाम है और इसकी ज़रूरत ही क्या है! जनपक्षधर प्रगतिशील शक्तियाँ सही प्रश्न पूछने और सत्ताछल का जवाब देने की असफल कोशिश में जूझ रही हैं। जसिंता का यह संग्रह इन जनपक्षधर शक्तियों के दुस्साहस का काव्यफल है। उनका यह संकलन समकालीन नागरिक जीवन में चल रही बहसों का सबसे प्रगतिशील जवाब है। उनका कवि-व्यक्तित्व अपनी सार्थकता किसी उक्ति-वैचित्र्य की बजाय अपने समय का सबसे सटीक जवाब होने में खोजता है। लेकिन तरह-तरह के जवाब तो हवा में घूम ही रहे हैं। रेडीमेड जवाबों पुनर्योजन से कविता होने से रही। इसके लिए अनुभूति की आग चाहिए जो पुराने जवाबों को भी नई धार दे दे। अनेक कविताओं में, जहाँ अनुभूति का दबाव पड़ा है, वहाँ भाषा और भंगिमा में वह कसाव है कि पाठक प्रभावित हुए बिना न रहेंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह रचनात्मक तनाव ढीला पड़ जाता है। कई कविताओं में ऐसी प्रभविष्णु तार्किकता है कि पूरी सामाजिक संरचना को एक उक्ति में खोल दे। एक सामान्य-सी बात है कि सवर्ण अपनी समृद्धि को स्वतः सिद्ध समझता है। वह वंशानुक्रम से चले आते इस समृद्धि के सामजिक कारणों में नहीं झाँककर इसे अपनी क़ाबिलियत का प्रमाण मानता है। इस बात के लिए जसिंता कितनी सधी मार करती हैं :
“बेईमानी का ब्याज हम ईमानदारी से
आज भी खाते हैं
और बेशर्म इतने हैं कि
इसे अपना हक़ बताते हैं”
अभिजन वर्ग की पूरी सत्ता पूर्व में की गई बेईमानियों का ब्याज है। यह बेईमानी कभी आर्थिक थी तो कभी सामाजिक। बेईमानी इतनी पुरानी और स्वीकृत है कि अपना हक़ लगती है। शिक्षा के पतन और साम्प्रदायिकता में आवयविक संबंध है। अधिसंख्य जनता को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान किस दिशा में और कितनी दूर है। इसलिए लोग अगल-बग़ल की कोई मुस्लिम बस्ती देखकर उसे ही पाकिस्तान समझ लेते हैं। अब पाकिस्तान देश से बाहर नहीं है। अब देश के अंदर ही तरह-तरह का पाकिस्तान है। बाहर वाले पाकिस्तान से राजनीति को उतना फ़ायदा नहीं था, अंदर वाले से बहुत फ़ायदा है। मैं जिस बात के लिए इतने शब्द ख़र्च कर रहा हूँ, जसिंता उसे बहुत किफ़ायतसारी से एक जुमले में कह सकती हैं।
यह संग्रह पढ़ते हुए मिलेगा कि जसिंता कविता को मानवीय संवेदना का नव-संयोजन मानने की बजाय विचारों का पुनर्योजन मानती हैं। इसलिए वह कविताओं से संवेदित करने की बजाय कन्विंस करने की कोशिश करती हैं; इसलिए तथ्यों, तर्कों और वक्तृता का इस्तेमाल करती हैं। अनेक जगहों पर इस वक्तृता में नवीन उक्तियों, जुमलों और अदायगी का कसाव है। लेकिन कई बार यह सब बहुस्थापित तर्कों और आख्यानों का ढीला-ढाला पुनरुत्पादन भर है। मैं समझता हूँ कि कविता स्थापित सत्यों और आख्यानों की मौलिक भंगिमा भर भी हो सकती है। लेकिन यह भी तभी होगा जब वह या तो तथ्यों का संवेदनात्मक पुनर्बलन करे या नवीन सक्षम भंगिमा की खोज। लेकिन यह जोड़ना चाहिए कि कविता की आत्मा स्थापित सत्यों को कहने में नहीं, बल्कि नवीन सत्यों की खोज में है। यही होकर ही कविता सभ्यता का दरवाज़ा बनती है।
कई बार कुछ कविताएँ अपनी पीढ़ी के तेज़ और साहस का परचम बन जाती हैं। और इस समय जब हम अपने लोकतंत्र के सबसे शर्मनाक दिनों से गुज़र रहे हैं तो जसिंता का तेजोदीप्त मस्तक हमारी जुर्रत का प्रतीक लगता है। ये कविताएँ गाढ़े लिसलिसे अँधेरे से जूझती हमारी जनता की जबान को थोड़ा और साफ़ करेंगी। जसिंता की कविताएँ बैरिकेड के दूसरे तरफ़ खड़े किसी विवेकदीप्त युवा की तमाम सत्ताओं से की गई अथक ज़िरह हैं। उनका सीधा संबोधन और लगातार प्रश्नों की झड़ी से निरुत्तर कर देने वाली मुद्रा रगों में हलचल पैदा करती है। लेकिन यही एकतरफ़ा संबोधन काव्यबोध की कई सीमाएँ भी रचता है। ऐसा लगता है कि कवि दुनिया को ‘हम और वे’ के जिस मोटे विभाजन को मानकर चल रहा है, न उसमें कोई संशय है; न आत्मसंदेह। फलतः ‘वे’ पर अथक आक्षेप आत्मरक्षा का ओट बनता है और कविता की अंतर्वस्तु में विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है। अगर जसिंता में किंचित आत्मसंबोधन भी होता तो इसके साथ उनकी विधेयात्मक आत्मपहचान, आदिवासी लोकेल और कविता में एक अक्षुण्ण अनुनाद भी पैदा होता।
~•~
जसिंता केरकेट्टा की कविताएँ यहाँ पढ़ें : जसिंता केरकेट्टा का रचना-संसार






