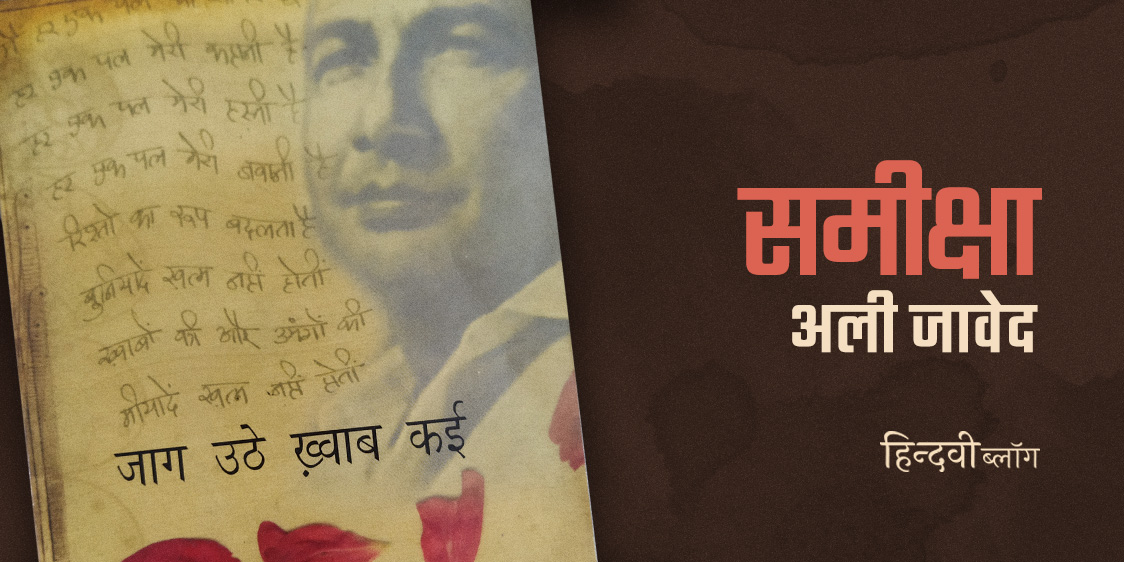
जनवाद और साहित्य की तिजारत
 अली जावेद
जुलाई 13, 2021
अली जावेद
जुलाई 13, 2021
साहिर लुधियानवी ने एक जगह कहा है :
अपना हक़ माँग मगर उनके तआउन से न माँग
जो तेरे हक़ का तसव्वुर ही फ़ना कर डालें
इंसानी हुक़ूक़ की पामाली, सांस्कृतिक आतंक और इस अन्याय के ख़िलाफ़ उठती हुई अवाज़ों की गूँज हर दौर और हर समाज में जनमानस की चिंताओं का केंद्र रही है। इस अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले महात्माओं ने अपने आदर्शों को हासिल करने की ख़ातिर अपनी हस्ती मिटा दी जिसका ताज़ा उदाहरण फ़ादर स्टेन स्वामी की शहादत है।
लेकिन अनंतकाल से होता आ रहा है कि बहती गंगा में डुबकी लगा लेने वाले भी हालात के मुताबिक़ डुबकी लगाकर अपनी दुकानें सजाने में पीछे नहीं होते। आज हम अपने समाज में जिन हालात से दो चार हैं, उनकी वजह तलाश करने के लिए किसी रिसर्च या गहन इतिहास के अध्ययन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साफ़ है कि अँग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने अपनी जानें क़ुर्बान कर दीं और यह नहीं सोचा कि जान देने से उनका अपना फ़ायदा क्या होगा बल्कि अपने आदर्शों के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। आज़ादी मिलने के बाद जो लोग बच गए, उन्होंने किसी पद या ओहदे की कामना नहीं की; बल्कि ज़्यादातर स्वतंत्रता-सेनानियों ने यह कहकर कोई पद लेने से मना कर दिया कि उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में किसी पद हासिल करने के लिए हिस्सा नहीं लिया था, यह तो उनके उसूलों और फ़र्ज़ का तक़ाज़ा था। हम कई ऐसे इंक़लाबियों को जानते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता-सेनानी होने की सनद और पेंशन लेने से इंकार कर दिया और सत्ता में बैठकर आज़ादी का सुख भोगने से भी।
इसके साथ यह भी ग़ौरतबलब है कि अँग्रेज़ी सत्ता के दौर में हुक्मरानों की मुख़बिरी के लिए क्रांतिकारियों के साथ जेल में रहने वाले बहुत से अँग्रेज़ों के दलाल सत्तासीन हो गए और आज हम सत्ताधारियों के उसी गिरोह से घिरे हुए हैं।
यह विडंबना सिर्फ़ सियासत के क्षेत्र तक सीमित नहीं रही और साहित्य-संस्कृति के मैदान में भी यही नज़ारा देखने को मिला। यह हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि साहित्य अकादेमी जैसे संस्थान के चुनाव में महाश्वेता देवी जैसी बुद्धिजीवी और लेखक हार जाती हैं। ज़ाहिर है कि यह चुनाव आम जनमानस नहीं, बल्कि लेखक और बुद्धिजीवी ही अपने मत देकर करते हैं। यही हाल साहित्य अकादेमी के पुरस्कारों का है जिसकी तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इतना इशारा काफ़ी होगा कि कैफ़ी आज़मी और कृश्न चंदर इस पुरस्कार से वंचित रहे। यह सोचकर ख़ुद को सांत्वना दी जा सकती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो कृश्न चंदर के उपन्यास ‘एक गधे की सर-गुज़श्त’ से साहित्यप्रेमी महरूम रह जाते। बात लंबी होती जा रही है और मेरे कर्ब यानी दर्द के इज़हार की भूमिका तूल पकड़ती जा रही है तो इतना कह दूँ :
रखियो ‘ग़ालिब’ मुझे इस तल्ख़-नवाई में मुआफ़
आज कुछ दर्द मिरे दिल में सिवा होता है
मुआमला यह है कि इन विसंगतियों और लालच के मायाजाल में अगर बात साहित्यिक दुकानदारों तक सीमित रहती तो इतना दुख नहीं होता क्योंकि बक़ौल शकील बदायुनी :
मेरा अज़्म इतना बलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं
मुझे ख़ौफ़ आतिश-ए-गुल से है ये कहीं चमन को जला न दे
प्रगतिशील/जनवादी आंदोलन में शामिल होकर सज्जाद ज़हीर ने अपनी सुख-सुविधाएँ और ज़मीन-जायदाद छोड़ दी तो फ़ैज़, सरदार जाफ़री और मजरूह जैसे शाइरों ने जेल की सलाख़ों के पीछे का उत्पीड़न झेला। और इन सबके अगुवा प्रेमचंद फटे जूते पहनकर अदब (साहित्य) की सेवा में अपनी बेटी का मुनासिब इलाज भी नहीं करवा सके। लेकिन इन सबकी बैसाखी का सहारा लेकर हमारे ‘लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों’ का एक ऐसा रेला आया कि जो सारे मंज़रनामे पर ऐसा छा गया कि अदब पर राय ही नहीं फ़रमान जारी करने का हक़ भी अपने हाथों में ले लिया। बक़ौल हबीब जालिब :
जिनको जहाँ का दर्द वो मादूद-ए-चंद हैं
बाक़ी तमाम, ‘‘अपनी तरक़्क़ी पसंद’’ है
आप अपने इर्द-गिर्द भी नज़र दौड़ाएँगे तो जनवाद और प्रगतिशीलता के नाम पर ‘अपनी तरक़्क़ी’ करने वाले असंख्य महारथी मिल जाएँगे।
इस लंबी भूमिका के लिए माफ़ी, लेकिन इसका संदर्भ यह है कि पिछले दिनों साहिर लुधियानवी काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि सारी दुनिया के साहित्यप्रेमियों ने उनके शताब्दी वर्ष का जश्न मनाया। ज़ाहिर है कि साहिर की शाइरी दबे-कुचले, शोषित समाज और मानवाधिकारों की आवाज़ को बलंद करने वाली ऐसी शाइरी है जो तक़रीबन सारे उर्दू और हिंदी पाठकों को न सिर्फ़ समझ में आती है, बल्कि उनके दिलों उतर कर उन्हें आंदोलित भी करती है। साहिर छात्रों, मेहनतकशों और किसानों-मज़दूरों के बीच इस क़दर मक़बूल थे कि उनकों सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ता था। लेकिन साहिर ने यह अधिकार किसी को नहीं दिया कि वे लोग जो साहिर की काव्य-भाषा उर्दू से नावाक़िफ़ हैं और उनकी सांस्कृतिक विरासत ही नहीं बल्कि उसकी बारीकियों से भी नावाक़िफ़ हैं, वे साहिर को अपनी शोहरत और तिजारत का ज़रिया बनाएँ।
मेरे सामने ‘जाग उठे ख़्वाब कई’ नाम से नागरी लिपि में छपी एक किताब है, जिसमें साहिर की शाइरी और उनके फ़िल्मी गीतों का संकलन किया गया है और जिसे पेंगुइन बुक्स और यात्रा बुक्स ने 2010 में छापा है। यह किताब मेरे एक मित्र ने पिछले दिनों मुझे भिजवाई। इस किताब का संचयन-संपादन, मुरलीमनोहर प्रसाद सिंह, कांतिमोहन ‘सोज़’ और रेखा अवस्थी ने किया है तथा प्रस्तावना गुलज़ार ने लिखी है। इनके नाम प्रमुखता के साथ किताब के कवर पेज पर दिए गए हैं। किताब के अंदर के पेज पर उर्दू से लिप्यंतरण करने वाले का नाम एम. ए. ख़ालिद है।
विडंबना यह है कि अगर एम. ए. ख़ालिद ने उर्दू से नागरी में लिप्यंतरण न किया होता तो प्रकाशन संभव ही नहीं था यानी साहिर की शाइरी को नागरी लिपि जानने वाले पाठकों तक पहुँचाने का मुख्य श्रेय तो ख़ालिद को जाता है, लेकिन मुख्य पृष्ठ तो दूर किताब के संपादन का कॉपीराइट मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, कांतिमोहन ‘सोज़’ और रेखा अवस्थी का है। इस खुली जालसाज़ी और साहित्यक डकैती के लिए प्रकाशकों को जो माली मुनाफ़ा हुआ वह अपनी जगह पर, मुरली जी, कांतिमोहन ‘सोज़’ और रेखा अवस्थी की किटी में कितनी मुद्रा हाथ आई उसका अंदाज़ा प्रकाशकों के नाम से लगाया जा सकता है। एम. ए. ख़ालिद के हाथ क्या आया, कहना मुश्किल है। सिर्फ़ इतना कहा जा सकता है कि :
दुख सहें बी-फ़ाख़्ता, कौवे अंडे खायं
उर्दू में किताबत का रिवाज तो है, पर यह काम अब कम्प्यूटर ऑपरेटर करता है, लेकिन एक भाषा की लिपि से दूसरी भाषा की लिपि में करने का काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए दोनों भाषाओं की लिपियों का ज्ञान होना ज़रूरी है और यही अस्ल काम की श्रेणी में आता है। यह बात हिंदी और उर्दू के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुरलीमनोहर प्रसाद सिंह और रेखा अवस्थी को उर्दू लिपि लिखना, पढ़ना और समझना नहीं आता। कांतिमोहन के बारे में कहा जाता है कि वह उर्दू से वाक़िफ़ ही नहीं बल्कि उर्दू में शायरी भी करते हैं। इस दावे की सार्थकता का मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है और मेरी राय में उनको भी उर्दू नहीं आती। उनका यह दावा कि उर्दू के बड़े लेखक मोहम्मद हसन साहब से उन्होंने उर्दू सीखी है, यह उसी तरह है जैसे किसी संस्कृत के विद्वान के साथ चंद रोज़ बैठने के बाद मैं यह दावा करूँ कि मुझे संस्कृत आती है। और अगर कांतिमोहन ‘सोज़’ को उर्दू आती है तो लिप्यंतरण का काम किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया जो इस क़ाबिल भी नहीं था कि कवर पेज पर उसका नाम दिया जा सके।
उर्दू के साथ मुआमला ये है :
दीवार क्या गिरी मेरे टूटे मकान की
लोगों ने मेरे सह्न से रस्ते बना लिए
दरअस्ल, 1947 में आज़ादी और देश-विभाजन के बाद एक बड़ा सांप्रदायिक गिरोह उर्दू को न सिर्फ़ विदेशी भाषा बल्कि विभाजन के लिए ज़िम्मेदार ठहराता रहा है और मुसलमानों की ज़बान के रूप में प्रचारित करता रहा है। यहाँ विस्तार में जाने के बजाय इतना कह देना काफ़ी है कि किसी भी भाषा को किसी धर्म विशेष के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता और जहाँ तक उर्दू का सवाल है, यह तो हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की बेहतरीन मिसाल है और हर तरह की धार्मिक संकीर्णता के ख़िलाफ़ इसका साहित्य भरा पड़ा है।
यह भी सच है कि इस संकीर्ण और सांप्रदायिक विचारधारा के ख़िलाफ़ हमारे प्रगतिशील/जनवादी विचारधारा रखने वाले साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और उर्दू को इस भू-भाग की साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा क़रार दिया और इसीलिए मीर, ग़ालिब, इक़बाल, फ़ैज़, मजरूह और साहिर आदि शाइर हमारी विरासत का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर उर्दू भाषा और साहित्य के साथ जो व्यवहार किया गया है, वह निंदनीय है। इसमें हमारे कुछ प्रगतिशील बुद्धिजीवी भी उसी संकीर्ण प्रचार का शिकार ज़रूर हुए, लेकिन प्रगतिशील/जनवाद से संबद्ध ज़्यादातर लेखक उर्दू को उसका जायज़ हक़ दिलवाने के लिए पहले भी पेश-पेश थे और अब भी हैं। लेकिन इसी प्रगतिशीलता और जनवाद की आग में रोटियाँ सेंकने वाले भी कम नहीं हैं। हर तरह की विपरीत परिस्थितियों और सरकार के दुश्मनी भरे रवैयों के बावजूद उर्दू आज भी अपनी सार्थकता और अहमियत मनवाने में कामयाब है और उर्दू के शाइरों-लेखकों की कृतियाँ नागरी लिपि में छपकर हिंदी पाठकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हैं।
यहाँ मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आज़ादी के बाद जैसे बहुत सारे छद्म स्वतंत्रता-सेनानी पैदा हो गए, उसी तरह उर्दू पर ‘अपार मेहरबानी और संरक्षक’ बनने के दावेदारों की भी भरमार हुई जो मुरलीमनोहर प्रसाद, कांतिमोहन ‘सोज़’ और रेखा अवस्थी द्वारा ‘संचयित’ इस ‘कारनामे’ के रूप में सामने आई है। अँग्रेज़ी में एक जुमला इस्तेमाल होता है, जिसे हम नेम ड्रापिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ भी कुछ बड़े नामों का रोब डालने की कोशिश की गई और गुलज़ार जैसे फ़िल्मी शाइर की प्रस्तावना और अनुराग कश्यप के विचार शामिल किए गए हैं। अनुराग कश्यप को तो उर्दू जानने का दावा नहीं है, लेकिन गुलज़ार उर्दू के लेखक होने का दावा ज़रूर करते हैं। उनकी उर्दू की जानकारी के अनेक ऐसे नमूने मिल जाएँगे जो मज़ाक़ का पात्र बनते हैं, उन पर फिर कभी बातें होंगी, लेकिन इस किताब में गुलज़ार साहब की प्रस्तावना का पहला शब्द है : ‘तज़रूबा’ है जबकि यह शब्द ‘तजरबा’ है। अगर मान लिया जाए कि यह कम्प्यूटर की ग़लती हो सकती है तो आगे वो ‘ख़ास व आम’ लिखते हैं, जबकि उर्दू में ‘ख़ास-ओ-आम’ लिखा जाता है। बैक पेज पर पाँचवी लाइन में ‘इंसानी जज़्बातों’ लिखा गया है। कोई भी उर्दू जानने वाला ‘जज़्बातों’ लिख ही नहीं सकता। यह अलग बात है कि उर्दू से नावाक़िफ़ लोग ऐसा लिखते और बोलते हैं, लेकिन गुलज़ार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ इसके दो ही मतलब निकाले जा सकते हैं : या तो यह ड्राफ़्ट गुलज़ार को दिखाया नहीं गया और अगर दिखाया गया है तो उनके उर्दू-ज्ञान पर शक होना लाज़मी है।
मुझे हैरत इस बात पर है कि पेंगुइन और यात्रा जैसे प्रकाशक ने इस बात को सुनिश्चित नहीं किया कि संचयन, संपादन करने वालों को उर्दू का ज्ञान है या नहीं। जैसा कि मुरलीमनोहर प्रसाद सिंह ने अपनी भूमिका में ज़िक्र किया है कि इस प्रकाशक को किताब छापने के लिए रज़ामंद करने में सत्यानंद सिंह निरुपम और रवि सिंह की अहम भूमिका रही है और मुरली जी के शब्दों में, ‘‘अगर ये लोग मेरे प्रस्ताव पर अविलंब क़दम नहीं उठाते और गहरी अभिरुचि न लेते तो संभव है कि इस सजधज के साथ तथा इतनी जल्दी यह पुस्तक पाठकों को पढ़ने के लिए मिलती ही नहीं।’’
मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं कि इतने बड़े प्रकाशन समूह से रिश्ता रखने वाले सत्यानंद सिंह निरुपम और रवि सिंह की निष्ठा ही नहीं, बल्कि अपने प्रकाशन समूह के साथ उनकी ईमानदारी पर भी यहाँ प्रश्नचिह्न क़ायम होता है।
इसी किताब में साहिर लुधियानवी की एक बहुचर्चित ऩज्म ‘जश्ने-ग़ालिब’ के शीर्षक से है। इस नज़्म में साहिर कहते हैं :
उर्दू के तअल्लुक़ से कुछ भेद नहीं खुलता
ये जश्न, ये हंगामा, ख़िदमत है कि साज़िश है
या
ग़ालिब जिसे कहते हैं, उर्दू ही का शाइर था
उर्दू पे सितम ढाकर, ग़ालिब पे करम क्यूँ है
इस नज़्म का आख़री शेर है :
गांधी हो के ग़ालिब हो, इंसाफ़ की नज़रों में
हम दोनों के क़ातिल हैं, दोनों के पुजारी है
मुरली जी, कांतिमोहन जी और रेखा अवस्थी जी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ से लंबे अरसे तक जुड़े रहे हैं, बल्कि मुरली जी कई बरसों तक शिक्षक संघ के पदाधिकारी (दो बार अध्यक्ष) भी रहे हैं। उनके रहते हुए हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, ख़ालसा कॉलेज से उर्दू के विभाग बंद कर दिए गए। इनकी लीडरशिप में उर्दू विभागों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या क़दम उठाए गए, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। जिस कॉलेज में मुरली जी ख़ुद अध्यापक थे यानी स्कूल ऑफ़ करस्पांडेंस या अब कॉलेज ऑफ़ ओपन लर्निंग और लेडी श्रीराम कॉलेज में उर्दू विभाग बंद होने के कगार पर हैं। इस सिलसिले में इन साहित्यकारों और उर्दू प्रेमियों का क्या योगदान रहा है, अगर मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे तो ख़ुशी होगी।
यहाँ जिस किताब का ज़िक्र हो रहा है, उस पर वापस आते हैं। मुरली जी के उर्दू-ज्ञान की कुछ मिसालें देखिए। भूमिका में पहले पन्ने पर उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे : ख़्याल, ख़्यालों, जज़्बातों जबकि सही शब्द इस तरह हैं : ख़याल, ख़यालों और जज़्बात। आगे पृष्ठों पर तहरीक़ लिखा है, जबकि सही लफ़्ज़ तहरीक है यानी क के नीचे बिंदी नहीं है। यह अगर एक जगह होता तो कम्प्यूटर की भूल मानी जा सकती थी, लेकिन यह शब्द इसी ग़लत तरीक़े से कई जगह दुहराया गया है। इसी तरह दकनी को दक़नी, मरकज़ को मरक़ज, सरदार जाफ़री को सरदार ज़ाफ़री, मजाज़ को मज़ाज़, तख़य्युल को तख़्य्युल, बलंद को बुलंद, रिफ़्यूजी को रिफ़्यूज़ी, ख़य्याम को ख़्ययाम, क़ूव्वत को क़ुव्वत लिखा गया है।
हमारे गाँव में कहते हैं : ‘‘नया नमाज़ी, फुलौरी की तस्बीह!’’
इसके अलावा उर्दू के शब्दों को नागरी में लिखने के अलग-अलग तरीक़े हो सकते हैं। लेकिन जो तरीक़ा अपनाया जाए उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जैसे दीवान-ए-ग़ालिब और दीवाने-ग़ालिब। दोनों तरीक़े ठीक हैं, लेकिन फिर पूरी किताब में यकसानियत होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं किया गया। वैसे पहला तरीक़ा ज़्यादा बरता जाता है, क्योंकि दीवाने-ग़ालिब इसलिए अटपटा लगता है, जैसे : ग़ालिब दीवाने हो गए हों। इसी तरह जब उर्दू के शब्दों का लिप्यंतरण हो रहा है तो आपको यह हक़ नहीं है कि उर्दू के शब्दों का उच्चारण ही बदल दें, जैसा कि हमारे फ़ाज़िल बुद्धिजीवी ने किया है। भूक को भूख और पौदे को पौधा करके। इन शब्दों को जिस रूप में उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उसी रूप में रहने देना चाहिए था, ताकि उर्दू ज़बान की चाशनी बनी रहे।
मेरी बातें लंबी होती जा रही हैं, इसलिए चंद बातों की तरफ संक्षेप में इशारा करता हूँ। मूल टेक्स्ट में उच्चारण की ग़लतियों के साथ एम. ए. ख़ालिद भी उर्दू ठीक से पढ़ नहीं पाए, इसलिए उनकी उर्दू की जानकारी पर भी शक होता है। मिसाल के तौर पर साहिर की एक ऩज्म ‘कुछ बातें’ के उन्वान से पेज 19 पर है। इसकी पहली पंक्ति में एक शब्द ‘ओबार’ लिखा है। मैंने अपनी जानकारी के लिए कई शब्दकोश तलाश किए, लेकिन यह शब्द कहीं नहीं मिला। फिर मैंने नज़्म को उर्दू में पढ़ा तो पता चला कि ‘इदबार’ शब्द को ‘ओबार’ कर दिया है, यानी ख़ालिद साहब को ठीक से उर्दू पढ़नी नहीं आती। इसके अलावा अपने उर्दू-ज्ञान का दावा करने वाले कांतिमोहन ‘सोज़’ को टेक्स्ट पर नज़र तो डालनी ही चाहिए थी।
इसके साथ ही यह भी कहना ज़रूरी है कि मुरलीमनोहर प्रसाद सिंह ने भूमिका लिखते वक़्त किन सोर्सेज़ का सहारा लिया है, इसका उल्लेख ज़रूर करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि अलग-अलग किताबों में साहिर की जीवनी पर उर्दू में जो लेख लिखे गए हैं, उन्हें पढ़वाकर कतर-ब्योंत (कटिंग-पेस्टिंग) करके जानकारियाँ एकत्रित कर दी गई हैं।
अंत में, मैं भी एक दावा करना चाहता हूँ। वह यह कि मुरली जी अपनी लिखी हुई भूमिका को पढ़कर अगर उसमें आए शब्दों का सही उच्चारण कर दें तो मैं अपनी सारी आपत्तियाँ आम माफ़ी के साथ वापस ले लूँगा। लेकिन मुरली जी से और तमाम उर्दू-प्रेमियों से निवेदन है कि उर्दू और उर्दू शाइरी को इतने हल्के में न लें और इसे अपनी बेजा शोहरत का ज़रिया न बनाएँ, वरना प्रगतिशील/जनवादी आदर्शों और तिजारत-व्यापार करने वालों में फ़र्क़ ही क्या रह जाएगा!






