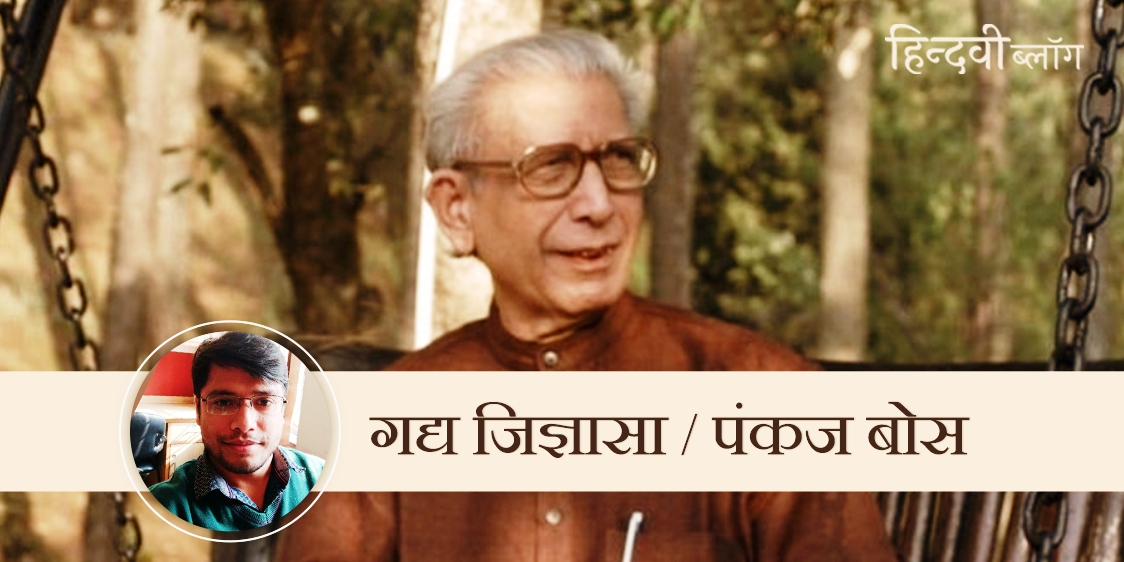
संस्मरण की पाँचवीं पद्धति
 पंकज बोस
जनवरी 31, 2021
पंकज बोस
जनवरी 31, 2021
ग़ालिब, अपना यह ‘अक़ीदः है, बक़ौल-ए-नासिख़
आप बेबहरः है, जो मो‘तक़िद-ए-मीर नहीं
हिंदी समाज में किसी बड़े साहित्यकार की मृत्यु के बाद उन्हें कम से कम पाँच पद्धतियों से याद किया जाता है। औपचारिक स्मरण के अलावा बहुत से लोग अत्यंत विनम्र और सदाशय होकर उनकी महानता को याद करते हैं और इसे एक बड़ी क्षति के रूप में देखते हैं। कुछ उनके साथ अपने आत्मीय और घनिष्ठ संबंधों को ज़ाहिर करते हुए यह भी जतलाते हैं कि वे स्वयं ‘उनके’ लिए बेहद महत्त्वपूर्ण रहे हैं, और ‘उनकी’ अनुपस्थिति के बाद अपनी उपस्थिति को एक प्रासंगिक और महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में पेश करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लगभग उदासीन रहते हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त करना ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि अपने भीतर कहीं एक विराट शून्य महसूस करते हैं। अपवाद स्वरूप ऐसे भी मिलेंगे जो सचमुच अनुभव करते हैं कि एक-एक कर सब प्रस्थान कर रहे हैं और निकट भविष्य में अगली बारी उनकी भी हो सकती है। ऐसा सोचते हुए वे अपने व्यवहार में पहले से अधिक विनम्र, शांत और गंभीर हो जाते हैं। एक प्रजाति ऐसी भी है जो उन्हें लेकर अपनी दबी हुई ग्रंथियों को बाहर निकालना शुरू कर देती है और सायास कुछ चौंकाने वाले प्रसंगों को इस प्रकार सामने लाती है मानो हिरण्मय पात्र से ढके हुए और सदियों से संचित उसके सत्य का मुख आज ही खुला है। इस प्रजाति के लोग कुछ समय तक अपने इस पात्र को क्रमशः धीरे-धीरे उलीचते रहते हैं। कालांतर में हम उन्हें भूल जाते हैं।
हमारे समय के शिखर आलोचक नामवर सिंह की मृत्यु के बाद भी कमोबेश ये पद्धतियाँ देखी गईं, लेकिन गए दिनों ‘समालोचन’ ब्लॉग पर प्रकाशित शिवमंगल सिद्धांतकर का संस्मरण उक्त पाँचवीं पद्धति का सबसे ताज़ा उदाहरण है। संस्मरण का मूल शीर्षक है ‘अंतर्विरोधों का सामंजस्य’ और उसके ऊपर संभवतः संपादकीय प्रस्तुति वाला दिया गया पूरक शीर्षक है—‘ऐसे थे नामवर सिंह’। ‘अंतर्विरोधों का सामंजस्य’ तो फिर भी तार्किक लगता है, लेकिन जो सतही और बचकाना पूरक शीर्षक दिया गया है, उसका क्या! पूरक शीर्षक चाहे लेखक की ओर से दिया गया हो या संपादक की ओर से, वह सामग्री की अंतर्वस्तु को देखते हुए लेखकीय प्रस्तुति या संपादकीय विवेक के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। जिसने संस्मरण लिखने की और जिसने उसे प्रकाशित करने की ज़िम्मेदारी ली है, क्या वह यह बतलाना चाहता है कि ऐसे ‘ही’ थे नामवर सिंह! क्या उसकी ध्वनि यह है कि उसने जैसा देखा, दूसरे लोग भी वैसा ही देखें? कि जो हमारा सत्य है वही एकमात्र सत्य है, दूसरों का सत्य सत्य नहीं है! वस्तुतः बौद्धिक या लेखकीय प्रक्रिया से अधिक यह पाठकों को आकर्षित करने की एक मनोवैज्ञानिक रणनीति का उदाहरण है।
यह ‘समालोचन’ का अपना विवेक हो सकता है, किंतु किसी समालोचक का विवेक नहीं हो सकता। ध्वनि यह भी है कि किसी संपादक में हमेशा एक समान आलोचनात्मक विवेक सक्रिय हो, यह क़तई ज़रूरी नहीं। संपादकों की नियति होती है कि कभी वह आलोचना के उच्च मानकों से लैस होकर काम करता है और कभी सस्ती लोकप्रियता या कोई विवाद पैदा करने का श्रेय लेने के लिए सनसनीख़ेज़ सामग्री प्रकाशित करता है या कभी निजी आग्रहों-रुचियों के अनुकूल या प्रतिकूल जाकर भी उसे ऐसा करना पड़ता है। एक समृद्ध ब्लॉग की, जिसने एक प्रतिष्ठित पत्रिका जैसी ख्याति अर्जित कर ली है, ऐसी हल्की और लोक-लुभावनी प्रस्तुति देखकर आश्चर्य होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक नियमित पाठक के रूप में अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी ख़ूबियाँ तो ख़ूब हैं और प्रशंसक भी बहुतेरे हैं; लेकिन कमियाँ बताने वाले कम से कम हैं, न के बराबर। हम उसके मानकों को गिरते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
समस्या किसी के संस्मरण लिखने या उसे प्रकाशित करने से नहीं है, बल्कि यह है कि किसी रचना से ध्वनित होने वाले किन मूल्यों को हम व्यापक पाठक जगत के सामने ला रहे हैं? दूसरी यह कि क्या संस्मरण जैसी विधा में—जो आमतौर पर साहित्य में मुख्यधारा की विधा नहीं मानी जाती—कुछ भी लिख देने से, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ देने भर से लेखक अपनी ज़िम्मेदारी से छुट्टी पा जाता है? जबकि किसी बड़े साहित्यकार का मूल्यांकन या उसकी स्मृतियों का अंकन भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है तो क्या अपने विवेच्य या स्मृत्य विषय को लेकर हमारी नैतिक भूमिका में अधिकतम गंभीरता और निष्पक्षता अपेक्षित नहीं है? उक्त संस्मरण को आरंभ करते हुए लगता है कि सिद्धांतकर एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन पूरा पढ़ लेने के बाद अंततः उस पर मैथिलीशरण गुप्त की यही पंक्ति चरितार्थ होती लगती है—“वह नवनीत कहाँ जाता है / रह जाता है तक्र!”
आख़िर ज़िम्मेदारी क्या है? किसी साहित्यकार की मृत्यु के बाद उसके स्वस्थ आकलन-मूल्यांकन की और नई पीढ़ी के लिए एक संतुलित परिदृश्य उपस्थित करने की ज़िम्मेदारी। एक बार जब किसी आयोजन में अमीर ख़ुसरो पर बोलने के लिए शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी को आमंत्रित किया गया तो उन्होंने छूटते ही कहा, “ज़माने में बड़े लोगों के मरने के बाद छोटे लोग भी बड़े बना दिए जाते हैं।” उनका आशय था कि कहाँ ख़ुसरो और कहाँ मैं! भला मैं क्या बोलूँगा! लेकिन वह बोले और ख़ूब बोले। अदबी दुनिया में ख़ुद फ़ारूक़ी के बड़प्पन को शिद्दत से महसूस किया गया है। लेकिन जब वह यह बोल रहे थे तो अमीर ख़ुसरो के बड़प्पन के प्रति झुके हुए थे। ख़ुसरो की महानता के स्वीकार की भावना से उनमें एक दुर्लभ विनम्रता देखी गई, और ऐसा एक नहीं अनेक मौक़ों पर देखा गया। इसका मतलब यह नहीं कि वह अवसर के अनुकूल बोल रहे थे, बल्कि यह कि उनके व्यक्तित्व की अंतर्धारा में ही यह घुली हुई थी। फ़ारूक़ी की विनम्रता उनका कातर होना नहीं, बल्कि एक सागर की विनम्रता थी जिसमें अगाध जल होता है। चूँकि उसमें अनंत गहराई होती है, इसलिए उसकी लहरें छोटी नालियों-नदियों की तरह मचलती और बलखाती नहीं हैं। ऊपर से उनमें शांत और मंथर प्रवाह दिखता तो है, पर भीतर कहीं त्वरा, काट और क्षिप्रता होती है; जहाँ लहरें एक दूसरे को काटती रहती हैं। यह बिजली की विनम्रता होती है। ज़िम्मेदारी की मूल भूमि यही है।
पिछ्ला वर्ष केवल साहित्य के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरी कलाओं और मूलतः पूरी मानव सभ्यता के लिए महानतम शोक का वर्ष साबित हुआ है। मानवीय अस्तित्व के संकट के इस शोक का एक छोटा हिस्सा हमारे साहित्यकारों और कलाकारों की मृत्यु का शोक भी है। जीवन और साहित्य के अनेकानेक विषयों के साथ यह शोक भी जब श्रद्धांजलि में, और श्रद्धांजलि प्रदर्शन में रूपांतरित होने लगी तो वेबिनार और लाइव के रूप में जमा हुआ लाखों टन ई-कचरा। वैसे संयुक्त राष्ट्र की ‘ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर’ के अनुसार इस शोक वर्ष में भारत में तीन मिलियन टन से भी अधिक ई-कचरे का आकलन किया गया जिसके सबसे बड़े केंद्र हमारे महानगर रहे। हालाँकि यह नहीं बताया गया कि बेतहाशा बढ़ने वाले ई-कचरे के इस वायुमंडल में असंख्य क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंडों का भी उदय हुआ है, जो एकबारगी कुछ डराते और चौंकाते हुए प्रकट होते हैं; लेकिन अंततः अपनी ही आग में जलते-भुनते हुए नष्ट हो जाते हैं।
इसी परिदृश्य में साहित्यिक व्यक्तित्वों, प्रसंगों और मुद्दों को नितांत अगंभीरता से लेने का चलन बढ़ने लगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ‘उच्छृंखलता के अतिवाद’ की संस्कृति तीव्रता से विकसित हुई। संस्कृति नहीं, विकृति। एक अराजक, अनुभवहीन और स्मृतिहीन होते समय में शायद ऐसा ही संभव है! साहित्य शेयर बाज़ार तो नहीं है, लेकिन इस शोक-वर्ष में अभिव्यक्ति की गुणवत्ता के सूचकांक में तेज़ी से गिरावट आई है। यह व्यापक साहित्यिक मंदी का दौर है। बिचौलिए मुनाफ़ा लूट रहे हैं और बाज़ार में जश्न मना रहे हैं। एक तरह से सोचें तो वास्तव में यह बड़े लोगों के मरने के बाद छोटे लोगों को बड़ा बना दिए जाने का समय है। शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी ने जिस बात को विनम्रता में कहा था, वह इस समय एक भयानक विसंगति के रूप में घटित हो रही है : बड़ी चतुराई से ‘बड़े लोग’ ‘छोटे लोगों’ द्वारा अपदस्थ किए जा रहे हैं।
हम पहले एक पैटर्न बनाते हैं—साहित्य, कला और अकादेमी की दुनिया में जो बड़े क़द का आदमी है, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं; लाभ-लोभ की आशा में उसके पिछलग्गू बने फिरते हैं, उसके जीवन-काल में उस पर प्रशंसात्मक लेख तथा मूल्यांकनपरक पुस्तकें लिखते हैं, और महान संस्मरण प्रकाशित करते हैं। फिर उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद एक दूसरा पैटर्न बनाते हैं—असामयिक को सामयिक, अप्रासंगिक को प्रासंगिक और अयोग्य को योग्य के रूप में प्रोजेक्ट करने की रणनीति करते हैं। शिवमंगल सिद्धांतकर का संस्मरण कमोबेश इसी पैटर्न पर लिखा गया है और प्रकाशित हुआ है। आज आप विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडेय और अशोक वाजपेयी आदि के सम्मान में लिखते और प्रकाशित करते हैं तो क्या इनके बाद जब साहित्याकाश में अपने-अपने छद्म सत्यों के हिरण्मय पात्र वाले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह अचानक प्रकट होने लगेंगे तो इन पर भी ऐसे छिछले संस्मरण नहीं लिखे जाएँगे? नहीं छापे जाएँगे?
किसी भाषा के बड़े रचनाकारों की मृत्यु उस समाज में बहुतों के लिए एक क्षति का अनुभव होती है तो बहुतों के लिए उनकी यादगारी या श्रद्धांजलि किसी उत्सव की तरह जिसे वे सेलिब्रेट करते हैं। हम दो पैटर्न बनाते हैं जिसमें एक बार अपने पूज्य पुरुषों के रहते हुए ‘भक्ति’ और दूसरी बार उसके न रहते हुए ‘उत्सव’ को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार कहलाना तो प्रगतिशील चाहते हैं, लेकिन एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से चालित होकर अपनी दमित आकांक्षाओं के सतह पर आने की सतत प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसके बाद जो बचे हुए हैं और इस पैटर्न में शामिल नहीं हैं, वे ‘क्षति-बोध’ और ‘उत्सव-आनंद’ के दो अतिवादी छोरों के बीच जीने के लिए अभिशप्त हैं।
सवाल यह नहीं है कि सिद्धांतकर ने ऐसा संस्मरण क्यों प्रस्तुत किया, बल्कि यह कि उन्होंने संकीर्ण और विकृत मानसिकता के वशीभूत होकर प्रस्तुत किया है। निजी जीवन या संबंधों में संगतियाँ-विसंगतियाँ कहाँ नहीं होतीं! होती हैं, लेकिन अंततः वे ‘व्यक्तिगत इतिहास’ की वस्तु होती हैं। जबकि किसी बड़े लेखक-आलोचक द्वारा छोड़ी गई उपलब्धियाँ वस्तुतः ‘सांस्कृतिक इतिहास’ की संपदा होती हैं तो वैसे संस्मरण में जिसमें एक व्यक्ति के साथ-साथ एक आलोचक को भी याद किया गया हो, ‘सांस्कृतिक इतिहास’ की सायास उपेक्षा क्यों? और संस्मरण में भी केवल स्याह पक्ष का बखान क्यों? एकपक्षीय वर्णन क्या संतुलित कहा जाएगा, क्या यह ख़ुद संस्मरणकार—यदि सच्चे अर्थों में वह है तो—की एकांगिकता का प्रमाण नहीं है? क्या किसी बड़े लेखक को उसकी मृत्यु के बाद एक पूर्व समकालीन द्वारा ऐसे याद किया जाता है? यदि याद करने का आपका यही तरीक़ा है तो ज़रा सोचिए कि फिर आपके बाद भी आपके बारे में याद करने लायक़ क्या बचा रह जाएगा?
किसी भी संस्मरण में मार्मिकता आती है—अपने पात्र के आत्मीय सामीप्य से, सुदीर्घ साहचर्य से और उसके जीवन और चरित्र के सूक्ष्म अवलोकन से। इसके बाद यदि उसकी आलोचना भी की जाए तो सर्जनात्मक धरातल पर चरित्र के उद्घाटन की दृष्टि से वह सोद्देश्य होगी। यों कोई चाहे तो सूरदास के ‘भ्रमर-गीत’ को भी गोपियों के संस्मरण के रूप में पढ़ सकता है, जहाँ उनकी उलाहना भी कृष्ण के चरित्रोद्घाटन के साथ-साथ एक उदात्त काव्य-वस्तु के रूप में कायांतरित हो जाती है। अगर ऐसा प्रेम हो तो कोई भी पात्र उलाहना के लिए लालायित रहेगा, अपनी आलोचना की कामना करता रहेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि महादेवी वर्मा ने अपनी कृति का नाम ‘पथ के साथी’ रखा है, जो संस्मरण विधा की मूल प्रकृति या स्मृति-प्रक्रिया की सबसे सटीक संज्ञा है। आचार्य शुक्ल ने गोपियों की स्मृति-प्रक्रिया के पीछे जिस ‘साहचर्य’ को लक्षित किया है, महादेवी के संस्मरणों में वही ‘साथी’ के रूप में उजागर हुआ है। महादेवी के अलावा दिनकर या अज्ञेय के संस्मरण या निराला पर रामविलास शर्मा के स्मृति-लेखन को भी हम मानक के तौर पर देख सकते हैं।
अज्ञेय ने अपनी ‘स्मृति-लेखा’ में “निराला इज़ डेड!” वाला जो प्रसंग बतलाया है, फिर निराला से अगली मुलाक़ात और पुस्तक के दूसरे संस्करण की भूमिका में इस संबंध में जो कहा है, उससे प्रमाणित होता है कि संस्मरण में भी समय के साथ परिष्कार होता है, किंतु कभी-कभार कोई विरला ही इस परिष्कृति के लिए प्रस्तुत हो सकता है। वरना जो अपने को ब्रह्म और अपने लिखे को ब्रह्मवाक्य मानकर बैठे हैं, उनका तो स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते! अज्ञेय ने ‘स्मृति-लेखा’ की भूमिका में एक और बात लिखी है : “…माध्यमों ने आज जिस नए प्रकार के काल का निर्णय किया है—एक बहुत छोटे-से आयाम वाले वर्तमान का, जो स्वयं तो अतिप्रकाशित है, लेकिन जिसके आगे-पीछे अँधेरा है—उस काल में जीने वालों के लिए ऐसे श्लाका-पुरुषों की प्रतिमाएँ भी धूल से ढक जाती हैं। ‘स्मृति-लेखा’ ने प्रतिमाएँ फिर से गढ़ी नहीं, केवल उन पर पड़ी धूल झाड़ने का एक अवसर मुझे दिया।” संस्मरण अवसर देते हैं—यह एक स्थिति है जहाँ ख़ाली हाथ, कुछ पाने की उम्मीद से पहुँचना होता है। लेकिन जब कोई यह सोचे कि संस्मरण को वह अवसर दे रहा है या प्रतिमाएँ गढ़ रहा है—तो यह बिल्कुल दूसरी स्थिति है जहाँ वह अपने अहम्, क्षुद्रताओं और ग्रंथियों में जकड़ा हुआ पहुँचता है। भूमिका के अंत में अपने अग्रजों को प्रणाम करते हुए वे लिखते हैं : “आशा करता हूँ कि कि यह पुस्तक नए पाठकों को भी उनके व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की ओर आकृष्ट करेगी। वे रचनाएँ हमारे साहित्य की पूँजी हैं और पूँजी का लगातार नया विनियोग होता रहे, तभी उससे समाज की समृद्धि होती है।” ये हैं अज्ञेय : और यह है संस्मरण-कला में मार्मिकता के स्रोतों की उनकी बेचैन खोज। क्या आज के संस्मरण लेखकों के लिए अज्ञेय के इन शब्दों का कोई मूल्य रह गया है?
सिद्धांतकर का यह संस्मरण न ठीक-ठीक संस्मरण है और न ठीक-ठीक आलोचना, अगर कुछ है तो केवल उनका विष-वमन। अंतर्वस्तु के बिखराव से इसका रूप भी बिखर गया है। ‘सतृणाभ्यवहारी’ वृत्ति के अनुकूल कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से लेकर जोड़ने की कोशिश की तो गई है; लेकिन एक-एक चित्र विरूपित हो गया है। अंततः यह एक टूटा हुआ दर्पण है जिसमें ख़ुद उनकी आत्मा का चेहरा लहूलुहान और धूलि-धूसरित दिखलाई पड़ता है। उनकी गति अपनी ही आग में जलती हुए उस उल्का की तरह है जो कभी भी भस्म हो जाने वाली है। फ़िलहाल उनकी अधिक आलोचना न करते हुए, एक पाठक के रूप में सुखद अनुभव साझा करता हूँ। ठीक इसी समय जब यह लेख लिखा जा रहा है, ‘आजकल’ के फ़रवरी अंक में नामवर सिंह पर राजेंद्र गौतम का एक स्वस्थ और समृद्ध करने वाला संस्मरण पढ़ने को मिला है। ऐसा लगता है कि साहित्य में भी ‘चेक एंड बैलेंस’ का कोई अज्ञात नियम क्रियाशील रहता है—चाहे सायास हो या अनायास, सौभाग्य से हो या दुर्भाग्य से। अगर आप शिवमंगल सिद्धांतकर का ‘ऐसे थे नामवर सिंह’ के साथ राजेंद्र गौतम का संस्मरण ‘नामवर सिंह : चंद यादें’ पढ़ेंगे तो आपको समझते देर न लगेगी कि ऐसे ‘ही’ नहीं, बल्कि ऐसे ‘भी’ थे नामवर सिंह! ‘ऐसे थे’ में एकाधिकार और अहम् वाली जो चट्टान है, वह ‘चंद यादें’ में आपको टूटती-बिखरती हुई मिलेगी, जहाँ पिछले श्लाका पुरुषों की प्रतिमाओं से धूल झाड़ने का काम किया गया है, क्योंकि संस्मरण ने ऐसा अवसर दिया है। इसलिए यह एक स्वस्थ स्मृति-रचना है। इसमें एक संस्मरणकार के नाते नामवर सिंह के व्यक्तित्व को ढकने या आच्छादित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसे और उजागर किया गया है। जबकि प्रायः लोग संस्मरण लिखते हुए उनकी कम और ‘अपनी’ ही बात अधिक करते हैं और अपने को उनसे बड़ा दिखाना चाहते हैं, उनमें एक तग़ाफ़ुल वाला रवैया मिलता है। पहला संस्मरण जहाँ एक पूर्वकल्पित ‘एंटीथीसिस’ के साथ वस्तु को विकृत करता है, वहीं दूसरा एक ‘सिंथेसिस’ के रूप में उसे पुनः संस्कृत करता है। और यह केवल संयोग है। संभवतः ऐसे संस्मरणों के लिए ही अज्ञेय ने ‘साहित्य की पूँजी के लगातार नए विनियोग’ की बात की है।
अंत में ‘दूसरी परंपरा की खोज’ से एक छोटा-सा प्रसंग। गुरुदेव और हजारीप्रसाद द्विवेदी का। जब गुरुदेव के पास एक विधवा अपनी कन्या के विवाह की समस्या लेकर पहुँची तो उन्होंने द्विवेदी जी को कहा कि ज़रा हिंदुओं के हज़ार वर्षों का इतिहास देखिए और बताइए कि विधवा के ये अधिकार कहीं स्वीकार किए गए हैं या नहीं! उन्होंने स्मृति-ग्रंथों की छानबीन की तो देखा कि “पूर्वपक्ष में ऐसे बहुत से वचन हैं जो विधवा के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं। लेकिन वचनों की संगति लगाते समय निष्कर्ष रूप में यही कहा गया है कि विधवा को ऐसा अधिकार नहीं है। जाकर गुरुदेव को बताया तो हँसकर बोले, ‘क्या पूर्वपक्ष के वे ऋषि कुछ कम पूज्य हैं, जिनका खण्डन उत्तरपक्ष में किया गया है?’” इस प्रश्न ने काशी से नए-नए आए ज्योतिषाचार्य को झकझोर दिया। वह सोचने लगे, “परंपरा क्या उत्तरपक्ष ही है? पूर्वपक्ष नहीं?” और “जिस परंपरा को अब तक वह अखंड समझते आ रहे थे, देखते-देखते शिवधनुष के समान खंड-खंड हो गई।”
आज स्वयं नामवर सिंह हमारे समक्ष पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थित हैं और ऐसे में फिर वही प्रश्न, जो उन्होंने द्विवेदी जी के लिए कहा था, उनके लिए भी प्रासंगिक हो उठा है—क्या उत्तरपक्ष द्वारा खंडित किए जाने पर पूर्वपक्ष के विद्वान अप्रासंगिक हो जाते हैं? यह एक परिप्रेक्ष्य है जो हमें संतुलित दृष्टि प्रदान करता है, परंपरा को एक सामंजस्य और सातत्य में देखने की सीख देता है, और एकांगी आग्रह के प्रति सचेत भी करता रहता है। अब आप पाँचवीं पद्धति पर लिखने वाले किसी भी संस्मरणकार से यह उम्मीद करेंगे कि वह स्वयं अपनी अंतरात्मा से यह प्रश्न पूछे तो ग़लत उम्मीद करेंगे। ऐसा नहीं कि साहित्य के इतिहास में पूर्वपक्ष के प्रति कटुता प्रदर्शन का यह कोई नया प्रसंग है। राहुल और निराला जैसे हमारे अनेक महान साहित्यकारों पर भी जब-तब कीचड़ उछाला गया है, लेकिन दुहराने की ज़रूरत नहीं कि राहुल और निराला जैसों की अपनी परंपरा है और कीचड़ उछालने वालों की अपनी। एक दूसरी ही परंपरा।
ऐसे लेखकों को पढ़ते हुए मुक्तिबोध की कविता के उस ब्रह्मराक्षस का बिम्ब बार-बार उभरता है जो शहर के खंडहर की तरफ़ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अँधेरे में, अनेकों सीढ़ियाँ डूबी हुईं जल की गहराइयों में पैठा हुआ है और अपनी मलिनता दूर करने के लिए पाखंड पर पाखंड किए जा रहा है, और—
घिस रहा है देह
हाथ के पंजे, बराबर,
बाँह-छाती-मुँह छपाछप
ख़ूब करते साफ़,
फिर भी मैल
फिर भी मैल!!
~•~
पंकज बोस हिंदी की नई पीढ़ी के अत्यंत मेधावी आलोचक हैं। ‘हिन्दवी’ के लिए पाक्षिक स्तंभ ‘गद्य जिज्ञासा’ के अंतर्गत देश-विदेश के चुनिंदा रचनाकारों के बहाने साहित्य के सौंदर्य, सिद्धांत और बहसों का विश्लेषण कर रहे हैं। प्रस्तुत लेख के प्रारंभ में उद्धृत शे’र मिर्ज़ा ग़ालिब का है जिसके कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं : अकीदः (अकीदा) = बुनियादी धारणा। बेबहरः (बेबहरा) = मूर्ख। मोतक़िद-ए-मीर = मीर के प्रति श्रद्धा रखने वाला।






