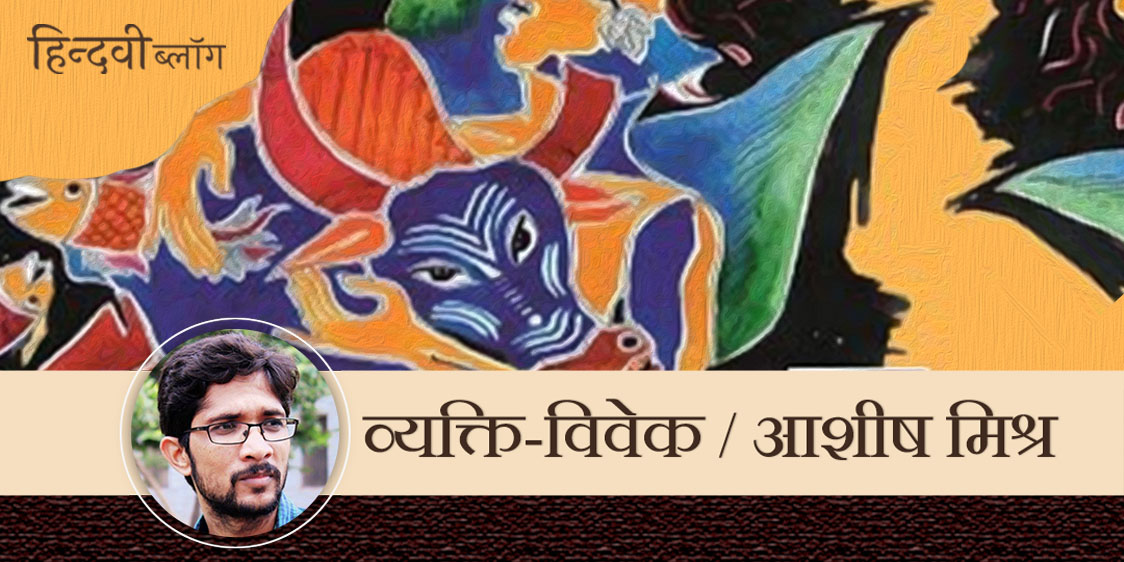
पहचान की ज़मीन पर
 आशीष मिश्र
जनवरी 22, 2021
आशीष मिश्र
जनवरी 22, 2021
नई सदी की राजनीति हमसे हमारी पहचानों के कगारों, किनारों और सीमांतों को ही हमारा स्व-बोध मान लेने का इसरार करती है। कविता उसे घेर-घेरकर जीवन-बोध के मँझधार में लाती है, जहाँ स्व-बोध उदात्त आशय प्राप्त करता है। पहचानों के सीमांत जितने छिछले होते हैं, उतने ही उद्वेलनकारी। मनुष्य की भावनात्मक ऊर्जा का बहुलांश पहचानों के इन्हीं सीमांतों पर होम होता रहता है। युगों-युगों तक मनुष्य का यह भावादोहन धर्म द्वारा किया जाता रहा। आधुनिक समय में अधिक तार्किक और विश्वासप्रद ढंग से यह राजनीति द्वारा होता है, बल्कि आज तो धर्म भी राजनीति का ही एक प्रकल्प है। हर समय की अच्छी कविताएँ भावादोहन की प्रतिक्रिया में मनुष्य के भाव-संसार को केंद्राभिमुख बल की तरह खींचती रहती हैं। मनुष्य को अपने ही दुस्तर दह में उतरने के लिए टेरती रहती हैं। इस दह में सर्वतोन्मुखी प्रवाह है, सार्वदेशिक आवाह है, मनुष्यता के लाखों वर्ष की स्मृतियों की गहराई और सृष्टिपर्यंत विस्तार है। यहाँ से वह धर्म और राजनीति को ठीक उसी रूप में नहीं देखता जैसा कि उसे उसके समय की लोकप्रिय धारणाएँ उसे बताती रहती हैं।
यह कविता का अपना धर्म और अपनी राजनीति होती है। जहाँ व्यक्ति के सारे पहचान और सीमांत घुलकर उसकी मौलिक भावदृष्टि बनते हैं, जो राजनीति से परिभाषित होने के बजाय उसे पुनर्परिभाषित करने की संवेदनात्मक ऊर्जा रखती है। अगर ऐसा नहीं है तो कविता लोकप्रिय राजनीतिक अभिकथन से ज़्यादा क्या होगी? कहना न होगा कि कविता राजनीतिक अभिकथन नहीं, राजनीतिक नवकथन है। कविता की इस नवकथित राजनीति को समझने और पल्लवित करने के लिए राजनीति से अलग औज़ारों और कौशल की ज़रूरत पड़ती है। पिछले तीन दशकों में कविता ने तमाम तरह की पहचानों से लगातार संवाद किया है। इस प्रक्रिया का सुफल अब दिखने लगा है। ज़ाहिर है, इस संवाद में कविता भी कम नहीं बदली है। आज से तीन-चार दशक पहले लैंगिक, वर्णगत और धार्मिक पहचान जितनी सुलझी, सपाट और उत्तेजक थी; उतनी अब नहीं रही, अब एक पहचान और-और पहचानों में सुलझते-उलझते अपने वृत्त का विस्तार करती गई जिससे उसकी दृष्टिगत गहराई बढ़ी और उत्ताप में कमी आती गई। अब वह अपने आत्म को किसी एकल पहचान वृत्त का केंद्र मानने के बजाय अनगिनत पहचानों का प्रतिच्छेदी केंद्र पाती है। उसका भाव-संसार उलझकर थिर हो चुका है। उसमें सत्त के सूत्र बहुत बड़े संदर्भों में सूक्ष्म और उलझे हुए रूप में आते हैं।
हिंदी-कविता में धार्मिक पहचान का आग्रह तो कभी नहीं टिक पाया, लेकिन लैंगिक और जातीय पहचान सामाजिक न्याय के आग्रह के साथ अवश्य मज़बूत हुए। परंतु कविता में न्याय को भी सुंदरता, मनुष्यता, नैतिकता और करुणा के मानवीय सार में ढलना होता है। न्याय के विमर्शों और पहचान की ज़मीन से आने वाली कविताओं के अब तीन दशक बाद नई पीढ़ी में यह बात दिखाई पड़ती है। उन्होंने न्याय को मनुष्यता के अधिक गहन संदर्भों से देखना शुरू कर दिया है। अब स्त्री कविता और दलित कविता की स्थापित श्रेणियाँ नाकाफ़ी हो रही हैं।
हिंदी कविता के भीतर सुरक्षित अंतःपुर की दलित, स्त्री कविता का सुविधाजनक कैनन जुज़ बनकर रह गया है। आज इन श्रेणियों को लाँघकर कितने ही कवि आ गए हैं, जो न तो आलोचना से कोई सुविधाएँ चाहते हैं और न हिंदी आलोचना इनकी उपेक्षा करके विश्वसनीय हो सकती है। आप आशाराम जागरथ, अदनान कफ़ील दरवेश, हुस्न तबस्सुम निहाँ, अनुज लुगुन, पूनम विश्वकर्मा वासम, घनश्याम कुमार देवांश, वीरू सोनकर, विहाग वैभव आदि अनेक कवि ऐसे हैं जिन पर बात किए बिना आप युवा कविता का अखंड भूगोल नहीं पा सकते। इस भूमिका के द्वारा मैं इस पीढ़ी के एक प्रतिनिधि कवि पर बात करना चाहता हूँ। उनका नाम है—वीरू सोनकर। इस युवा कवि के लिए किसी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा नहीं खोला। यह अपनी क्षमता और प्रतिभा के दम पर हिंदी समाज को हलकारने वाला बरियार साँड है। इस कवि का जो संग्रह मेरे हाथ में है, वह मुझे बहुत व्यक्ति-व्यंजक लगा—‘मेरी राशि का अधिपति एक साँड है’। इसकी चमकदार सींगों के निशाने पर जब-तब मैं भी पड़ता और किसी तरह बचकर निकलता रहा हूँ। मैं जानता हूँ, वह मित्र है और उससे भी आगे एक क्षमतावान कवि है—
इस दुनिया को चाहिए
कि उसके मुँह न लगे
उसे रास्ता दें और उसके सींगों की इज़्ज़त करें।
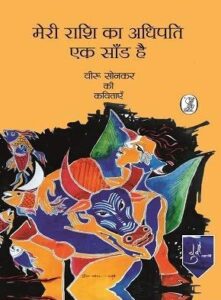
मेरी राशि का अधिपति एक साँड है │ स्रोत : वाणी प्रकाशन
जब दुनिया इतनी समतल होती जा रही है तो एक युवा कवि में इतना उत्ताप और सात्विक क्रोध आश्वस्तिकारी लगता है। इसी साहस और उत्ताप पर तो इतिहास का इंजन आगे बढ़ता है। ये पंक्तियाँ इस संग्रह की किंचित लंबी कविता—‘एक उजड्ड का बयान’—से हैं। इस कविता को पढ़ते हुए मुझे देवी प्रसाद मिश्र की कविताओं में अंतर्विन्यस्त आदिम क्रोध और उत्ताप याद आता रहा—
तमाम लामबंदियों के ख़िलाफ़ मेरे पास एक गुलेल थी
और नदियों की तरह शहरों और शिल्पों और वस्तुओं
को छोड़ देने का वानप्रस्थ, मेरे पास बहुत आदिम क्रोध
था और सत्तावानों को घूरकर देखने का हुनर।
वीरू सोनकर के पास कविता में घूरकर देखने का ‘हुनर’ भले कम हो, साहस की कमी नहीं है। यह साहस ही इस कवि के लिए कविता में संभावनाएँ और दुर्घटनाएँ लेकर आता है। उसके भीतर का ग़ुस्सा संग्रह की तमाम कविताओं में मद्धम-मुखर दिखाई पड़ेगा। पहचान की ज़मीन में धँसी कविताओं में आक्रोश और प्रतिशोध की टेर होती है। आक्रोश और प्रतिशोध एकोन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी, परिणामोन्मुख और आवेगशील होता है। ग़ुस्सा सर्वतोन्मुखी होता है, इसकी कई दिशाएँ होती हैं। आक्रोश और प्रतिशोध को किन्हीं व्याख्याओं और धारणाओं से नियंत्रित किया जाता है। ग़ुस्सा बहुत कुछ प्रतिक्रियाशील और सहज होता है। वीरू की कविताओं में मौजूद ग़ुस्सा बहुमुखी है। वह सामाजिक, आर्थिक, संरचना और परिवेशगत विडंबनाओं के प्रति है। यह ग़ुस्सा अंदर की तरफ़ खुलकर गाँठ नहीं बनता, बाहर की तरफ़ खुलकर विस्फोट करता है। इसका फल यह होता है कि चीथ डालने वाले आत्मसंघर्ष और बेचैन कर देने वाली मॉर्बिडिटी से बच जाते हैं, जो मृत्युंजय, उस्मान ख़ान, अच्युतानंद मिश्र आदि कुछ अच्छे युवा रचनाकारों में गहराई से महसूस होती है।
इसकी दुनिया बहुत उन्मुक्त और खुली हुई है। इसका आत्मवृत्त और और वृत्तों को छूता, काटता, शामिल करता, समोता बढ़ता दिखाई पड़ता है। शायद इसीलिए बहुत से युवा रचनाकारों में पाई जाने वाली मुग्ध क़िस्म की उदासी से बच गया है। इसमें अपराधबोध, पराजयबोध, अवसाद आदि लगभग नहीं है। अभी इसकी चेतना दरकी नहीं है। यह अखंड, मुकम्मल और ठोस है। इसकी आवाज़ सदिश और ताक़तवर इसीलिए ही है। उसकी अभिव्यक्ति सुलझी हुई, सीधी और प्रभावी है। इस नोकदार प्रभावशीलता का कारण इसका अखंडित, कुँवारा आत्म है। इसके पीछे इसके निर्दोष भाव हैं, जिसमें कोई फाँक नहीं आई। अगर उसके स्व-बोध में टूटन होती तो अभिव्यक्तियाँ खंडित होकर बिखर जातीं। इसलिए इस संग्रह की कविताएँ अपने सधेपन, लक्ष्योन्मुख प्रक्षेप और सुलझेपन के कारण अपनी शैली से साठोत्तरी वाम कविता की याद दिलाएँगी—
मैं आदमी नहीं मातृभाषा से हटकर
दूसरी भाषा में बरती गई एक चालाकी हूँ”
“कई तरीक़े हैं भविष्य तक जाने के
एक औरत को जितनी तरह से उतारा जा सकता है बाज़ार में
उतनी ही तरह से जाया जा सकता है एक बहुत बुरे भविष्य में
~•~
भूख अपने हर रंग में एक गर्म रोटी का चेहरा है
जिस पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ता
~•~
जंगल एक अमिट स्मृति है
सड़कों पर छाई सुनसान रात उस बाघ की परछाई है
जो तुम्हारे शहर कभी नहीं आता
इन पंक्तियों को संग्रह में जहाँ-तहाँ से उठा लिया गया है। ऐसे कितने ही कथन मिलेंगे जहाँ आप सोचने के लिए रुकेंगे और फिर वे पंक्तियाँ आपके साथ हो लेंगी। लेकिन इससे भी आगे की उल्लेखनीय बात यह है कि ये पंक्तियाँ कविता का आवयविक हिस्सा हैं। इन्हें वहाँ से अलग करना भी कलात्मक हिंसा है। इनके पीछे अनुभव और गहन अंतर्दृष्टि है। इस भाषा और शैली को समझने के लिए संग्रह के पहले खंड की एक बहुत गठी हुई कविता—‘ठीक-ठाक देश-सा’—का काव्यांश देखिए—
जहाँ रोज़ घट रही हैं
उस देह को काटने की साज़िशें,
मैं उसके मुँह से बस्तर की आवाज़-सा कराहता हूँ
ऋचाएँ और आयतें सुन-सुन कर
मैं एक कान से बहरा हूँ
मैं विकास की दौड़ में पीछे रह गया
डेढ़ पैर का धावक हूँ
मैं सन्नाटे में मिल गई
एक अकेली स्त्री का भय हूँ,
नक़्शे की शक्ल में बहुत दूर तक फैली एक राष्ट्रीय असुरक्षा हूँ,
तीन युद्ध जीतने, और एक युद्ध हारने का सीधा-सपाट बयान हूँ,
मैं सबसे पीछे खड़े आदमी की शक्ल पर हर रात उतर आया
एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न हूँ
अगर सहमत हों आप सब,
तो मैं उस देश से पूछना चाहता हूँ
कि क्या मैं तुममें किसी ठीक-ठाक देश-सा घट जाऊँ?
वीरू सोनकर जागरूक और ज़िम्मेदार कवि हैं। इनके जीवन-बोध का संसार बाहर की तरफ़ खुलता है और अपनी पीढ़ी की अपेक्षा विस्तृत है। लेकिन अभी अंदर की आँख खुलेगी। अभी आत्म-सजगता का वैभव उद्घाटित होना शेष है। आत्म-शोधन और आत्म-सजगता भाषिक सजगता को विस्तार मिलेगा। जहाँ वह शब्दों के अर्थ आयाम से आगे बढ़कर उनके ध्वन्यात्मक, लयात्मक और दृश्यगत आयामों का नया द्वार खोल देगा। ये सीमाएँ और युवा कवियों की भी हैं। इस संग्रह से ठीक पहले रश्मि भारद्वाज का नया संग्रह पढ़ रहा था—‘मैंने अपनी माँ को जन्म दिया’। रश्मि ने एक जगह ‘आँख में कंकड़’ पड़ना लिखा है। उनका यह प्रयोग सूजी के हलवे में कंकड़ की तरह गले में अटक गया। रश्मि का संग्रह अच्छा है, इसलिए किसी तरह घोंट गया। लेकिन अभी उसे पचा भी नहीं पाया था कि वीरू के एक ही संग्रह में एकाधिक बार आँख में कंकड़ पड़ गया—
देखा जा सकता था उसे
कंकड़ पड़ी आँख को मलते हुए
~•~
पड़ा रहता है विडंबना की आँख में
किसी कंकड़ की तरह
~•~
मेरी आँखों में पड़ा पुंसत्व का कंकड़
एक बन रही स्त्री की आँख में चुभता रहा
जब कोई कवि अपनी मौलिक अनुभूति के प्रति सजग और आग्रही होता है तो वह उसी रंग और वज़न के शब्द चुनता है, लेकिन अगर यह आत्म-सजगता और उसे उसी मौलिक रूप में अभिव्यक्त करने का आग्रह ढीला-ढाला है तो वह शब्द चुनाव भी तदर्थ और कामचलाऊ करता है। वर्षों पहले मुझे मेरे कवि मित्र अच्युतानंद मिश्र ने अपना संग्रह दिया था। संग्रह का शीर्षक है—‘आँख में तिनका’। मुझे याद है कि उनके अमर्ष का जोखिम लेकर मैं घंटों बहस करता रहा था। दरअसल, तिनका के ‘क’ में जो अकार लगा है वह तृण की गुरुता और आकार को इतना बढ़ा देता है कि वह आँख में पड़ ही नहीं सकता। और अगर पड़ भी जाए तो गड़ नहीं सकता। परंतु अब दो युवा कवियों के इस कंकड़धर्मी प्रयोग को देखकर मैं अपने मित्र अच्युताजी को माफ़ कर सकता हूँ। ‘कंकड़’ में जो ‘ड़’ है, वह इतना बड़ा और कड़ा है कि उससे आँख फूट सकती है, लेकिन वह आँख में पड़ नहीं सकता।
युवा कवि मित्रों को अपनी परंपरा से सीखना चाहिए। बहुत महान लोग गुजरे हैं। उनसे भाषिक सजगता सीख सकते हैं। निराला ने अपनी पहली लोकप्रिय कविता का शीर्षक ही ग़लत लिखा है! शब्द ‘जुही’ नहीं ‘जूही’ है। निराला ने ‘जुही की कली’ शीर्षक दिया है। तमाम लोग इसे सुधार कर ‘जूही की कली’ लिखते और बोलते हैं। निराला ने अपनी कविता का विश्लेषण करते हुए इसका औचित्य समझाया है। ‘जूही’ लिखते ही कुप्पीकार, तन्वंगी, कोमल कली ‘ऊकार’ की गुरुता से अपना सारा सौंदर्य ही खो देगी। निराला ने जिस लेख में इस प्रयोग के औचित्य को समझाया है, वह काव्य-सौंदर्य-समीक्षा में अपूर्व और अतुलनीय है। अगर आधुनिक साहित्य में इससे तुलनीय कोई विश्लेषण है तो वह महाप्राण की ही ‘बैठ लें कुछ देर आओ’ शीर्षक कविता का कवियों के कवि शमशेर द्वारा किया गया विश्लेषण। जो मूलतः शमशेर का इलाहाबाद में दिया गया एक व्याख्यान है। कहना यह है कि यदि इन कविताओं का कवि आत्म-जिज्ञासा और आत्म-संघर्ष में उतरता है तो उसमें आंतरिकता, विविधार्थकता, सूक्ष्मता, सघनता आती जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपना रचनात्मक तनाव खोते ही बड़बोला, भड़भड़िया और सार्वभौमिक लताड़िया बन जाएगा।






