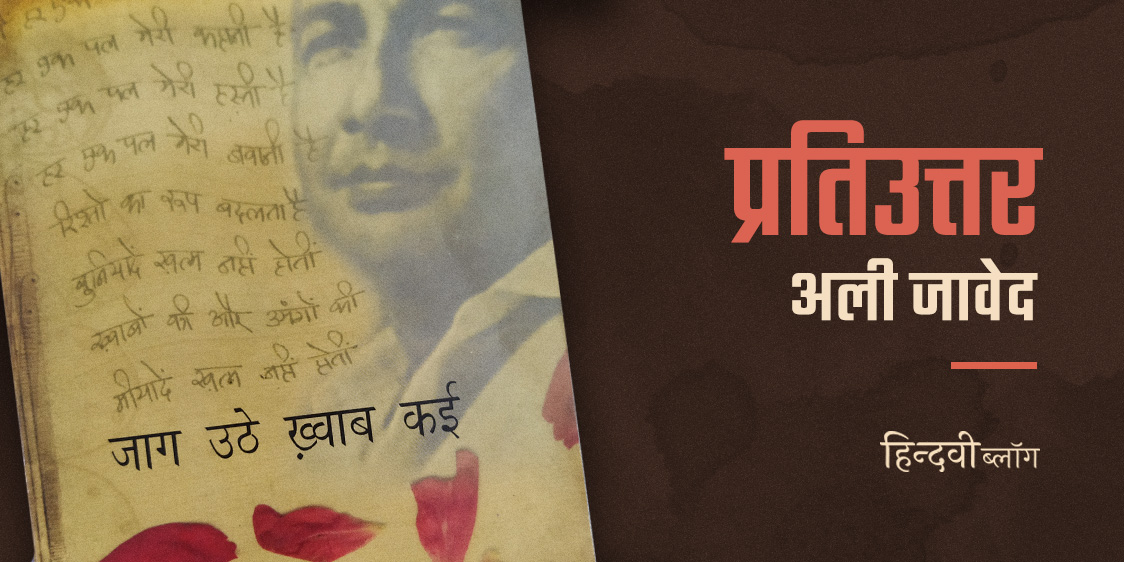
दुश्मनी जम कर करो लेकिन…
 अली जावेद
अगस्त 9, 2021
अली जावेद
अगस्त 9, 2021
प्रतिउत्तर की पृष्ठभूमि :
जनवाद और साहित्य की तिजारत
इतनी न बढ़ा पाकी-ए-दामाँ की हिकायत
दामन को ज़रा देख ज़रा बंद-ए-क़बा देख
— मुस्तफ़ा ख़ाँ शेफ़्ता
पिछले दिनों यानी 13 जुलाई 2021 को ‘जाग उठे ख़्वाब कई’ (साहिर लुधियानवी की रचनाएँ, संचयन-संपादन : मुरलीमनोहर प्रसाद सिंह, कांतिमोहन ‘सोज़’ और रेखा अवस्थी; प्रकाशक : पेंगुइन हिंदी, संस्करण : 2010) पर मेरी एक समीक्षात्मक टिप्पणी हिन्दवी ब्लॉग पर छपी थी। इस पर इस पुस्तक के संकलनकर्ताओं और ‘जनवादी लेखक संघ’ के राष्ट्रीय उपमहासचिव (संजीव कुमार) की प्रतिक्रियाएँ मुझे प्राप्त हुई हैं। संकलनकर्ताओं की प्रतिक्रिया मेरी टिप्पणी के कमेंट के रूप में और और ‘जनवादी लेखक संघ’ के राष्ट्रीय उपमहासचिव की प्रतिक्रिया उनकी फ़ेसबुक पोस्ट (30 जुलाई 2021) के रूप में पढ़ी जा सकती हैं। फ़ेसबुक पोस्ट में मैं भी टैग हूँ।
इन प्रतिक्रियाओं पर कुछ कहने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह टिप्पणी मैंने जनवादी लेखक संघ के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उस किताब के संकलनकर्ताओं द्वारा की गई विसंगतियों को लेकर की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं, न कि प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। अफ़सोस की बात है कि संजीव कुमार ने इसे दो लेखक संगठनों के बीच विवाद के रूप में पेश किया है। पाठकों से मेरा निवेदन है कि इसे साहित्यिक स्तर पर विचारों की सहमति और असहमतियों के रूप में देखें और राय क़ायम करें। मैं अपने दोस्त संजीव कुमार से भी निवेदन करता हूँ कि इसे दो संगठनों के दरमियान वाद-विवाद का मुद्दा न बनाएँ। अगर विचारों के स्तर पर सहमतियों और असहमतियों को जगह नहीं दी गई तो हम जिस बात पर ज़ोर देते हैं यानी ‘अनेकता में एकता’, उस सोच को नुक़सान होगा और हम एकरूपता के मकड़जाल में फँस जाएँगे जो सांप्रदायिक ताक़तों का एक मात्र एजेंडा है यानी ‘एक भाषा, एक धर्म और एक देश’ वाली मानसिकता। साहित्यिक विचारों में अगर मतभेद नहीं होंगे और विचारों का आदान-प्रदान नहीं होगा तो हम जड़ता का शिकार होंगे और यह संकीर्णता हमें उन सांप्रदायिक ताक़तों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के हथियार के रूप में मददगार साबित होगी। इस बात को बार-बार दुहराते हुए कि इसे दो संगठनों के बीच विवाद का मुद्दा न बनाकर बहस को साहित्यिक स्तर पर विचारों के आदान-प्रदान के रूप में देखने की कोशिश करें, वरना ऐसा न करने से क्या नुक़सान हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में संजीव कुमार को और ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
दूसरे यह कि राजनैतिक और साहित्यिक विचारों में भी फ़र्क़ करना चाहिए। साहित्य, राजनैतिक स्तर पर तैयार किया गया पार्टी का दस्तावेज़ नहीं है, जिस पर एक ख़ास राजनैतिक दल के लोग अमल करने को बाध्य हो सकते हैं; साहित्य में ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए 1936 में प्रेमचंद ने साहित्य को सियासत का मार्गदर्शन करने वाली एक मशाल के रूप में देखने की बात की थी। सज्जाद ज़हीर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, लेकिन प्रेमचंद और दूसरे बड़े साहित्यकार अलग-अलग जनतांत्रिक विचारों से संबद्ध थे जो प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े थे और जिनके विचारों में भिन्नता थी। यही वजह है 1949 की प्रगतिशील लेखक संघ की आल इंडिया कॉन्फ़्रेंस में सआदत हसन मंटो के ख़िलाफ़ जो प्रस्ताव आया उसका मौलाना हसरत मोहानी ने विरोध किया और वह प्रस्ताव वापस लिया गया। इसी तरह फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की मशहूर नज़्म—‘सुब्ह-ए-आज़ादी’ पर सरदार जाफ़री ने अपनी सख़्त टिप्पणी दी जिसकी फ़ैज़ ने परवाह नहीं की और दोनों अपने विचारों पर क़ायम रहे और पाठकों का बहुमत फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के साथ रहा।
यह दुखद है संकलनकर्ताओं के वकील के तौर पर संगठन के उपमहासचिव संजीव कुमार उतरे जिनका रवैया यह है कि :
न करो ज़िल्ले इलाही की बुराई कोई
दोस्तो कुफ़्र न फैलाओ नमकख़्वारों में
लेकिन अस्ल मुद्दा यह है कि :
आप दस्तार उतारें तो कोई फ़ैसला हो
लोग कहते हैं के सर होते हैं दस्तारों में
दरअस्ल, 2021 साहिर लुधियानवी का जन्मशती वर्ष है और इस सिलसिले में उन पर विभिन्न भाषाओं में लिखित और संकलित किताबों को पढ़ने के दौरान यह चर्चित किताब भी मेरी नज़र से गुज़री; जिसमें एक पाठक के तौर पर मुझे कई कमियाँ नज़र आईं जिस पर मैंने अपना रद्दे-अमल ज़ाहिर किया तो हमारे दोस्त संजीव कुमार अपने साथ भक्तों की एक फ़ौज लेकर कूद पड़े, जैसे मुझसे कोई ईश-निंदा का जुर्म सरज़द हो गया है। मैं उनको इक़बाल का एक शे’र सुनाते हुए उनकी प्रतिक्रिया पर कुछ जवाब देने की हिम्मत करूँगा, अगर उनके तेवर कुछ नर्म हों और वह कुछ सुनने के मूड में हों। शे’र यह है :
नहीं है ना-उमीद ‘इक़बाल’ अपनी किश्त-ए-वीराँ से
ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी
संजीव कुमार की टिप्पणी का क्रमवार जवाब :
एक
मैंने पहले भी साफ़ किया और एक बार फिर दुहराता चलूँ कि 2021 साहिर लुधियानवी का जन्मशती वर्ष है और इसी सिलसिले में साहिर पर जो किताबें हिंदी, उर्दू या अँग्रेज़ी में छपी हैं; उन्हें पढ़ने में मेरी दिलचस्पी हुई तो यह किताब भी नज़र से गुज़री जो 2010 में छपी थी। मैं अपनी कम-इल्मी और अपराध के लिए संजीव कुमार से क्षमा-याचना करता हूँ कि 2010 में छपी यह किताब मैंने पढ़ी। क्या प्रकाशकों ने इस किताब को वापस लेने की घोषणा कर दी थी? उनसे इस बात की इजाज़त की उम्मीद तो करता ही हूँ कि 2010 में छपी किताब पर अपनी टिप्पणी दे सकूँ या फिर यह मानकर चलूँ कि 2021 से पहले छपी किताबों पर अपनी राय देने का कोई अधिकार नहीं है? संजीव जी के ध्यानाकर्षण के बाद मैं 2012 का संस्करण भी पढ़ूँगा, लेकिन क्या संजीव जी इस बात की गारंटी लेते हैं कि उसमें कोई ग़लती नहीं होगी? क्या वह भी मुरली जी की तरह उर्दू के ज्ञानी हो गए हैं?
दो
मैंने ग़लतियाँ निकालते वक़्त कोई स्वयंभू फ़ैसला नहीं दिया, बस इतना निवेदन किया है कि शुरू से अंत तक लिप्यंतरण का उर्दू शब्दों की देवनागरी वर्तनी का जो तरीक़ा अपनाया जाए उसमें यकसानियत होनी चाहिए थी, जिसकी मिसाल भी मैंने दी है। यानी ग़ालिब के काव्य-संग्रह को देवनागरी में लिखने के दो तरीक़े हो सकते हैं : ‘दीवाने-ग़ालिब’ या ‘दीवान-ए-ग़ालिब’। ये दोनों तरीक़े सही हैं, लेकिन पूरी किताब में शब्दों के देवनागरी में लिखने के अलग-अलग तरीक़े नहीं होने चाहिए। जहाँ तक मद्दाह के शब्दकोश का ताअल्लुक़ है, बलंद और बुलंद के उच्चारण के मामले में ‘बुलंद’ को ग़लत-उल-आम माना गया है, यानी अवामी सतह पर कुछ शब्द ग़लती से रवाज पा जाने की श्रेणी में आता है। तजरुबा या तजुरबा दोनों सही हैं, लेकिन सजीव कुमार ने पाठकों को गुमराह करने की कोशिश की है।
गुलज़ार ने प्रस्तावना में पहला शब्द ‘तज़रुबा’ लिखा है जो बिल्कुल ग़लत है। यानी ‘ज’ के नीचे बिंदी (नुक़्ता) नहीं होनी चाहिए थी। संजीव कुमार मद्दाह को बीच में लाकर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोई मानक रूप तय नहीं किया। सिर्फ़ निवेदन यह है कि अगर शब्दों के उच्चारण को ठीक करने की बात है तो उन शब्दों के नीचे बिंदी लगाने से परहेज़ किया जाए जिससे शब्द निरर्थक हो जाए या उसके मानी ही बदल जाएँ क्योंकि उर्दू ज़बान के उच्चारण की बारीकियाँ न जानने से शब्दों के मानी बदल जाते हैं। जैसे ‘तज़रुबा’ उर्दू में कोई शब्द नहीं है। इसी तरह नुक़्ता लगाने या न लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे अगर आप जलील शब्द के नीचे बिंदी लगा दें तो यह एक गाली बन जाती है। यानी जलील माने प्रतिष्ठित और ज़लील माने घटिया या कमीना हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, जो उर्दू से वाक़फ़ियत न रखने वाला समझ नहीं सकता। मैंने ‘ख़ास-व-आम’ की बात भी की थी और कहा था उर्दू में ‘ख़ास-ओ-आम’ सही है। इसके अलावा मैंने ‘जज़्बातों’ पर भी एतराज़ किया था और कहा था कि ‘जज़्बातों’ कोई शब्द नहीं है, ‘जज़्बात’ सही है, इसे संजीव कुमार ने अपनी सुविधानुसार जानबूझकर अनदेखा कर दिया।
तीन
जहाँ तक ‘क़ूव्वत’ और ‘क़ुव्वत’ की बात है, ये दोनों ठीक हैं। अगर मद्दाह साहब ने ‘क़ूव्वत’ का ज़िक्र नहीं किया तो इससे उर्दू के विद्वानों को क्या सरोकार, लेकिन क़ूव्वत ज़्यादा सही है। यहाँ पर रेखांकित करना ज़रूरी है कि उर्दू में ‘क़ूव्वत’ और ‘क़ुव्वत’ दोनों सही हैं। देखना यह होता है कि शायरी में वज़्न की ज़रूरत के तहत किस रूप में लिखना उचित है। बाक़ी जिन ग़लतियों की तरफ़ मैंने इशारा किया है और जिसे हमारे क़ाबिल दोस्त ने जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया है, क्या उन्हें संजीव कुमार की तरफ़ से सनद के तौर पर मान लिया जाए? मैं उन हिंदी लेखकों का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ जो शब्दों के नीचे बिंदी लगाने के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें महान लेखक अमृतलाल नागर भी शामिल हैं। लेकिन अगर उच्चारण की सार्थकता के लिए शब्दों के नीचे बिंदी की वकालत की जाए तो फिर इसमें ‘तजरूबा या तजुरबा’ का ‘तज़रूबा’ कर देना उचित नहीं बल्कि अज्ञानता दर्शाता है। दूसरे यह कि मद्दाह साहब का रोब झाड़कर ग़लत को सच नहीं साबित किया जा सकता। शब्दों के लिखने और बोलने में थोड़ा फ़र्क़ होता है। ग़लत बोलने को ग़लत-उल-आम के दायरे में रखा जा सकता है। लेकिन लिखने में तो सतर्कता बरतनी ही पड़ती है।
मद्दाह साहब ने ख़ुद लिखा है कि ‘बलंद’ ज़्यादा सही है।
चार
अब रही बात गुलज़ार साहब और मुरली जी की तो हमारे दोस्त ने बातों की जलेबी इस तरह बनाई है, जैसे मैंने गुलज़ार साहब को उर्दू न जानने वाला कहा है। संजीव जी ग़ौर से पढ़िए मेरी बात को। मैंने संदेह व्यक्त किया है कि शायद गुलज़ार द्वारा लिखी प्रस्तावना का मसविदा उन्हें दिखाया नहीं गया। फिर आगे मैंने लिखा है कि अगर देखने के बाद उन्होंने ‘तज़रूबा’ या ‘जज़्बातों’ लिखा है तो मुझे उनके उर्दू के ज्ञान पर शक है।
मैंने मुरली जी की ‘भूमिका’ की तरफ़ इशारा करते हुए यह दावा किया है कि उन्हें उर्दू नहीं आती। इसी संदर्भ में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जब हम साहित्य की बात करते हैं तो फ़िल्मी और संजीदा शाइरी में फ़र्क़ करते हैं। मजरूह, कैफ़ी, साहिर या जाँ निसार अख़्तर वग़ैरह की साहित्यिक पहचान इसलिए नहीं कि उन्होंने फ़िल्मी गाने लिखे; बल्कि ये लोग साहित्य के क्षेत्र में उर्दू के बड़े शाइर इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी सृजनशीलता और गहरी साहित्यिक दृष्टि के आधार पर फ़िल्मों को भी प्रतिष्ठित किया। ये अपनी फ़िल्मी शाइरी की वजह से नहीं, उर्दू की उच्च साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने की वजह से प्रतिष्ठित हैं; जबकि गुलज़ार साहब का उर्दू साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है और वह केवल एक फ़िल्मी शाइर की हैसियत रखते हैं। यह अलग बात है कि मुरली जी को प्रस्तावना लिखने के लिए उर्दू का कोई प्रतिष्ठित आलोचक नहीं मिला और उनको गुलज़ार साहब, उर्दू शाइर साहिर पर टीका करने को मिले।
पाँच
हमारे दोस्त ने 60-70 हज़ार शब्दों में फैली किताब से 8-10 ग़लतियों की बात करके प्रसंग को और भी हास्यप्रद बना दिया है। मुरली जी की भूमिका के अलावा साहिर की शाइरी के टेक्स्ट में जो ग़लतियाँ की गई हैं, वे अनगिनत हैं और इन्हें यूँ ही टाइपिंग की ग़लती कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह हास्यास्पद ही नहीं, बल्कि ग़लत को ग़लत न मानकर ‘चोरी और सीनाज़ोरी’ जैसा व्यवहार है, जो और भी अधिक निंदनीय है। अच्छा होता कि मेरी टिप्पणी पर बदले की भावना न अपनाकर अपने किसी जानकार उर्दू के मित्र से, जो वैचारिक स्तर पर मेरे ख़िलाफ़ भी हो, जवाब लिखवाने का काम किया गया होता। लेकिन ‘बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुब्हान अल्लाह’ वाला रवैया अपनाया गया है।
छह
अब आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर! मैं संजीव कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा ज्ञानवर्धन कराते हुए यह बताया कि मुरली जी दो बार नहीं बल्कि तीन बार डूटा (Delhi University Teacher Association) के अध्यक्ष रहे। तब तो यह तथ्य मेरी बात को और भी मज़बूती देता है कि तीन बार डूटा का अध्यक्ष रहने वाले शख़्स ने कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली उर्दू को बचाने में ज़ीरो भूमिका अदा की और आज कई कॉलेजों में उर्दू विभाग बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं। यह दलील कि मैं भी एक बार डूटा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा। मैं क्या कहूँ! यह एक ऐसी बचकानी दलील है जिस पर रोया जाए या हँसा जाए, समझ में नहीं आता! सब जानते हैं कि डूटा पूरी तरह से अध्यक्ष केंद्रित संगठन है। मुरली जी जिस शिक्षक गुट के सदस्य हैं, उसका पहले भी डूटा में वर्चस्व रहा है और आज भी है। मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर हमारे मित्र इस पर विस्तार से बात करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना कहता चलूँ कि अपने ग्रुप की ओर से मैं अकेला निर्वाचित प्रतिनिधि था और इक्कीस कार्यकारिणी सदस्यों पर आधारित मेरी आवाज़ सुनी-अनसुनी कर दी गई सिवाय इसके कि विजय सिंह और तृप्ता वाही, जो डूटा कार्यकारिणी में नहीं थे, इन लोगों ने बाहर से उर्दू के ख़िलाफ़ प्रशासन के रवैए की निंदा की और मेरा साथ दिया।
सात
यह दलील कि अली जावेद ने प्रकाश पंडित के अलावा अपनी तरफ़ से क्या योगदान दिया। क्या कहूँ, सिवाय अफ़सोस के! प्रकाश पंडित के नाम पर मैं अपना सिर झुकाता हूँ कि उन्होंने उर्दू शाइरी को हिंदी पाठकों तक पहुँचाने में बड़ा सराहनीय कारनामा अंजाम दिया है। उनको हक़ भी था, क्योंकि बुनियादी तौर पर वह उर्दू के लेखक थे और उर्दू शाइरी की बारीकियों से बख़ूबी वाक़िफ़ थे। अब यह सवाल कि अली जावेद का क्या योगदान है तो इसका जवाब यह है कि मुरली जी की तरह मेरे पास ऐसे संसाधन नहीं थे—दूसरे यह कि अगर अली जावेद का कोई योगदान नहीं है तो यह अधिकार मुरली जी को कैसे मिल जाता है कि अपने असर और संपर्कों का इस्तिमाल करके उर्दू के साथ खिलवाड़ करें। क्या इससे, इस रवैए की पुष्टि नहीं होती कि ‘उर्दू-सुर्दू’ को जैसे चाहो इस्तिमाल करो!
क्या इसे भी साहित्य के नैतिक मूल्यों की एक मिसाल समझा जाए कि जिस व्यक्ति ने बुनियादी काम यानी लिप्यंतरण किया, वह इस बात का हक़दार भी नहीं कि उसका नाम कवर पेज पर हो और उसका नाम कॉपीराइट रखने वालों की सूची में हो?
आठ
मैं मुरली जी से परिचित पीढ़ी का व्यक्ति हूँ, इसलिए उनके इस कार्य पर और भी दुखी और पीड़ित महसूस करता हूँ कि एक साहित्यकार को जो बुनियादी साहित्यिक नैतिकता का निर्वहन करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया। आपातकाल में अठारह माह जेल में रहने से क्या उन्हें यह सनद हासिल हो जाती है कि भविष्य में उनके सारे ग़लत कामों पर सदाक़त की मुहर लगा दी जाए। और क्या अठारह माह जेल में रहने का मुआवज़ा इस तरह वसूल करेंगे?
मेरे पास मिसालें बहुत हैं। लेकिन मैं इस वक़्त विस्तार में नहीं जाना चाहता कि किस तरह मुरली जी की रणनीतियों ने डूटा को कितना नुक़सान पहुँचाया है। आज डूटा, जो सारे देश में सबसे प्रतिष्ठित संगठन था, उसकी जो हालत हो गई है। इस पर अगर संजीव कुमार चाहेंगे तो विस्तार से बहस करने को तैयार हूँ।
नौ
आख़िर में संजीव जी ने मेरे हल्केपन का ज़िक्र किया है। वाह भाई, वाह! ‘बुत हमको कहें काफ़िर, अल्लाह की मर्ज़ी है।’ …यहाँ बुनियादी बहस यह नहीं कि हिंदी-उर्दू पट्टी से आने वाले व्यक्ति को उर्दू पर अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं। ज़ाहिर है, उर्दू पर मेरी इजारादारी नहीं है और मैं मुरली जी के इस अधिकार को कैसे छीन सकता हूँ। लेकिन एक साहित्य के विद्यार्थी की हैसियत से मैं अपना सवाल फिर दुहराता हूँ, जिसका जवाब मेरे क़ाबिल दोस्त ने नहीं दिया या जानबूझकर अठारह माह की जेल और मुरली जी के ‘नि:स्वार्थ जीवन’ की भूल भुलैयों में घुमाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति जो उर्दू से नावाक़िफ़ है, उसे यह अधिकार है कि उर्दू के किसी शाइर पर एक किताब का संकलन करे। मैं तो इसे साहित्यिक नैतिकता के ख़िलाफ़ ही समझूँगा। अगर कल मैं कबीर, रहीम, रसख़ान, सूर, तुलसी या मीराबाई जैसे दिग्गज कवियों का संकलन करके किताब छपवाने का साहस करूँ तो यह साहस मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं हिंदी साहित्य का एक विद्यार्थी ज़रूर हूँ; लेकिन इन कवियों की उन गूढ़ परंपराओं से वाक़िफ़ नहीं हूँ जिनका ज्ञान ऐसा करते हुए ज़रूरी है। मैं तो यह चेष्टा मीर और ग़ालिब का कलाम संकलित करने में भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए शाइरी की उन बारीकियों से वाक़िफ़ होना ज़रूरी होगा जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपरिहार्य हैं। इसीलिए यह काम किसी साधारण उर्दू के विद्यार्थी ने नहीं किया और इस काम को अली सरदार जाफ़री ने अंजाम दिया, जो कि उनका अधिकार था।
क्या यह कार्य उस मानसिकता की तरफ़ इशारा नहीं करता कि सांप्रदायिक तत्त्वों की ओर से नफ़रत और बहिष्कृत करने के बदले कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए ‘हमदर्दी’ के नाम पर उर्दू को बेचारी समझकर जिस तरह चाहें बर्ताव करें?
यह बात इसलिए भी दुहराते हुए दुख होता है कि संजीव कुमार अपनी टिप्पणी के साथ जिस तरह ट्रोल करने वाले भक्तों का एक दल लेकर मैदान में कूदे हैं, वह एक जनवादी परंपरा का श्रेय लेने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कुछ भक्तों ने मुझे कुंठित मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति कहा तो कुछ ने हिंदी और उर्दू के विवाद का अखाड़ा बना दिया। कुछ ने इस बात का दावा किया कि अली जावेद श्रद्धा लिखकर या बोलकर दिखाएँ आदि-आदि।
भक्तों ने एक साहित्यिक बहस को आगे न बढ़ाकर हिंदी के वर्चस्व का झंडा बलंद किया, जिससे हमारी उस प्रगतिशील-जनवादी परंपरा को गहरा आघात लगा है; जिसकी विरासत का हम दावा करते हैं।
मैं बार-बार यह बात दुहराऊँगा कि मुरली जी चूँकि उर्दू भाषा और साहित्य से वाक़िफ़ नहीं हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करने की ग़लती स्वीकार करनी चाहिए।
मैं आगे भी बहस के लिए तैयार हूँ और अपनी तरफ़ से एक बार फिर साफ़ कर देना चाहता हूँ कि आगे जो भी बहस होगी, वह प्रगतिशील लेखक संघ का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं करेगा बल्कि अली जावेद अपनी व्यक्तिगत पहचान के आधार पर करेगा और दो संगठनों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता के तौर पर नहीं करेगा।
साहित्य में सहमतियाँ और असहमतियाँ रही हैं और रहेंगी जिनका मैं सम्मान करता हूँ और इस बात का यक़ीन दिलाता हूँ कि मैं अपने समर्थकों की फ़ौज लेकर मैदान सर करने के लिए नहीं, बल्कि एक सकारात्मक मानसिकता के साथ बहस करूँगा। मैं अपनी बात अली सरदार जाफ़री की इन पंक्तियों के साथ समाप्त करते हुए संजीव कुमार को यह राय दूँगा कि आने वाले कारवाँ के सिपह-सालार आप जैसे नौजवान होंगे, क्योंकि मैं तो एक सत्तर साल के बूढ़े की हैसियत से इतनी सक्रिय भूमिका नहीं अदा कर सकूँगा। (यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अनुमान के मुताबिक़ संजीव कुमार शायद मुझसे 15-20 साल छोटे होंगे)। ख़ैर! सरदार जाफ़री की पंक्तियाँ यूँ हैं :
इधर भी हल्क़-ए-याराँ, हुजूम-ए-मुश्ताक़ाँ
इधर भी चाहने वालों की कुछ कमी ही नहीं
हज़ारों साल की तारीख़ है सुबूत इसका
खड़े हैं सीने प ज़ख़्मों के गुल खिलए हुए
क्या करूँ, एक शे’र और याद आ गया, वह भी सुनाता चलूँ :
दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे
जब कभी हम दोस्त हो जाएँ तो शर्मिंदा न हों
~•~
और अंत में
मेरी टिप्पणी पर संकलनकर्ताओं का जवाब देखकर एक बार फिर से दुहराता हूँ कि उर्दू या साहिर पर मेरी इजारादारी नहीं है और न ही मुझे हक़ है कि किसी को साहिर पर कुछ करने-लिखने से रोकूँ। लेकिन जिस भाषा की बारीकियों से संकलनकर्ता वाक़िफ़ नहीं हैं, उन्हें एक किताब संकलित करने से बचना चाहिए। यहाँ मैंने मिसालें भी दी हैं कि संस्कृत में दिलचस्पी और संस्कृत साहित्य के तहत आदर भाव मुझे इस बात का हक़ नहीं देता कि मैं ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ का संपादन करूँ।
साहिर लुधियानवी से लगाव सराहनीय है और इस कार्य के लिए जिस शख़्स ने उनकी शाइरी का लिप्यंतरण किया है, उसका नाम न तो कवर पेज पर है और न ही कॉपीराइट में। यह तिजारत नहीं तो और क्या है?
उर्दू लेखकों पर विशेषांक छापने का यह मतलब नहीं कि भाषा में अज्ञानता के वबावजूद हठधर्मी की जाए। विशेषांक छापना यह भी दर्शाता है कि उपेक्षा के बावजूद उर्दू पर तैयार की गई सामग्री का बाज़ार आज भी है।
मेरी बात पर ध्यान दें, किसी उर्दू वाले ने साहिर पर किताब नहीं लिखी तो क्या हमारे उर्दूप्रेमी संकलनकर्ताओं को कोई उर्दू जानने वाला नहीं मिला कि यह काम उससे करवाया जाता? अगर ऐसा होता तो शायद दूसरे या तीसरे संस्करण में ग़लतियाँ ठीक करने का आश्वासन न देना पड़ता।
जहाँ तक प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) और उर्दू पर प्रगतिशील लेखकों के विचारों का सवाल है तो यह कहना उचित होगा कि सिर्फ़ प्रलेस ने यह माँग बार-बार दुहराई है कि उर्दू को उसका हक़ दिया जाए और जहाँ भी उर्दू लिखने-पढ़ने वालों की बड़ी संख्या है, वहाँ सरकारी स्तर पर उचित सहूलतें मुहय्या करवाई जाएँ। अगर जनवादी लेखक संघ (जलेस) इससे बेहतर विकल्प रखता है तो उसका स्वागत है। लेकिन मेरा फिर से यही निवेदन है कि इसे दो संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा का विषय न बनाया जाए। मैंने जलेस की नीयत पर शक नहीं किया, बल्कि संकलनकर्ताओं की साहित्य के तहत नैतिक ज़िम्मेदारी की बात की है।
मैंने मुरली जी के ‘उर्दू-प्रेम’ पर बात करते हुए यह भी सवाल उठाया है कि तीन बार डूटा के अध्यक्ष रहे और उनके रहते दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कालेजों में उर्दू विभाग बंद हो गए या बंद होने के कगार पर हैं। इस पर मुरली जी के डिप्टी (संजीव कुमार) ने उल्टा मुझसे यह सवाल किया कि मैं भी एक बार डुटा की कार्यकारिणी में था तो मैंने क्या किया!
मेरा निवेदन है कि मुरली जी और साथी इस मानसिकता को छोड़ें कि उनसे कोई ग़लती हो ही नहीं सकती। यह मानसिकता किसी व्यक्ति को रूढ़िवादी और कट्टर बनाती है। हर जगह offense is the best defence की नीति काम नहीं करती। दबे शब्दों में कठमुल्ला और संकीर्ण उर्दूवादी कहकर आप मुझे अपनी बात कहने से रोक नहीं सकते।
अब बात को विराम देते हुए एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि इसे प्रलेस और जलेस के बीच विवाद का मुद्दा न बनाया जाए। सभी लेखकों और सांस्कृतिक संगठनों का फ़र्ज़ है कि सांप्रदायिकता और आतंकवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष में एकजुट हों। साहित्यिक असहमतियों को नाक का सवाल न बनाकर विवेकशीलता से काम लें और प्रगतिशील-जनवादी एकता के भंग होने का डर दिखाकर अपनी ग़लतियों को सही ठहराने की कोशिश न करें।
पुनश्च
कांतिमोहन ‘सोज़’ जी से निवेदन है कि ‘तिज़ारत’ कोई शब्द नहीं, तिजारत है। यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने दो जगह ‘तिज़ारत’ लिखा है।






