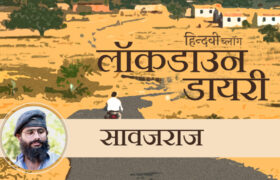दूसरी लहर के साये में
आज सुबह चार बजे ही उठ गया। बादल हैं, हल्का-हल्का उजाला हो रहा है। द्वार पर लगे बेल के पेड़ पर किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया है। वह चहचहा रही है। उसके बच्चे भी हैं। माँ और शिशुओं की आवाज़ आपस में मिल जाती है। बाईं बाँह में वहाँ हल्का-सा दर्द हो रहा है, जहाँ कल टीका लगा था।